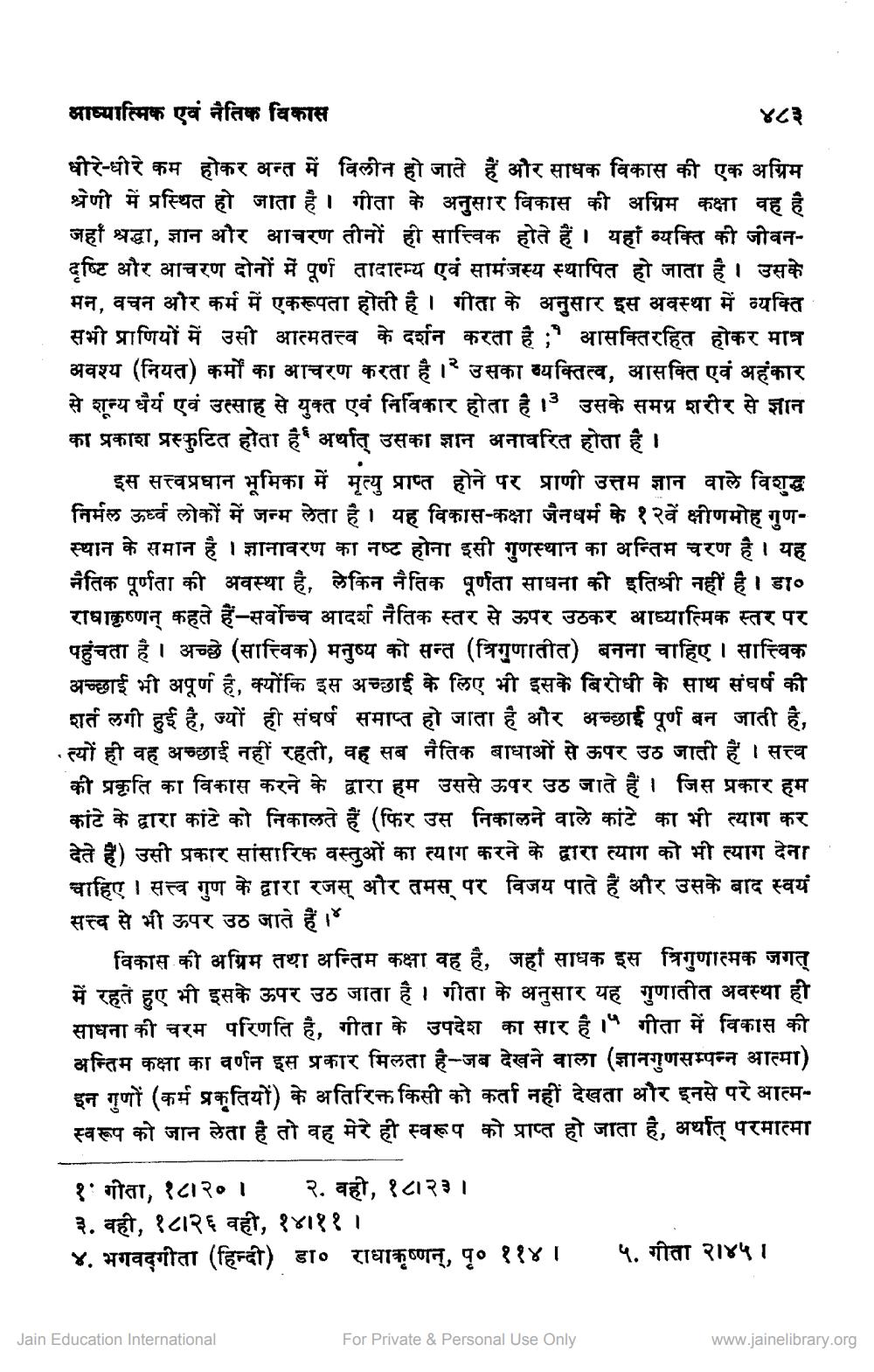________________
आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास
४८३ धीरे-धीरे कम होकर अन्त में विलीन हो जाते हैं और साधक विकास की एक अग्रिम श्रेणी में प्रस्थित हो जाता है। गीता के अनुसार विकास की अग्रिम कक्षा वह है जहाँ श्रद्धा, ज्ञान और आचरण तीनों ही सात्त्विक होते हैं। यहां व्यक्ति की जीवनदृष्टि और आचरण दोनों में पूर्ण तादात्म्य एवं सामंजस्य स्थापित हो जाता है। उसके मन, वचन और कर्म में एकरूपता होती है। गीता के अनुसार इस अवस्था में व्यक्ति सभी प्राणियों में उसी आत्मतत्त्व के दर्शन करता है ; आसक्तिरहित होकर मात्र अवश्य (नियत) कर्मों का आचरण करता है। उसका व्यक्तित्व, आसक्ति एवं अहंकार से शून्य धैर्य एवं उत्साह से युक्त एवं निर्विकार होता है। उसके समग्र शरीर से ज्ञान का प्रकाश प्रस्फुटित होता है अर्थात् उसका ज्ञान अनावरित होता है। ___ इस सत्त्वप्रधान भूमिका में मृत्यु प्राप्त होने पर प्राणी उत्तम ज्ञान वाले विशुद्ध निर्मल ऊर्ध्व लोकों में जन्म लेता है। यह विकास-कक्षा जैनधर्म के १२वें क्षीणमोह गुणस्थान के समान है । ज्ञानावरण का नष्ट होना इसी गुणस्थान का अन्तिम चरण है। यह नैतिक पूर्णता की अवस्था है, लेकिन नैतिक पूर्णता साधना की इतिश्री नहीं है । डा० राधाकृष्णन् कहते हैं-सर्वोच्च आदर्श नैतिक स्तर से ऊपर उठकर आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचता है । अच्छे (सात्त्विक) मनुष्य को सन्त (त्रिगुणातीत) बनना चाहिए । सात्त्विक अच्छाई भी अपूर्ण है, क्योंकि इस अच्छाई के लिए भी इसके बिरोधी के साथ संघर्ष की शर्त लगी हुई है, ज्यों ही संघर्ष समाप्त हो जाता है और अच्छाई पूर्ण बन जाती है, • त्यों ही वह अच्छाई नहीं रहती, वह सब नैतिक बाधाओं से ऊपर उठ जाती है । सत्त्व की प्रकृति का विकास करने के द्वारा हम उससे ऊपर उठ जाते हैं। जिस प्रकार हम कांटे के द्वारा कांटे को निकालते हैं (फिर उस निकालने वाले कांटे का भी त्याग कर देते हैं) उसी प्रकार सांसारिक वस्तुओं का त्याग करने के द्वारा त्याग को भी त्याग देना चाहिए । सत्त्व गुण के द्वारा रजस् और तमस पर विजय पाते हैं और उसके बाद स्वयं सत्त्व से भी ऊपर उठ जाते हैं।
विकास की अग्रिम तथा अन्तिम कक्षा वह है, जहाँ साधक इस त्रिगुणात्मक जगत् में रहते हुए भी इसके ऊपर उठ जाता है। गीता के अनुसार यह गुणातीत अवस्था ही साधना की चरम परिणति है, गीता के उपदेश का सार है। गीता में विकास की अन्तिम कक्षा का वर्णन इस प्रकार मिलता है-जब देखने वाला (ज्ञानगुणसम्पन्न आत्मा) इन गुणों (कर्म प्रकृतियों) के अतिरिक्त किसी को कर्ता नहीं देखता और इनसे परे आत्मस्वरूप को जान लेता है तो वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, अर्थात् परमात्मा
१. गीता, १८।२०। २. वही, १८।२३ । ३. वही, १८।२६ वही, १४।११। ४. भगवद्गीता (हिन्दी) डा० राधाकृष्णन्, पृ० ११४ ।
५. गीता २।४५ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org