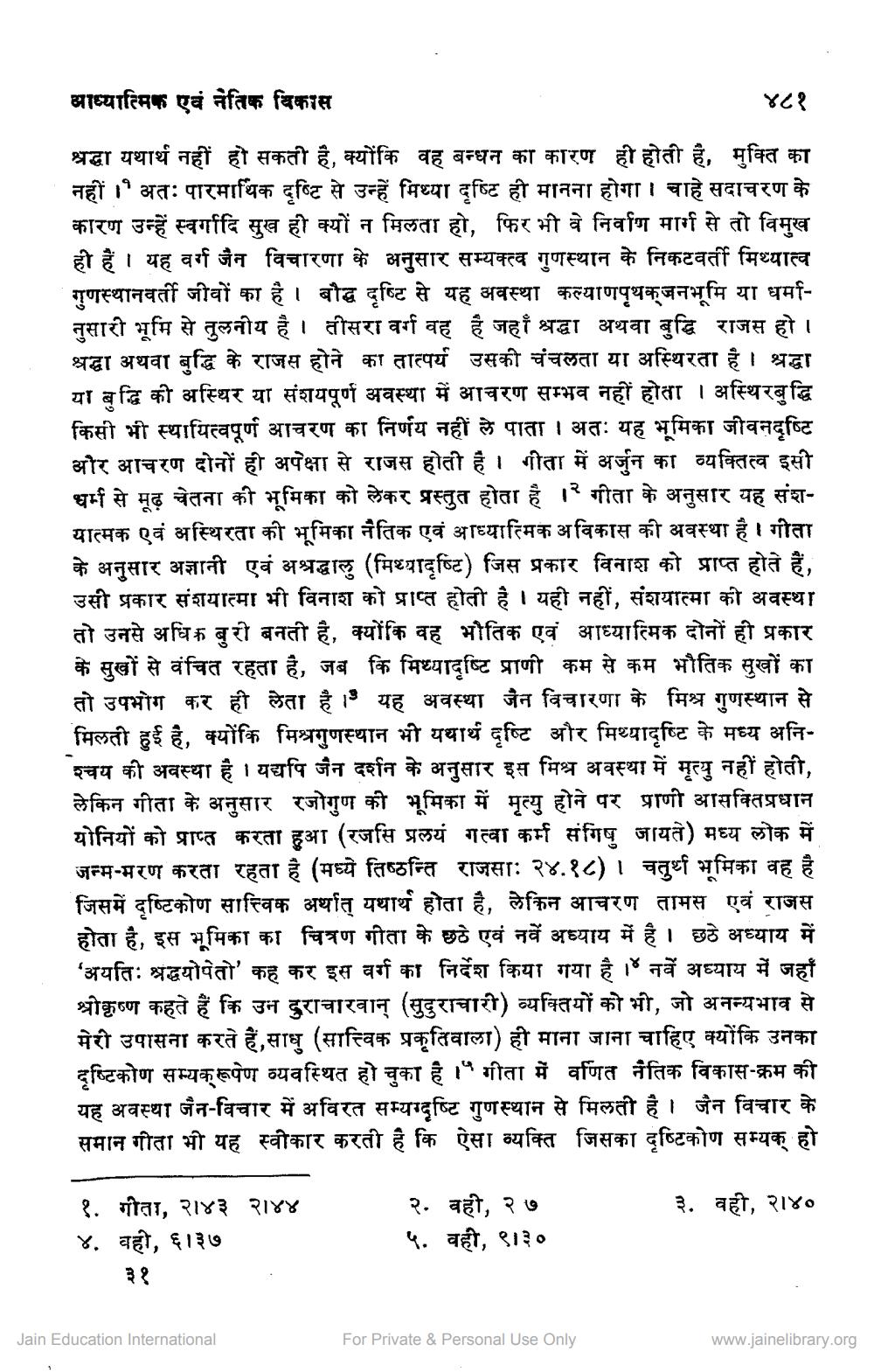________________
आध्यात्मिक एवं नैतिक विकास
४८१
श्रद्धा यथार्थ नहीं हो सकती है, क्योंकि वह बन्धन का कारण ही होती है, मुक्ति का नहीं।' अतः पारमार्थिक दृष्टि से उन्हें मिथ्या दृष्टि ही मानना होगा। चाहे सदाचरण के कारण उन्हें स्वर्गादि सुख ही क्यों न मिलता हो, फिर भी वे निर्वाण मार्ग से तो विमुख ही हैं । यह वर्ग जैन विचारणा के अनुसार सम्यक्त्व गुणस्थान के निकटवर्ती मिथ्यात्व गुणस्थानवी जीवों का है। बौद्ध दृष्टि से यह अवस्था कल्याणपृथक्जनभूमि या धर्मानुसारी भूमि से तुलनीय है। तीसरा वर्ग वह है जहाँ श्रद्धा अथवा बुद्धि राजस हो । श्रद्धा अथवा बुद्धि के राजस होने का तात्पर्य उसकी चंचलता या अस्थिरता है। श्रद्धा या बुद्धि की अस्थिर या संशयपूर्ण अवस्था में आचरण सम्भव नहीं होता । अस्थिरबुद्धि किसी भी स्थायित्वपूर्ण आचरण का निर्णय नहीं ले पाता । अतः यह भूमिका जीवनदृष्टि
और आचरण दोनों ही अपेक्षा से राजस होती है। गीता में अर्जुन का व्यक्तित्व इसी धर्म से मूढ़ चेतना की भूमिका को लेकर प्रस्तुत होता है । गीता के अनुसार यह संशयात्मक एवं अस्थिरता की भूमिका नैतिक एवं आध्यात्मिक अविकास की अवस्था है। गीता के अनुसार अज्ञानी एवं अश्रद्धालु (मिथ्यादृष्टि) जिस प्रकार विनाश को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार संशयात्मा भी विनाश को प्राप्त होती है । यही नहीं, संशयात्मा की अवस्था तो उनसे अधिक बुरी बनती है, क्योंकि वह भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार के सुखों से वंचित रहता है, जब कि मिथ्यादृष्टि प्राणी कम से कम भौतिक सुखों का तो उपभोग कर ही लेता है। यह अवस्था जैन विचारणा के मिश्र गुणस्थान से मिलती हुई है, क्योंकि मिश्रगुणस्थान भी यथार्थ दृष्टि और मिथ्यादृष्टि के मध्य अनिश्चय की अवस्था है । यद्यपि जैन दर्शन के अनुसार इस मिश्र अवस्था में मृत्यु नहीं होती, लेकिन गीता के अनुसार रजोगुण की भूमिका में मृत्यु होने पर प्राणी आसक्तिप्रधान योनियों को प्राप्त करता हुआ (रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते) मध्य लोक में जन्म-मरण करता रहता है (मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः २४.१८)। चतुर्थ भूमिका वह है जिसमें दृष्टिकोण सात्त्विक अर्थात् यथार्थ होता है, लेकिन आचरण तामस एवं राजस होता है, इस भूमिका का चित्रण गीता के छठे एवं नवें अध्याय में है। छठे अध्याय में 'अयतिः श्रद्धयोपेतो' कह कर इस वर्ग का निर्देश किया गया है। नवें अध्याय में जहाँ श्रीकृष्ण कहते हैं कि उन दुराचारवान् (सुदुराचारी) व्यक्तियों को भी, जो अनन्यभाव से मेरी उपासना करते हैं,साधु (सात्त्विक प्रकृतिवाला) ही माना जाना चाहिए क्योंकि उनका दृष्टिकोण सम्यक्रूपेण व्यवस्थित हो चुका है। गीता में वर्णित नैतिक विकास-क्रम की यह अवस्था जैन-विचार में अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान से मिलती है। जैन विचार के समान गीता भी यह स्वीकार करती है कि ऐसा व्यक्ति जिसका दृष्टिकोण सम्यक् हो
३. वही, २।४०
१. गीता, २।४३ २।४४ ४. वही, ६।३७
२. वही, २७ ५. वही, ९।३०
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org