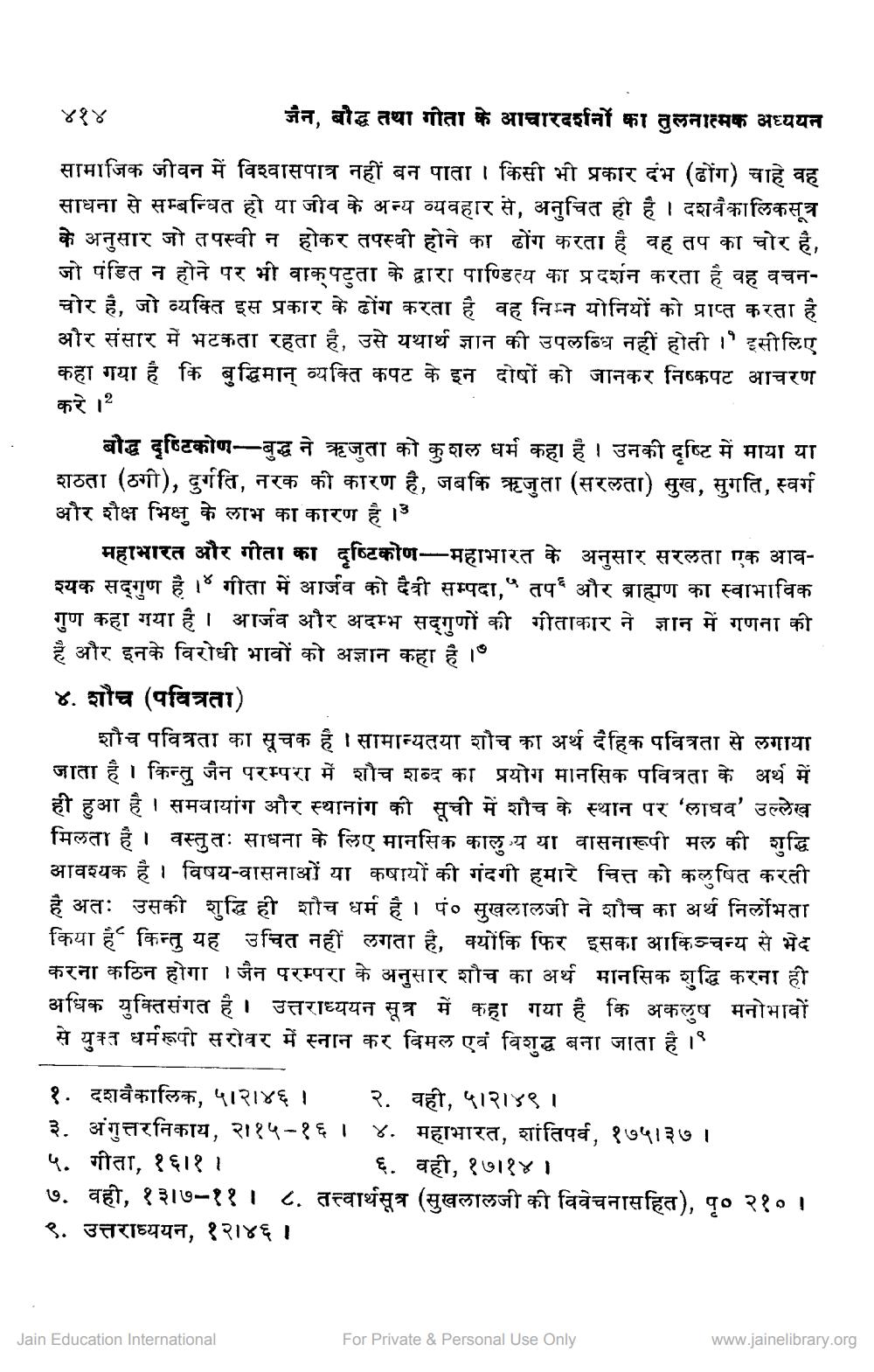________________
४१४
जैन, बौद्ध तथा गोता के आचारदर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन
सामाजिक जीवन में विश्वासपात्र नहीं बन पाता । किसी भी प्रकार दंभ ( ढोंग) चाहे वह साधना से सम्बन्धित हो या जीव के अन्य व्यवहार से, अनुचित ही है । दशवैकालिकसूत्र के अनुसार जो तपस्वी न होकर तपस्वी होने का ढोंग करता है वह तप का चोर है, जो पंडित न होने पर भी वाक्पटुता के द्वारा पाण्डित्य का प्रदर्शन करता है वह वचनचोर हैं, जो व्यक्ति इस प्रकार के ढोंग करता है वह निम्न योनियों को प्राप्त करता है और संसार में भटकता रहता है, उसे यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती ।" इसीलिए कहा गया है कि बुद्धिमान् व्यक्ति कपट के इन दोषों को जानकर निष्कपट आचरण करे | 2
बौद्ध दृष्टिकोण -- बुद्ध ने ऋजुता को कुशल धर्म कहा है । उनकी दृष्टि में माया या शठता ( ठगी), दुर्गति, नरक की कारण है, जबकि ऋजुता ( सरलता) सुख, सुगति, स्वर्ग और शैक्ष भिक्षु के लाभ का कारण है
महाभारत और गीता का दृष्टिकोण - महाभारत के श्यक सद्गुण है । * गीता में आर्जव को दैवी सम्पदा, ५ तप गुण कहा गया है। आर्जव और अदम्भ सद्गुणों की है और इनके विरोधी भावों को अज्ञान कहा है ।
४. शौच ( पवित्रता )
शौच पवित्रता का सूचक है । सामान्यतया शौच का अर्थ दैहिक पवित्रता से लगाया जाता है | किन्तु जैन परम्परा में शौच शब्द का प्रयोग मानसिक पवित्रता के अर्थ में ही हुआ है । समवायांग और स्थानांग की सूची में शौच के स्थान पर 'लाघव' उल्लेख मिलता है । वस्तुतः साधना के लिए मानसिक कालुग्य या वासनारूपी मल की शुद्धि आवश्यक है । विषय-वासनाओं या कषायों की गंदगी हमारे चित्त को कलुषित करती है अतः उसकी शुद्धि ही शौच धर्म है । पं० सुखलालजी किया है किन्तु यह उचित नहीं लगता है, क्योंकि फिर करना कठिन होगा | जैन परम्परा के अनुसार शौच का अर्थ अधिक युक्तिसंगत है । उत्तराध्ययन सूत्र में कहा गया है
युक्त धर्मरूपी सरोवर में स्नान कर विमल एवं विशुद्ध बना जाता है । "
१. दशवैकालिक, ५।२।४६ |
३. अंगुत्तरनिकाय, २०१५-१६ । ५. गीता, १६।१ ।
अनुसार सरलता एक आवऔर ब्राह्मण का स्वाभाविक गीताकार ने ज्ञान में गणना की
Jain Education International
२. वही, ५।२।४९ ।
ने
शौच का अर्थ निर्लोभता इसका आकिञ्चन्य से भेद मानसिक शुद्धि करना ही कि अकलुष मनोभावों
४.
६. वही, १७।१४ ।
७. वही, १३।७-११ । ८. तत्त्वार्थ सूत्र ( सुखलालजी की विवेचनासहित), पृ० २१० ।
९. उत्तराध्ययन, १२।४६ ।
महाभारत, शांतिपर्व, १७५।३७ ।
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org