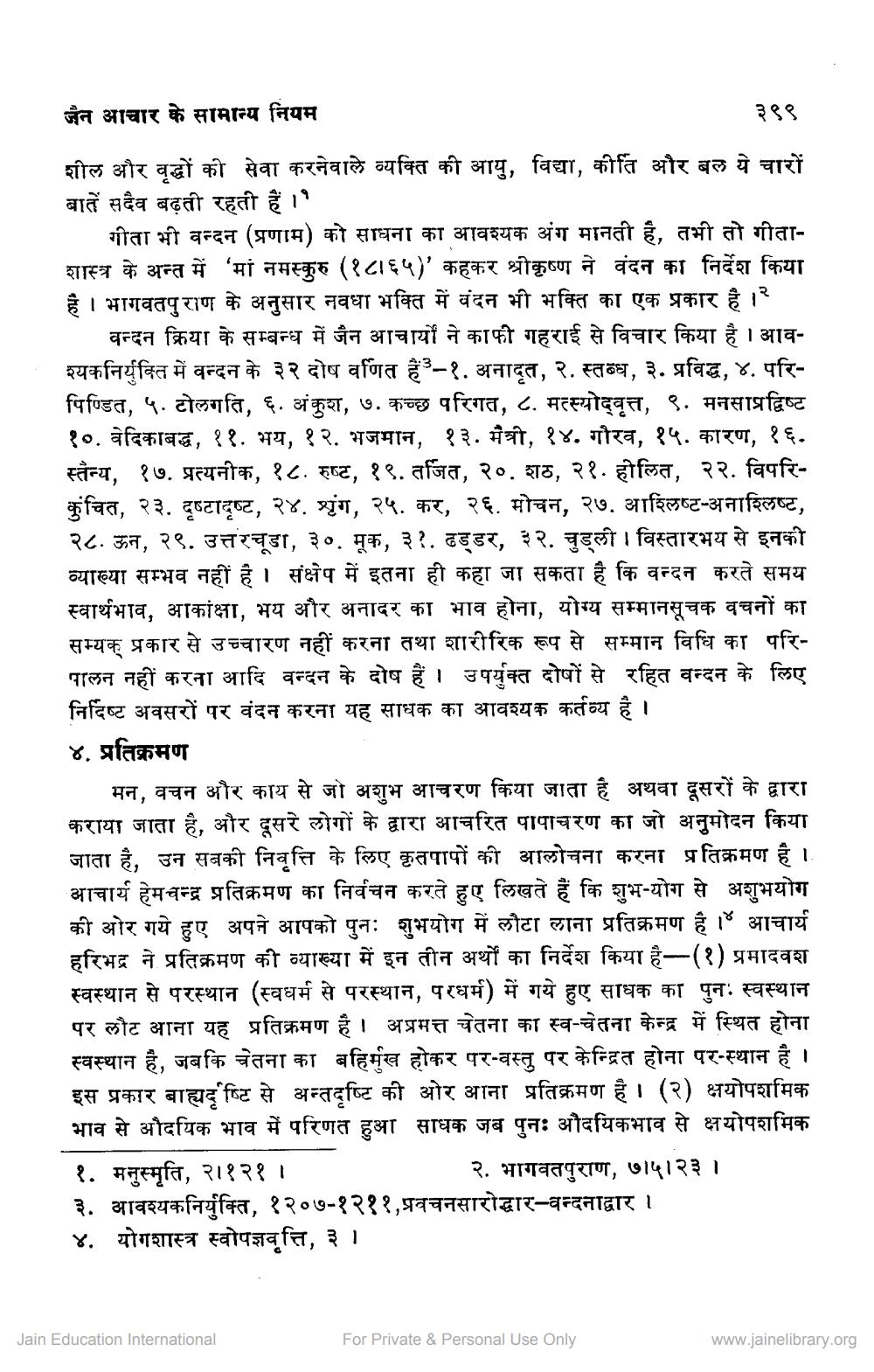________________
जैन आचार के सामान्य नियम
३९९
शील और वृद्धों की सेवा करनेवाले व्यक्ति की आयु, विद्या, कीर्ति और बल ये चारों बातें सदैव बढ़ती रहती हैं।'
गीता भी वन्दन (प्रणाम) को साधना का आवश्यक अंग मानती है, तभी तो गीताशास्त्र के अन्त में 'मां नमस्कुरु (१८।६५)' कहकर श्रीकृष्ण ने वंदन का निर्देश किया है । भागवतपुराण के अनुसार नवधा भक्ति में वंदन भी भक्ति का एक प्रकार है ।२ ___ वन्दन क्रिया के सम्बन्ध में जैन आचार्यों ने काफी गहराई से विचार किया है । आवश्यकनियुक्ति में वन्दन के ३२ दोष वणित हैं3-१. अनादृत, २. स्तब्ध, ३. प्रविद्ध, ४. परिपिण्डित, ५. टोलगति, ६. अंकुश, ७. कच्छ परिगत, ८. मत्स्योवृत्त, ९. मनसाप्रद्विष्ट १०. वेदिकाबद्ध, ११. भय, १२. भजमान, १३. मैत्री, १४. गौरव, १५. कारण, १६. स्तैन्य, १७. प्रत्यनीक, १८. रुष्ट, १९. तजित, २०. शठ, २१. हीलित, २२. विपरिकुंचित, २३. दृष्टादृष्ट, २४. शृंग, २५. कर, २६. मोचन, २७. आश्लिष्ट-अनाश्लिष्ट, २८. ऊन, २९. उत्तरचूडा, ३०. मूक, ३१. ढड्डर, ३२. चुड्ली । विस्तारभय से इनकी व्याख्या सम्भव नहीं है। संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है कि वन्दन करते समय स्वार्थभाव, आकांक्षा, भय और अनादर का भाव होना, योग्य सम्मानसूचक वचनों का सम्यक् प्रकार से उच्चारण नहीं करना तथा शारीरिक रूप से सम्मान विधि का परिपालन नहीं करना आदि वन्दन के दोष हैं । उपर्युक्त दोषों से रहित वन्दन के लिए निर्दिष्ट अवसरों पर वंदन करना यह साधक का आवश्यक कर्तव्य है । ४. प्रतिक्रमण __मन, वचन और काय से जो अशुभ आचरण किया जाता है अथवा दूसरों के द्वारा कराया जाता है, और दूसरे लोगों के द्वारा आचरित पापाचरण का जो अनुमोदन किया जाता है, उन सबकी निवृत्ति के लिए कृतपापों की आलोचना करना प्रतिक्रमण है । आचार्य हेमचन्द्र प्रतिक्रमण का निर्वचन करते हुए लिखते हैं कि शुभ-योग से अशुभयोग की ओर गये हुए अपने आपको पुनः शुभयोग में लौटा लाना प्रतिक्रमण है। आचार्य हरिभद्र ने प्रतिक्रमण की व्याख्या में इन तीन अर्थों का निर्देश किया है-(१) प्रमादवश स्वस्थान से परस्थान (स्वधर्म से परस्थान, परधर्म) में गये हुए साधक का पुनः स्वस्थान पर लौट आना यह प्रतिक्रमण है। अप्रमत्त चेतना का स्व-चेतना केन्द्र में स्थित होना स्वस्थान है, जबकि चेतना का बहिर्मुख होकर पर-वस्तु पर केन्द्रित होना पर-स्थान है । इस प्रकार बाह्यदृष्टि से अन्तदृष्टि की ओर आना प्रतिक्रमण है। (२) क्षयोपशमिक भाव से औदयिक भाव में परिणत हुआ साधक जब पुनः औदयिकभाव से क्षयोपशमिक १. मनुस्मृति, २।१२१ ।
२. भागवतपुराण, ७।५।२३ । ३. आवश्यकनियुक्ति, १२०७-१२११,प्रवचनसारोद्धार-वन्दनाद्वार । ४. योगशास्त्र स्वोपज्ञवृत्ति, ३ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org