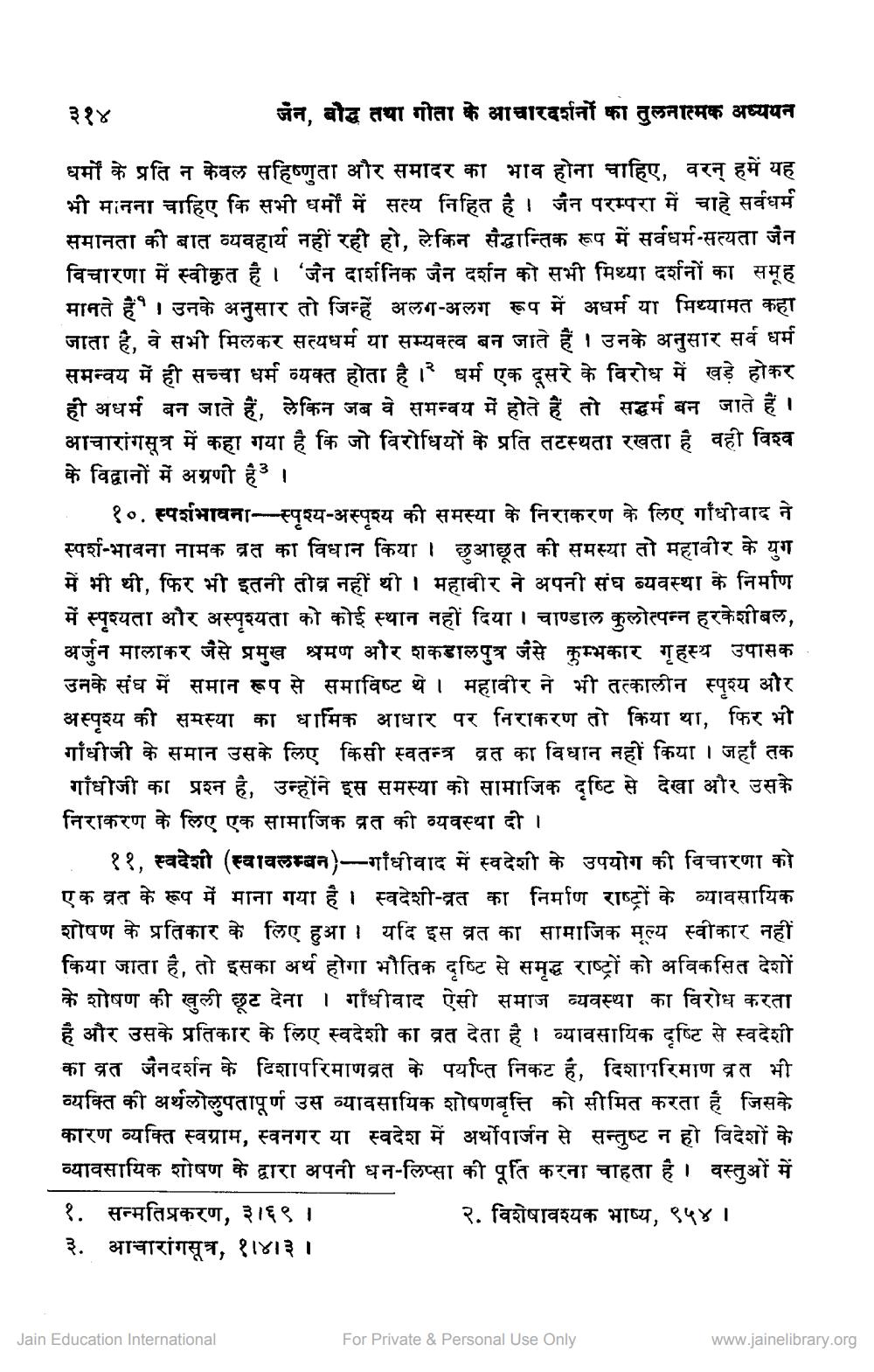________________
जन, बौद्ध तथा गोता के आचारवर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन
धर्मों के प्रति न केवल सहिष्णुता और समादर का भाव होना चाहिए, वरन् हमें यह भी मानना चाहिए कि सभी धर्मों में सत्य निहित है। जैन परम्परा में चाहे सर्वधर्म समानता की बात व्यवहार्य नहीं रही हो, लेकिन सैद्धान्तिक रूप में सर्वधर्म-सत्यता जैन विचारणा में स्वीकृत है । 'जैन दार्शनिक जैन दर्शन को सभी मिथ्या दर्शनों का समूह मानते हैं । उनके अनुसार तो जिन्हें अलग-अलग रूप में अधर्म या मिथ्यामत कहा जाता है, वे सभी मिलकर सत्यधर्म या सम्यक्त्व बन जाते हैं । उनके अनुसार सर्व धर्म समन्वय में ही सच्चा धर्म व्यक्त होता है । धर्म एक दूसरे के विरोध में खड़े होकर ही अधर्म बन जाते हैं, लेकिन जब वे समन्वय में होते हैं तो सद्धर्म बन जाते हैं । आचारांगसूत्र में कहा गया है कि जो विरोधियों के प्रति तटस्थता रखता है वही विश्व के विद्वानों में अग्रणी है ।
१०. स्पर्शभावना-स्पृश्य-अस्पृश्य की समस्या के निराकरण के लिए गाँधीवाद ने स्पर्श-भावना नामक व्रत का विधान किया। छुआछूत की समस्या तो महावीर के युग में भी थी, फिर भी इतनी तीव्र नहीं थी। महावीर ने अपनी संघ ब्यवस्था के निर्माण में स्पृश्यता और अस्पृश्यता को कोई स्थान नहीं दिया। चाण्डाल कुलोत्पन्न हरकेशीबल, अर्जुन मालाकर जैसे प्रमुख श्रमण और शकडालपुत्र जैसे कुम्भकार गृहस्थ उपासक उनके संघ में समान रूप से समाविष्ट थे। महावीर ने भी तत्कालीन स्पृश्य और अस्पृश्य की समस्या का धार्मिक आधार पर निराकरण तो किया था, फिर भी गांधीजी के समान उसके लिए किसी स्वतन्त्र व्रत का विधान नहीं किया । जहाँ तक गांधीजी का प्रश्न है, उन्होंने इस समस्या को सामाजिक दृष्टि से देखा और उसके निराकरण के लिए एक सामाजिक व्रत की व्यवस्था दी ।
११, स्वदेशी (स्वावलम्बन)-गांधीवाद में स्वदेशी के उपयोग की विचारणा को एक व्रत के रूप में माना गया है। स्वदेशी-व्रत का निर्माण राष्ट्रों के व्यावसायिक शोषण के प्रतिकार के लिए हुआ। यदि इस व्रत का सामाजिक मूल्य स्वीकार नहीं किया जाता है, तो इसका अर्थ होगा भौतिक दृष्टि से समृद्ध राष्ट्रों को अविकसित देशों के शोषण की खुली छूट देना । गाँधीवाद ऐसी समाज व्यवस्था का विरोध करता है और उसके प्रतिकार के लिए स्वदेशी का व्रत देता है । व्यावसायिक दृष्टि से स्वदेशी का व्रत जैनदर्शन के दिशापरिमाणवत के पर्याप्त निकट है, दिशापरिमाण व्रत भी व्यक्ति की अर्थलोलुपतापूर्ण उस व्यावसायिक शोषणबृत्ति को सीमित करता है जिसके कारण व्यक्ति स्वग्राम, स्वनगर या स्वदेश में अर्थोपार्जन से सन्तुष्ट न हो विदेशों के व्यावसायिक शोषण के द्वारा अपनी धन-लिप्सा की पूर्ति करना चाहता है। वस्तुओं में १. सन्मतिप्रकरण, ३।६९ ।
२. विशेषावश्यक भाष्य, ९५४ । ३. आचारांगसूत्र, ११४।३ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org