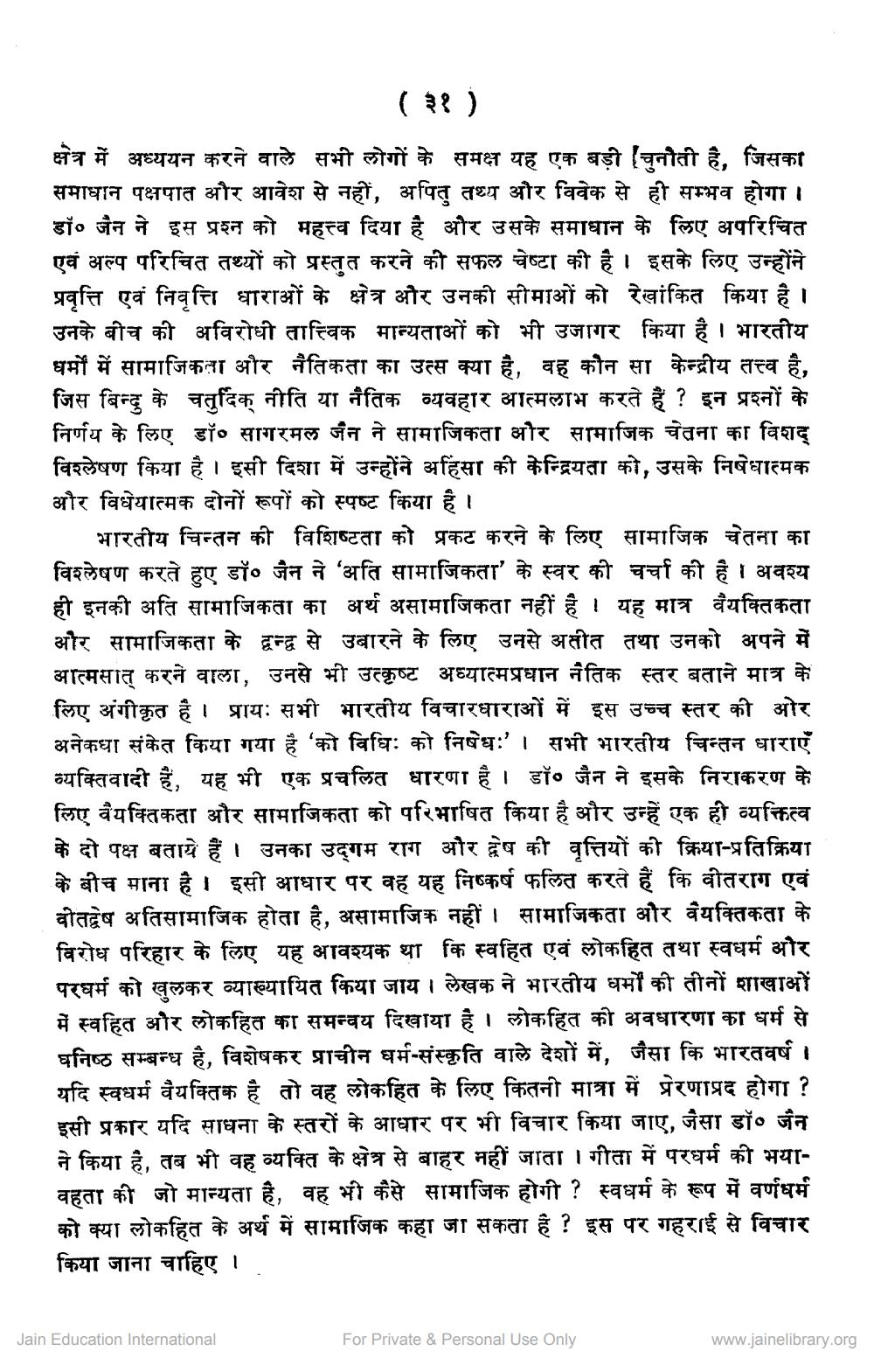________________
( ३१ )
क्षेत्र में अध्ययन करने वाले सभी लोगों के समक्ष यह एक बड़ी चुनौती है, जिसका समाधान पक्षपात और आवेश से नहीं, अपितु तथ्य और विवेक से ही सम्भव होगा । डॉ० जैन ने इस प्रश्न को महत्त्व दिया है और उसके समाधान के लिए अपरिचित एवं अल्प परिचित तथ्यों को प्रस्तुत करने की सफल चेष्टा की है । इसके लिए उन्होंने प्रवृत्ति एवं निवृत्ति धाराओं के क्षेत्र और उनकी सीमाओं को रेखांकित किया है । उनके बीच की अविरोधी तात्त्विक मान्यताओं को भी उजागर किया है । भारतीय धर्मों में सामाजिकता और नैतिकता का उत्स क्या है, वह कौन सा केन्द्रीय तत्त्व है, जिस बिन्दु के चतुर्दिक् नीति या नैतिक व्यवहार आत्मलाभ करते हैं ? इन प्रश्नों के निर्णय के लिए डॉ० सागरमल जैन ने सामाजिकता और सामाजिक चेतना का विशद् विश्लेषण किया है । इसी दिशा में उन्होंने अहिंसा की केन्द्रियता को, उसके निषेधात्मक और विधेयात्मक दोनों रूपों को स्पष्ट किया है ।
सामाजिक चेतना का
चर्चा की है । अवश्य यह मात्र वैयक्तिकता तथा उनको अपने में
भारतीय चिन्तन की विशिष्टता को प्रकट करने के लिए विश्लेषण करते हुए डॉ० जैन ने 'अति सामाजिकता' के स्वर की ही इनकी अति सामाजिकता का अर्थ असामाजिकता नहीं है । और सामाजिकता के द्वन्द्व से उबारने के लिए उनसे असीत आत्मसात् करने वाला, उनसे भी उत्कृष्ट अध्यात्मप्रधान नैतिक स्तर बताने मात्र के लिए अंगीकृत है । प्रायः सभी भारतीय विचारधाराओं में इस उच्च स्तर की ओर अनेकधा संकेत किया गया है ' को विधिः को निषेधः ' । सभी भारतीय चिन्तन धाराएँ व्यक्तिवादी हैं, यह भी एक प्रचलित धारणा है । डॉ० जैन ने इसके निराकरण के लिए वैयक्तिकता और सामाजिकता को परिभाषित किया है और उन्हें एक ही व्यक्तित्व के दो पक्ष बताये हैं । उनका उद्गम राग और द्वेष की वृत्तियों की क्रिया-प्रतिक्रिया के बीच माना है । इसी आधार पर वह यह निष्कर्ष फलित करते हैं कि वीतराग एवं तद्वेष अतिसामाजिक होता है, असामाजिक नहीं । सामाजिकता और वैयक्तिकता के विरोध परिहार के लिए यह आवश्यक था कि स्वहित एवं लोकहित तथा स्वधर्म और परधर्म को खुलकर व्याख्यायित किया जाय । लेखक ने भारतीय धर्मों की तीनों शाखाओं में स्वहित और लोकहित का समन्वय दिखाया है । लोकहित की अवधारणा का धर्म से घनिष्ठ सम्बन्ध है, विशेषकर प्राचीन धर्म-संस्कृति वाले देशों में, जैसा कि भारतवर्ष । यदि स्वधर्म वैयक्तिक है तो वह लोकहित के लिए कितनी मात्रा में प्रेरणाप्रद होगा ? इसी प्रकार यदि साधना के स्तरों के आधार पर भी विचार किया जाए, जैसा डॉ० जैन ने किया है, तब भी वह व्यक्ति के क्षेत्र से बाहर नहीं जाता । गीता में परधर्म की भयावहता की जो मान्यता है, वह भी कैसे सामाजिक होगी ? स्वधर्म के रूप में वर्णधर्म को क्या लोकहित के अर्थ में सामाजिक कहा जा सकता है ? इस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org