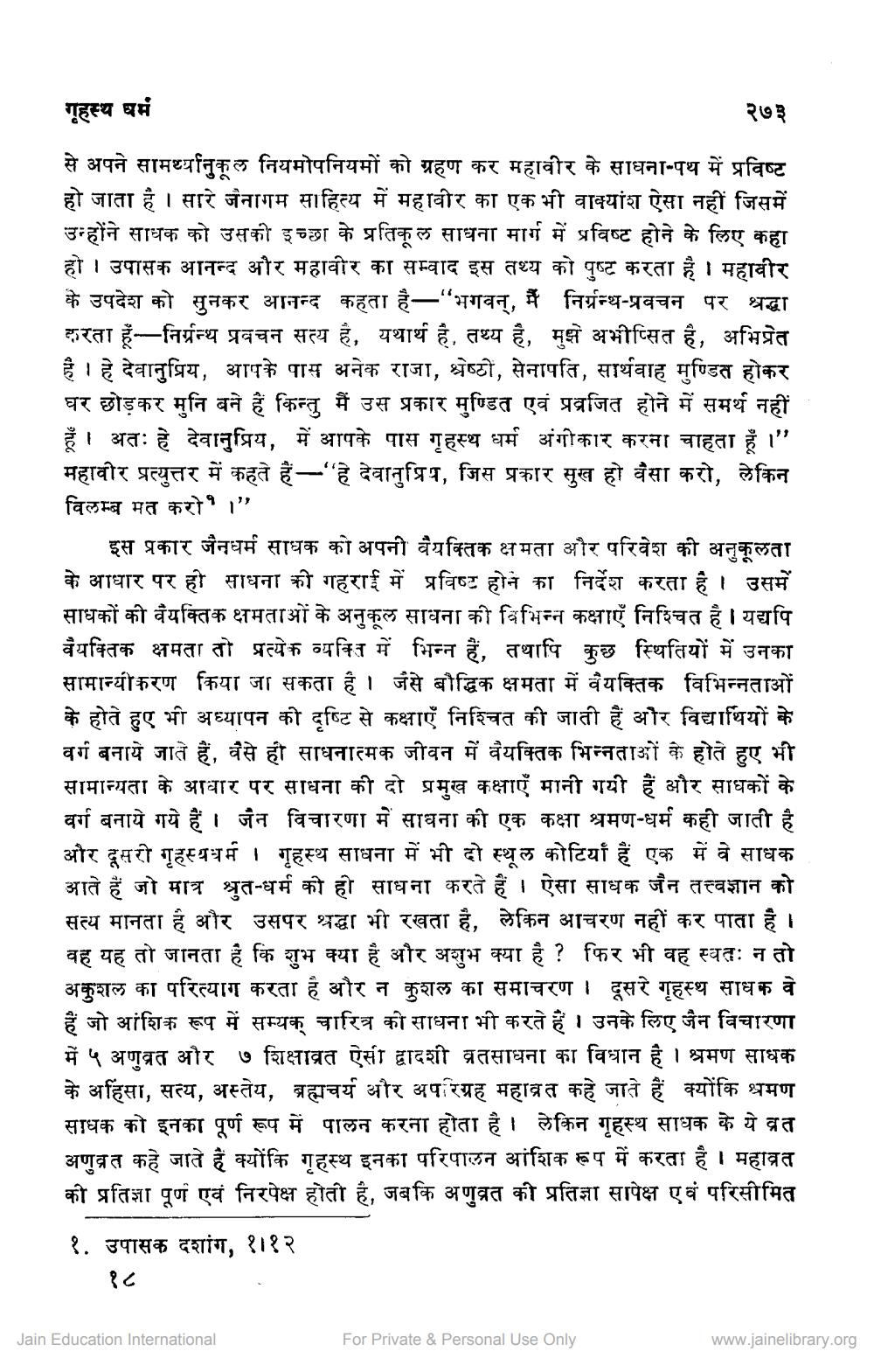________________
गृहस्थ धर्म
२७३
से अपने सामर्थ्यानुकूल नियमोपनियमों को ग्रहण कर महावीर के साधना-पथ में प्रविष्ट हो जाता है । सारे जैनागम साहित्य में महावीर का एक भी वाक्यांश ऐसा नहीं जिसमें उन्होंने साधक को उसकी इच्छा के प्रतिकूल साधना मार्ग में प्रविष्ट होने के लिए कहा हो । उपासक आनन्द और महावीर का सम्वाद इस तथ्य को पुष्ट करता है। महावीर के उपदेश को सुनकर आनन्द कहता है-“भगवन्, मैं निर्ग्रन्थ-प्रवचन पर श्रद्धा करता हूँ-निर्ग्रन्थ प्रवचन सत्य है, यथार्थ है, तथ्य है, मुझे अभीप्सित है, अभिप्रेत है । हे देवानुप्रिय, आपके पास अनेक राजा, श्रेष्ठी, सेनापति, सार्थवाह मुण्डित होकर घर छोड़कर मुनि बने हैं किन्तु मैं उस प्रकार मुण्डित एवं प्रव्रजित होने में समर्थ नहीं हूँ। अतः हे देवानुप्रिय, में आपके पास गृहस्थ धर्म अंगीकार करना चाहता हूँ।" महावीर प्रत्युत्तर में कहते हैं- 'हे देवानुप्रिप, जिस प्रकार सुख हो वैसा करो, लेकिन विलम्ब मत करो।"
इस प्रकार जैनधर्म साधक को अपनी वैयक्तिक क्षमता और परिवेश की अनुकूलता के आधार पर ही साधना की गहराई में प्रविष्ट होने का निर्देश करता है। उसमें साधकों की वैयक्तिक क्षमताओं के अनुकूल साधना की विभिन्न कक्षाएँ निश्चित है । यद्यपि वैयक्तिक क्षमता तो प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न हैं, तथापि कुछ स्थितियों में उनका सामान्यीकरण किया जा सकता है। जैसे बौद्धिक क्षमता में वैयक्तिक विभिन्नताओं के होते हुए भी अध्यापन की दृष्टि से कक्षाएँ निश्चित की जाती हैं और विद्यार्थियों के वर्ग बनाये जाते हैं, वैसे ही साधनात्मक जीवन में वैयक्तिक भिन्नताओं के होते हुए भी सामान्यता के आधार पर साधना की दो प्रमुख कक्षाएँ मानी गयी है और साधकों के वर्ग बनाये गये हैं। जैन विचारणा में साधना की एक कक्षा श्रमण-धर्म कही जाती है और दूसरी गृहस्यधर्म । गृहस्थ साधना में भी दो स्थूल कोटियाँ हैं एक में वे साधक आते हैं जो मात्र श्रुत-धर्म को ही साधना करते हैं । ऐसा साधक जैन तत्त्वज्ञान को सत्य मानता है और उसपर श्रद्धा भी रखता है, लेकिन आचरण नहीं कर पाता है । वह यह तो जानता है कि शुभ क्या है और अशुभ क्या है ? फिर भी वह स्वतः न तो अकुशल का परित्याग करता है और न कुशल का समाचरण । दूसरे गृहस्थ साधक वे हैं जो आंशिक रूप में सम्यक् चारित्र को साधना भी करते हैं । उनके लिए जैन विचारणा में ५ अणुव्रत और ७ शिक्षाव्रत ऐसी द्वादशी व्रतसाधना का विधान है । श्रमण साधक के अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह महाव्रत कहे जाते हैं क्योंकि श्रमण साधक को इनका पूर्ण रूप में पालन करना होता है। लेकिन गृहस्थ साधक के ये व्रत अणुव्रत कहे जाते हैं क्योंकि गृहस्थ इनका परिपालन आंशिक रूप में करता है । महाव्रत की प्रतिज्ञा पूर्ण एवं निरपेक्ष होती है, जबकि अणुव्रत की प्रतिज्ञा सापेक्ष एवं परिसीमित १. उपासक दशांग, १।१२
१८
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org