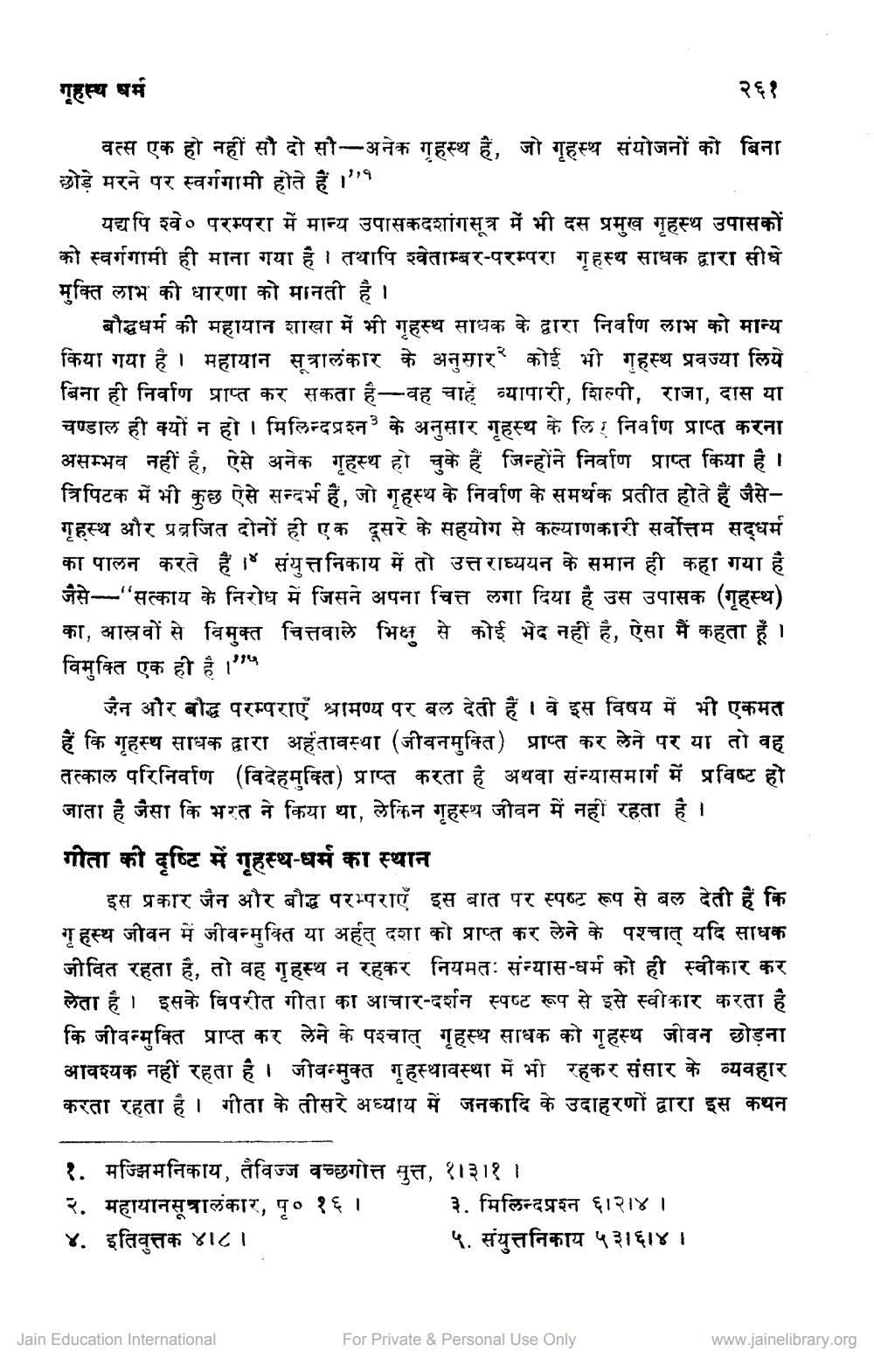________________
गृहस्य धर्म
२६१
वत्स एक हो नहीं सौ दो सौ-अनेक गृहस्थ है, जो गृहस्थ संयोजनों को बिना छोड़े मरने पर स्वर्गगामी होते हैं।"१
यद्यपि श्वे० परम्परा में मान्य उपासकदशांगसूत्र में भी दस प्रमुख गृहस्थ उपासकों को स्वर्गगामी ही माना गया है । तथापि श्वेताम्बर-परम्परा गृहस्थ साधक द्वारा सीधे मुक्ति लाभ की धारणा को मानती है ।
बौद्धधर्म की महायान शाखा में भी गृहस्थ साधक के द्वारा निर्वाण लाभ को मान्य किया गया है। महायान सूत्रालंकार के अनुसार कोई भी गृहस्थ प्रवज्या लिये बिना ही निर्वाण प्राप्त कर सकता है-वह चाहे व्यापारी, शिल्पी, राजा, दास या चण्डाल ही क्यों न हो । मिलिन्दप्रश्न' के अनुसार गृहस्थ के लिए निर्वाण प्राप्त करना असम्भव नहीं है, ऐसे अनेक गृहस्थ हो चुके हैं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया है। त्रिपिटक में भी कुछ ऐसे सन्दर्भ हैं, जो गृहस्थ के निर्वाण के समर्थक प्रतीत होते हैं जैसेगृहस्थ और प्रव्रजित दोनों ही एक दूसरे के सहयोग से कल्याणकारी सर्वोत्तम सद्धर्म का पालन करते हैं। संयुत्त निकाय में तो उत्तराध्ययन के समान ही कहा गया है जैसे-"सत्काय के निरोध में जिसने अपना चित्त लगा दिया है उस उपासक (गृहस्थ) का, आस्रवों से विमुक्त चित्तवाले भिक्षु से कोई भेद नहीं है, ऐसा मैं कहता हूँ। विमुक्ति एक ही है ।"५
जैन और बौद्ध परम्पराएँ श्रामण्य पर बल देती हैं । वे इस विषय में भी एकमत हैं कि गृहस्थ साधक द्वारा अहंतावस्था (जीवनमुक्ति) प्राप्त कर लेने पर या तो वह तत्काल परिनिर्वाण (विदेहमक्ति) प्राप्त करता है अथवा संन्यासमार्ग में प्रविष्ट हो जाता है जैसा कि भरत ने किया था, लेकिन गृहस्थ जीवन में नहीं रहता है। गीता की दृष्टि में गृहस्थ-धर्म का स्थान
__ इस प्रकार जैन और बौद्ध परम्पराएँ इस बात पर स्पष्ट रूप से बल देती हैं कि गृहस्थ जीवन में जीवन्मुक्ति या अर्हत् दशा को प्राप्त कर लेने के पश्चात् यदि साधक जीवित रहता है, तो वह गृहस्थ न रहकर नियमतः संन्यास-धर्म को ही स्वीकार कर लेता है। इसके विपरीत गीता का आचार-दर्शन स्पष्ट रूप से इसे स्वीकार करता है कि जीवन्मुक्ति प्राप्त कर लेने के पश्चात् गृहस्थ साधक को गृहस्थ जीवन छोड़ना आवश्यक नहीं रहता है । जीवन्मुक्त गृहस्थावस्था में भी रहकर संसार के व्यवहार करता रहता है। गीता के तीसरे अध्याय में जनकादि के उदाहरणों द्वारा इस कथन
१. मज्झिमनिकाय, तैविज्ज वच्छगोत्त सुत्त, १।३।१ । २. महायानसूत्रालंकार, पृ० १६ । ३. मिलिन्दप्रश्न ६।२।४ । ४. इतिवृत्तक ४।८।
५. संयुत्तनिकाय ५३१६।४ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org