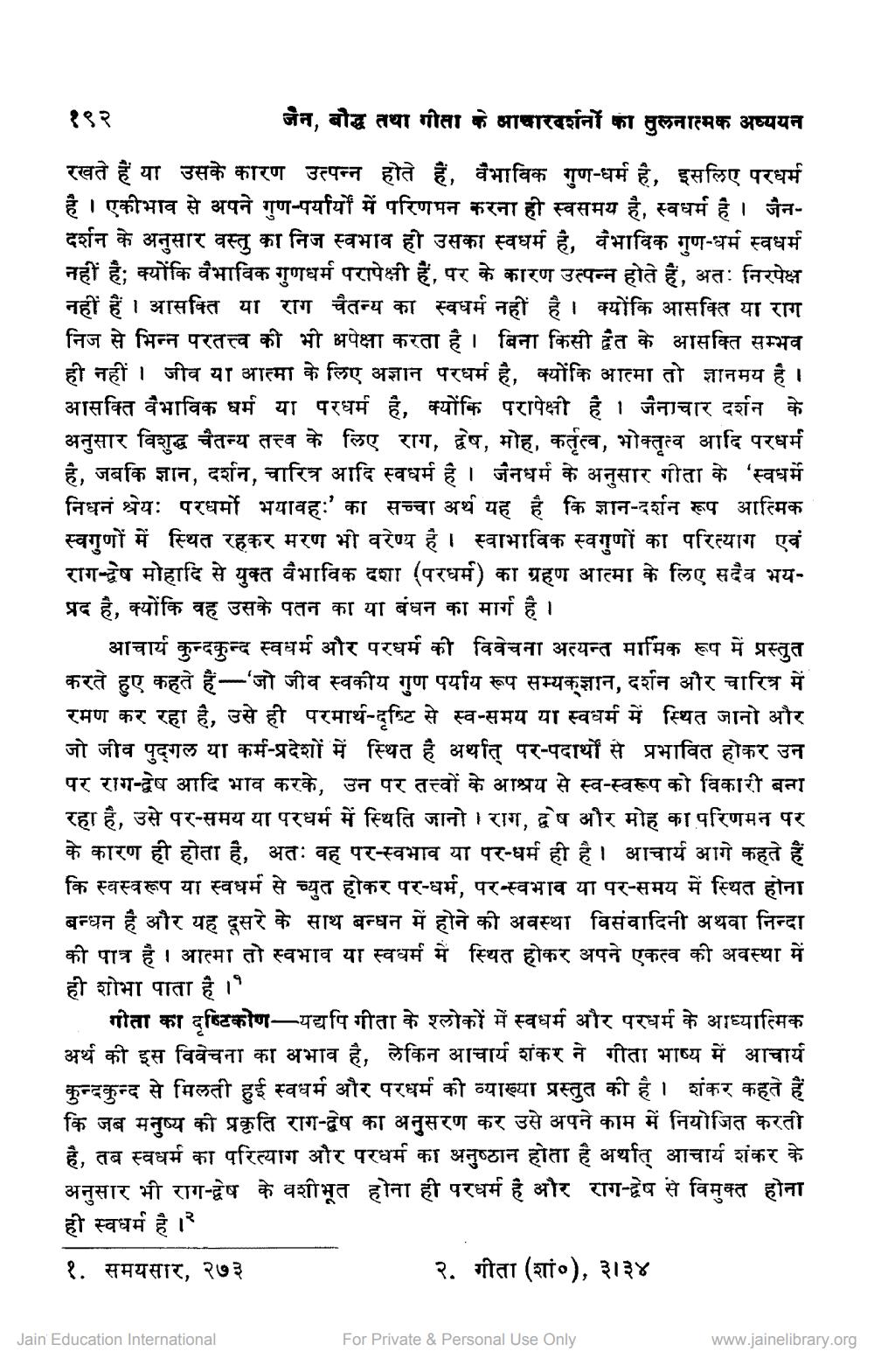________________
१९२
जैन, बौद्ध तथा गीता के आचारवर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन
रखते हैं या उसके कारण उत्पन्न होते हैं, वैभाविक गुण-धर्म है, इसलिए परधर्म है । एकीभाव से अपने गुण-
पर्यों में परिणमन करना ही स्वसमय है, स्वधर्म है। जैनदर्शन के अनुसार वस्तु का निज स्वभाव ही उसका स्वधर्म है, वैभाविक गुण-धर्म स्वधर्म नहीं है; क्योंकि वैभाविक गुणधर्म परापेक्षी हैं, पर के कारण उत्पन्न होते हैं, अतः निरपेक्ष नहीं हैं । आसक्ति या राग चैतन्य का स्वधर्म नहीं है। क्योंकि आसक्ति या राग निज से भिन्न परतत्त्व की भी अपेक्षा करता है। बिना किसी द्वैत के आसक्ति सम्भव ही नहीं। जीव या आत्मा के लिए अज्ञान परधर्म है, क्योंकि आत्मा तो ज्ञानमय है । आसक्ति वैभाविक धर्म या परधर्म है, क्योंकि परापेक्षी है । जैनाचार दर्शन के अनुसार विशुद्ध चैतन्य तत्त्व के लिए राग, द्वेष, मोह, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि परधर्म है, जबकि ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि स्वधर्म है । जैनधर्म के अनुसार गीता के 'स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः' का सच्चा अर्थ यह है कि ज्ञान-दर्शन रूप आत्मिक स्वगुणों में स्थित रहकर मरण भी वरेण्य है। स्वाभाविक स्वगुणों का परित्याग एवं राग-द्वेष मोहादि से युक्त वैभाविक दशा (परधर्म) का ग्रहण आत्मा के लिए सदैव भयप्रद है, क्योंकि वह उसके पतन का या बंधन का मार्ग है।
आचार्य कुन्दकुन्द स्वधर्म और परधर्म की विवेचना अत्यन्त मार्मिक रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं-'जो जीव स्वकीय गुण पर्याय रूप सम्यज्ञान, दर्शन और चारित्र में रमण कर रहा है, उसे ही परमार्थ-दृष्टि से स्व-समय या स्वधर्म में स्थित जानो और जो जीव पुद्गल या कर्म-प्रदेशों में स्थित है अर्थात् पर-पदार्थों से प्रभावित होकर उन पर राग-द्वेष आदि भाव करके, उन पर तत्त्वों के आश्रय से स्व-स्वरूप को विकारी बना रहा है, उसे पर-समय या परधर्म में स्थिति जानो । राग, द्वष और मोह का परिणमन पर के कारण ही होता है, अतः वह पर-स्वभाव या पर-धर्म ही है। आचार्य आगे कहते हैं कि स्वस्वरूप या स्वधर्म से च्युत होकर पर-धर्म, पर-स्वभाव या पर-समय में स्थित होना बन्धन है और यह दूसरे के साथ बन्धन में होने की अवस्था विसंवादिनी अथवा निन्दा की पात्र है । आत्मा तो स्वभाव या स्वधर्म में स्थित होकर अपने एकत्व की अवस्था में ही शोभा पाता है।'
गीता का दृष्टिकोण-यद्यपि गीता के श्लोकों में स्वधर्म और परधर्म के आध्यात्मिक अर्थ की इस विवेचना का अभाव है, लेकिन आचार्य शंकर ने गीता भाष्य में आचार्य कुन्दकुन्द से मिलती हुई स्वधर्म और परधर्म को व्याख्या प्रस्तुत की है। शंकर कहते हैं कि जब मनुष्य की प्रकृति राग-द्वेष का अनुसरण कर उसे अपने काम में नियोजित करती है, तब स्वधर्म का परित्याग और परधर्म का अनुष्ठान होता है अर्थात् आचार्य शंकर के अनुसार भी राग-द्वेष के वशीभूत होना ही परधर्म है और राग-द्वेष से विमुक्त होना ही स्वधर्म है। १. समयसार, २७३
२. गीता (शां०), ३।३४
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org