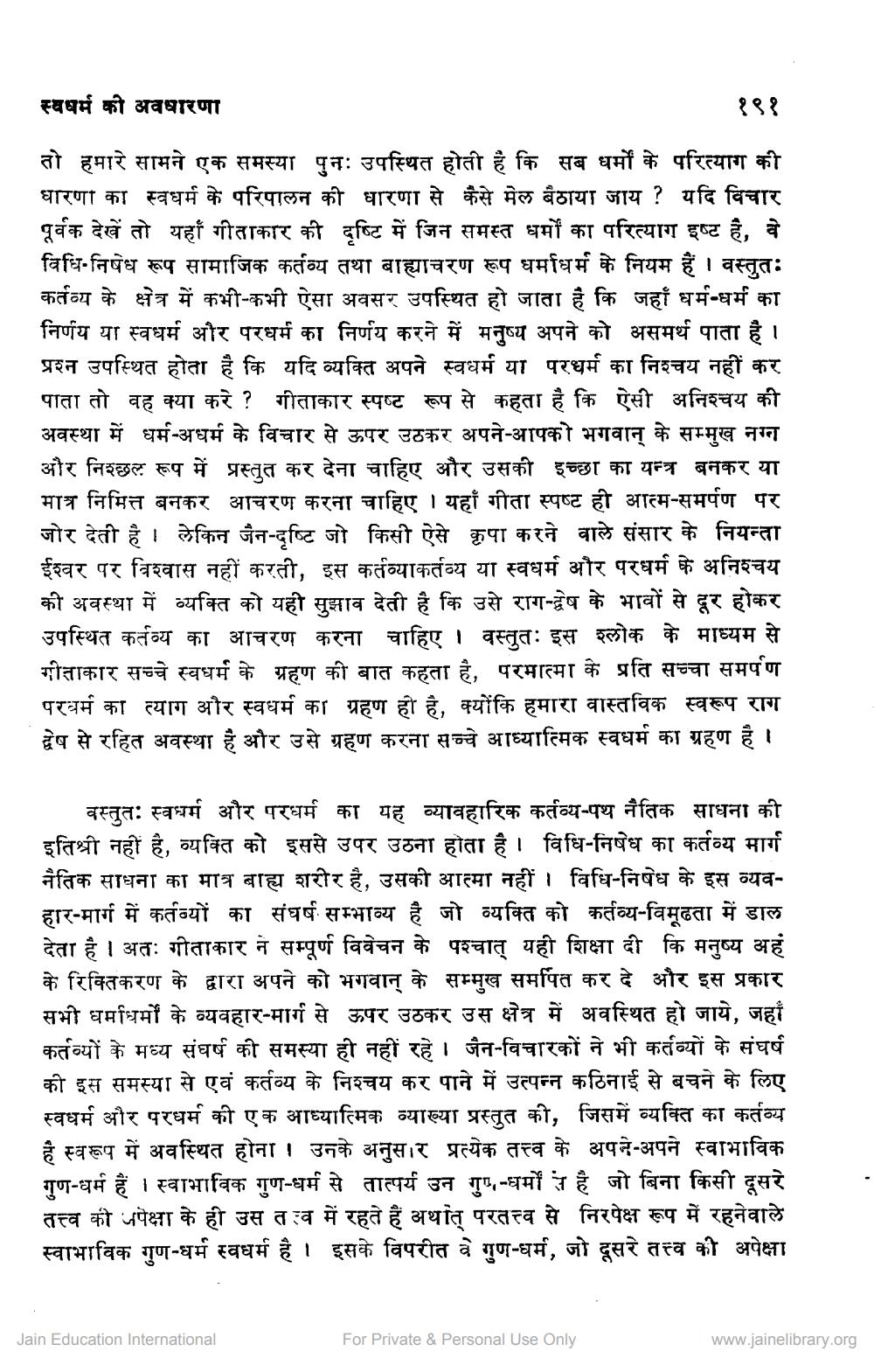________________
स्वधर्म की अवधारणा
१९१
तो हमारे सामने एक समस्या पुनः उपस्थित होती है कि सब धर्मों के परित्याग की धारणा का स्वधर्म के परिपालन की धारणा से कैसे मेल बैठाया जाय ? यदि विचार पूर्वक देखें तो यहाँ गीताकार की दृष्टि में जिन समस्त धर्मों का परित्याग इष्ट है, वे विधि-निषेध रूप सामाजिक कर्तव्य तथा बाह्याचरण रूप धर्माधर्म के नियम हैं । वस्तुतः कर्तव्य के क्षेत्र में कभी-कभी ऐसा अवसर उपस्थित हो जाता है कि जहाँ धर्म-धर्म का निर्णय या स्वधर्म और परधर्म का निर्णय करने में मनुष्य अपने को असमर्थ पाता है । प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि व्यक्ति अपने स्वधर्म या परधर्म का निश्चय नहीं कर पाता तो वह क्या करे ? गीताकार स्पष्ट रूप से कहता है कि ऐसी अनिश्चय की अवस्था में धर्म-अधर्म के विचार से ऊपर उठकर अपने-आपको भगवान् के सम्मुख नग्न और निश्छल रूप में प्रस्तुत कर देना चाहिए और उसकी इच्छा का यन्त्र बनकर या मात्र निमित्त बनकर आचरण करना चाहिए । यहाँ गीता स्पष्ट ही आत्म-समर्पण पर जोर देती है । लेकिन जैन-दृष्टि जो किसी ऐसे कृपा करने वाले संसार के नियन्ता ईश्वर पर विश्वास नहीं करती, इस कर्तव्याकर्तव्य या स्वधर्म और परधर्म के अनिश्चय की अवस्था में व्यक्ति को यही सुझाव देती है कि उसे राग-द्वेष के भावों से दूर होकर उपस्थित कर्तव्य का आचरण करना चाहिए । वस्तुतः इस श्लोक के माध्यम से गीताकार सच्चे स्वधर्म के ग्रहण की बात कहता है, परमात्मा के प्रति सच्चा समर्पण परवर्म का त्याग और स्वधर्म का ग्रहण ही है, क्योंकि हमारा वास्तविक स्वरूप राग द्वेष से रहित अवस्था है और उसे ग्रहण करना सच्चे आध्यात्मिक स्वधर्म का ग्रहण है ।
वस्तुतः स्वधर्म और परधर्म का यह व्यावहारिक कर्तव्य-पथ नैतिक साधना की इतिश्री नहीं है, व्यक्ति को इससे उपर उठना होता है। विधि-निषेध का कर्तव्य मार्ग नैतिक साधना का मात्र बाह्य शरीर है, उसकी आत्मा नहीं। विधि-निषेध के इस व्यवहार-मार्ग में कर्तव्यों का संघर्ष सम्भाव्य है जो व्यक्ति को कर्तव्य-विमूढता में डाल देता है । अतः गीताकार ने सम्पूर्ण विवेचन के पश्चात् यही शिक्षा दी कि मनुष्य अहं के रिक्तिकरण के द्वारा अपने को भगवान् के सम्मुख समर्पित कर दे और इस प्रकार सभी धर्माधर्मों के व्यवहार-मार्ग से ऊपर उठकर उस क्षेत्र में अवस्थित हो जाये, जहाँ कर्तव्यों के मध्य संघर्ष की समस्या ही नहीं रहे। जैन-विचारकों ने भी कर्तव्यों के संघर्ष की इस समस्या से एवं कर्तव्य के निश्चय कर पाने में उत्पन्न कठिनाई से बचने के लिए स्वधर्म और परधर्म की एक आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत की, जिसमें व्यक्ति का कर्तव्य है स्वरूप में अवस्थित होना । उनके अनुसार प्रत्येक तत्त्व के अपने-अपने स्वाभाविक गुण-धर्म हैं । स्वाभाविक गुण-धर्म से तात्पर्य उन गुण-धर्मों में है जो बिना किसी दूसरे तत्त्व की अपेक्षा के ही उस तत्व में रहते हैं अर्थात् परतत्त्व से निरपेक्ष रूप में रहनेवाले स्वाभाविक गुण-धर्म स्वधर्म है । इसके विपरीत वे गुण-धर्म, जो दूसरे तत्त्व की अपेक्षा
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org