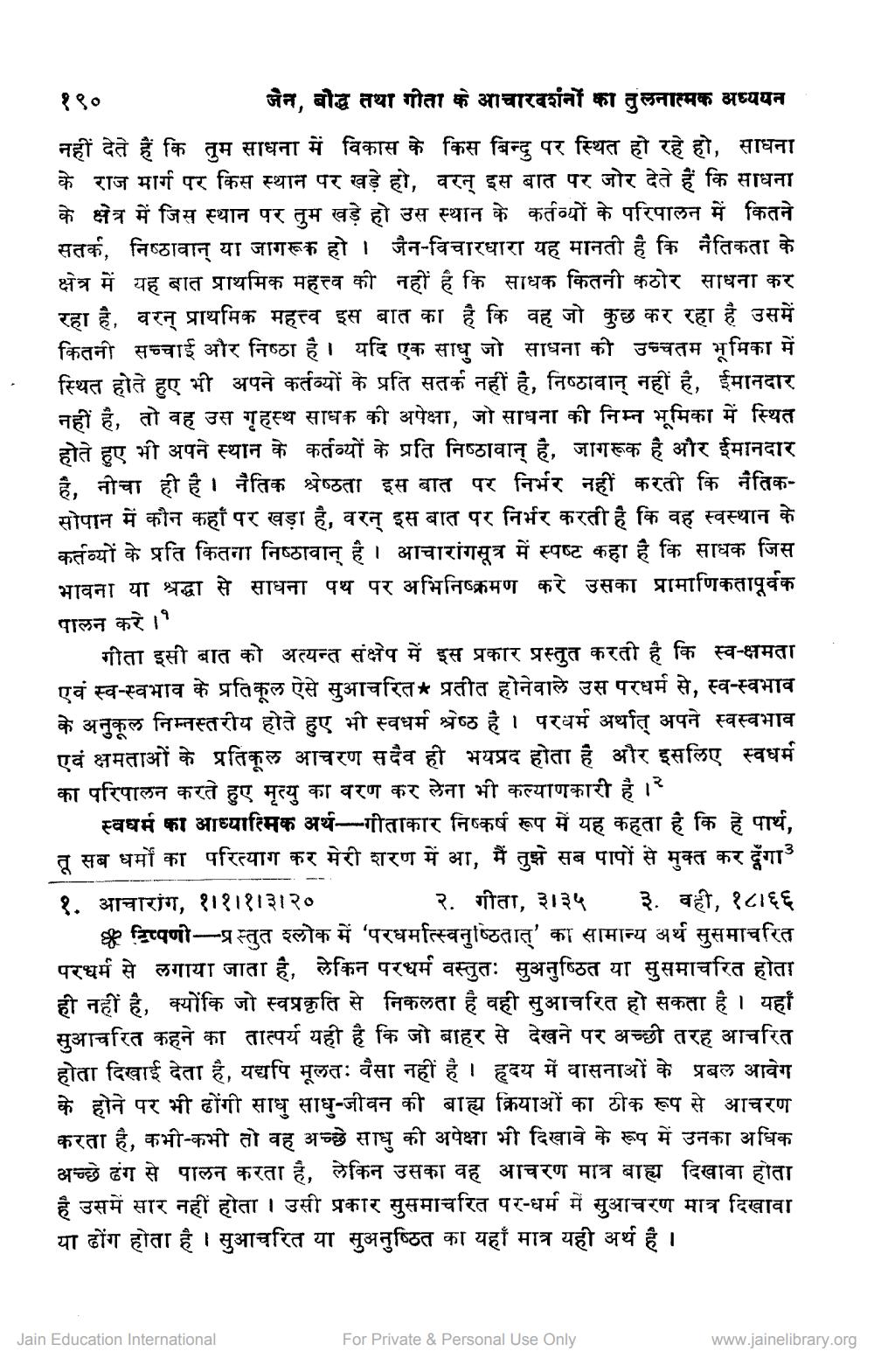________________
१९०
जैन, बौद्ध तथा गीता के आचारवशनों का तुलनात्मक अध्ययन नहीं देते हैं कि तुम साधना में विकास के किस बिन्दु पर स्थित हो रहे हो, साधना के राज मार्ग पर किस स्थान पर खड़े हो, वरन् इस बात पर जोर देते हैं कि साधना के क्षेत्र में जिस स्थान पर तुम खड़े हो उस स्थान के कर्तव्यों के परिपालन में कितने सतर्क, निष्ठावान् या जागरूक हो । जैन-विचारधारा यह मानती है कि नैतिकता के क्षेत्र में यह बात प्राथमिक महत्त्व की नहीं है कि साधक कितनी कठोर साधना कर रहा है, वरन् प्राथमिक महत्त्व इस बात का है कि वह जो कुछ कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई और निष्ठा है। यदि एक साधु जो साधना को उच्चतम भूमिका में स्थित होते हुए भी अपने कर्तव्यों के प्रति सतर्क नहीं है, निष्ठावान् नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो वह उस गृहस्थ साधक की अपेक्षा, जो साधना की निम्न भूमिका में स्थित होते हुए भी अपने स्थान के कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान् है, जागरूक है और ईमानदार है, नीचा ही है। नैतिक श्रेष्ठता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि नैतिकसोपान में कौन कहाँ पर खड़ा है, वरन् इस बात पर निर्भर करती है कि वह स्वस्थान के कर्तव्यों के प्रति कितना निष्ठावान् है। आचारांगसूत्र में स्पष्ट कहा है कि साधक जिस भावना या श्रद्धा से साधना पथ पर अभिनिष्क्रमण करे उसका प्रामाणिकतापूर्वक पालन करे।
गीता इसी बात को अत्यन्त संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत करती है कि स्व-क्षमता एवं स्व-स्वभाव के प्रतिकूल ऐसे सुआचरित* प्रतीत होनेवाले उस परधर्म से, स्व-स्वभाव के अनुकूल निम्नस्तरीय होते हुए भी स्वधर्म श्रेष्ठ है । परधर्म अर्थात् अपने स्वस्वभाव एवं क्षमताओं के प्रतिकूल आचरण सदैव ही भयप्रद होता है और इसलिए स्वधर्म का परिपालन करते हुए मृत्यु का वरण कर लेना भी कल्याणकारी है ।।
स्वधर्म का आध्यात्मिक अर्थ-गीताकार निष्कर्ष रूप में यह कहता है कि हे पार्थ, तू सब धर्मों का परित्याग कर मेरी शरण में आ, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा' १. आचारांग, १११।१।३।२० २. गीता, ३।३५ ३. वही, १८१६६
* टिप्पणी-प्रस्तुत श्लोक में 'परधर्मात्स्वनुष्ठितात्' का सामान्य अर्थ सुसमाचरित परधर्म से लगाया जाता है, लेकिन परधर्म वस्तुतः सुअनुष्ठित या सुसमाचरित होता ही नहीं है, क्योंकि जो स्वप्रकृति से निकलता है वही सुआचरित हो सकता है। यहाँ सुआचरित कहने का तात्पर्य यही है कि जो बाहर से देखने पर अच्छी तरह आचरित होता दिखाई देता है, यद्यपि मूलतः वैसा नहीं है । हृदय में वासनाओं के प्रबल आवेग के होने पर भी ढोंगी साधु साधु-जीवन की बाह्य क्रियाओं का ठीक रूप से आचरण करता है, कभी-कभी तो वह अच्छे साधु की अपेक्षा भी दिखावे के रूप में उनका अधिक अच्छे ढंग से पालन करता है, लेकिन उसका वह आचरण मात्र बाह्य दिखावा होता है उसमें सार नहीं होता । उसी प्रकार सुसमाचरित पर-धर्म में सुआचरण मात्र दिखावा या ढोंग होता है । सुआचरित या सुअनुष्ठित का यहाँ मात्र यही अर्थ है ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org