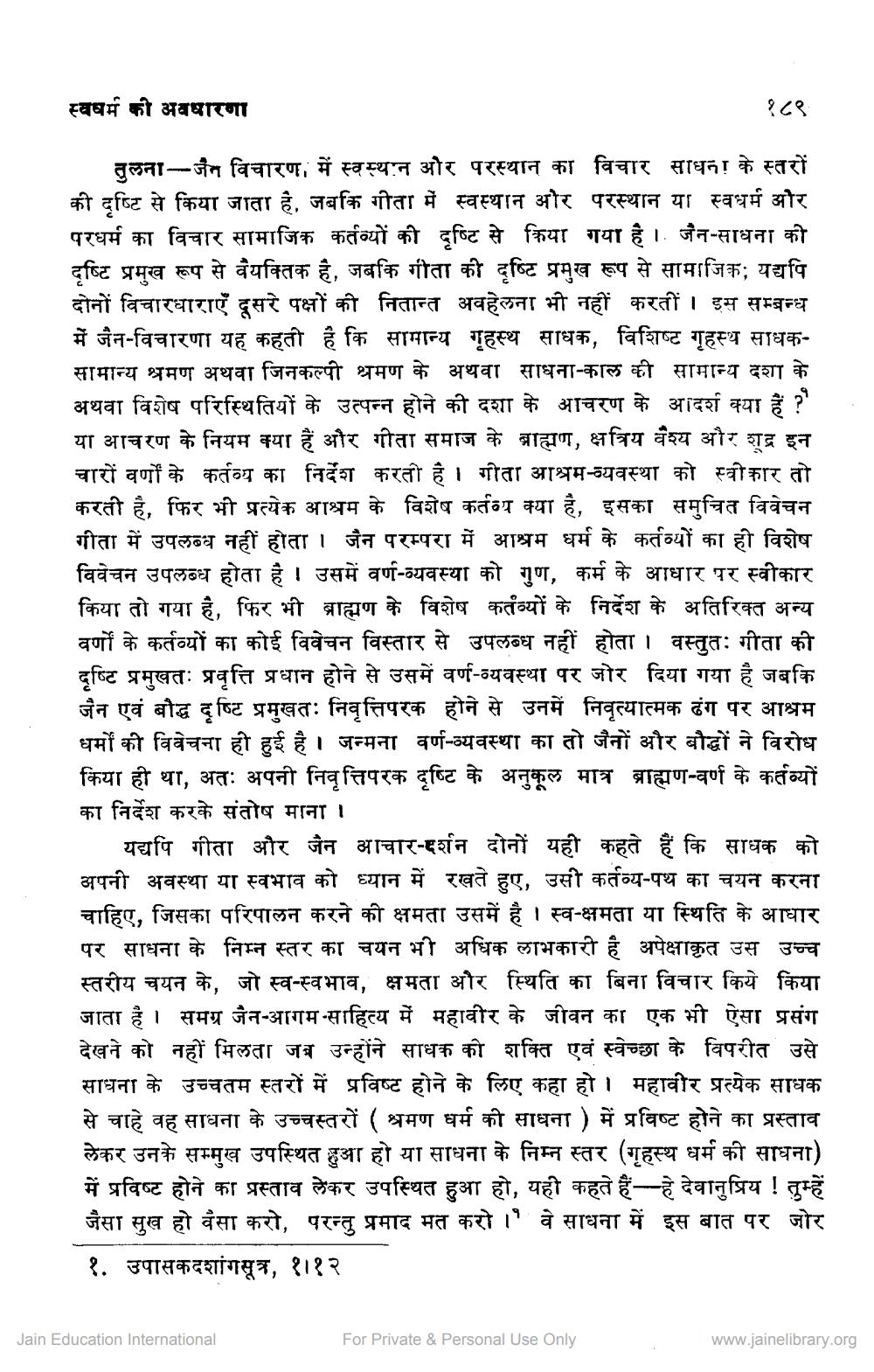________________
स्वधर्म की अवधारणा
१८९
तुलना-जैन विचारण, में स्वस्थान और परस्थान का विचार साधना के स्तरों की दृष्टि से किया जाता है, जबकि गीता में स्वस्थान और परस्थान या स्वधर्म और परधर्म का विचार सामाजिक कर्तव्यों की दृष्टि से किया गया है। जैन-साधना को दृष्टि प्रमुख रूप से वैयक्तिक है, जबकि गीता की दृष्टि प्रमुख रूप से सामाजिक; यद्यपि दोनों विचारधाराएँ दूसरे पक्षों की नितान्त अवहेलना भी नहीं करतीं। इस सम्बन्ध में जैन-विचारणा यह कहती है कि सामान्य गृहस्थ साधक, विशिष्ट गृहस्थ साधकसामान्य श्रमण अथवा जिनकल्पी श्रमण के अथवा साधना-काल की सामान्य दशा के अथवा विशेष परिस्थितियों के उत्पन्न होने की दशा के आचरण के आदर्श क्या हैं ? या आचरण के नियम क्या हैं और गीता समाज के ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारों वर्गों के कर्तव्य का निर्देश करती है। गीता आश्रम-व्यवस्था को स्वीकार तो करती है, फिर भी प्रत्येक आश्रम के विशेष कर्तव्य क्या है, इसका समुचित विवेचन गीता में उपलब्ध नहीं होता। जैन परम्परा में आश्रम धर्म के कर्तव्यों का ही विशेष विवेचन उपलब्ध होता है । उसमें वर्ण-व्यवस्था को गुण, कर्म के आधार पर स्वीकार किया तो गया है, फिर भी ब्राह्मण के विशेष कर्तव्यों के निर्देश के अतिरिक्त अन्य वर्गों के कर्तव्यों का कोई विवेचन विस्तार से उपलब्ध नहीं होता। वस्तुतः गीता की दृष्टि प्रमुखतः प्रवृत्ति प्रधान होने से उसमें वर्ण-व्यवस्था पर जोर दिया गया है जबकि जैन एवं बौद्ध दृष्टि प्रमुखतः निवृत्तिपरक होने से उनमें निवृत्यात्मक ढंग पर आश्रम धर्मों की विवेचना ही हुई है। जन्मना वर्ण-व्यवस्था का तो जैनों और बौद्धों ने विरोध किया ही था, अतः अपनी निवृत्तिपरक दृष्टि के अनुकूल मात्र ब्राह्मण-वर्ण के कर्तव्यों का निर्देश करके संतोष माना ।
यद्यपि गीता और जैन आचार-दर्शन दोनों यही कहते हैं कि साधक को अपनी अवस्था या स्वभाव को ध्यान में रखते हुए, उसी कर्तव्य-पथ का चयन करना चाहिए, जिसका परिपालन करने की क्षमता उसमें है । स्व-क्षमता या स्थिति के आधार पर साधना के निम्न स्तर का चयन भी अधिक लाभकारी है अपेक्षाकृत उस उच्च स्तरीय चयन के, जो स्व-स्वभाव, क्षमता और स्थिति का बिना विचार किये किया जाता है। समग्र जैन-आगम साहित्य में महावीर के जीवन का एक भी ऐसा प्रसंग देखने को नहीं मिलता जब उन्होंने साधक को शक्ति एवं स्वेच्छा के विपरीत उसे साधना के उच्चतम स्तरों में प्रविष्ट होने के लिए कहा हो। महावीर प्रत्येक साधक से चाहे वह साधना के उच्चस्तरों ( श्रमण धर्म की साधना ) में प्रविष्ट होने का प्रस्ताव लेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुआ हो या साधना के निम्न स्तर (गृहस्थ धर्म की साधना) में प्रविष्ट होने का प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुआ हो, यही कहते हैं-हे देवानुप्रिय ! तुम्हें जैसा सुख हो वैसा करो, परन्तु प्रमाद मत करो।' वे साधना में इस बात पर जोर १. उपासकदशांगसूत्र, १।१२
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org