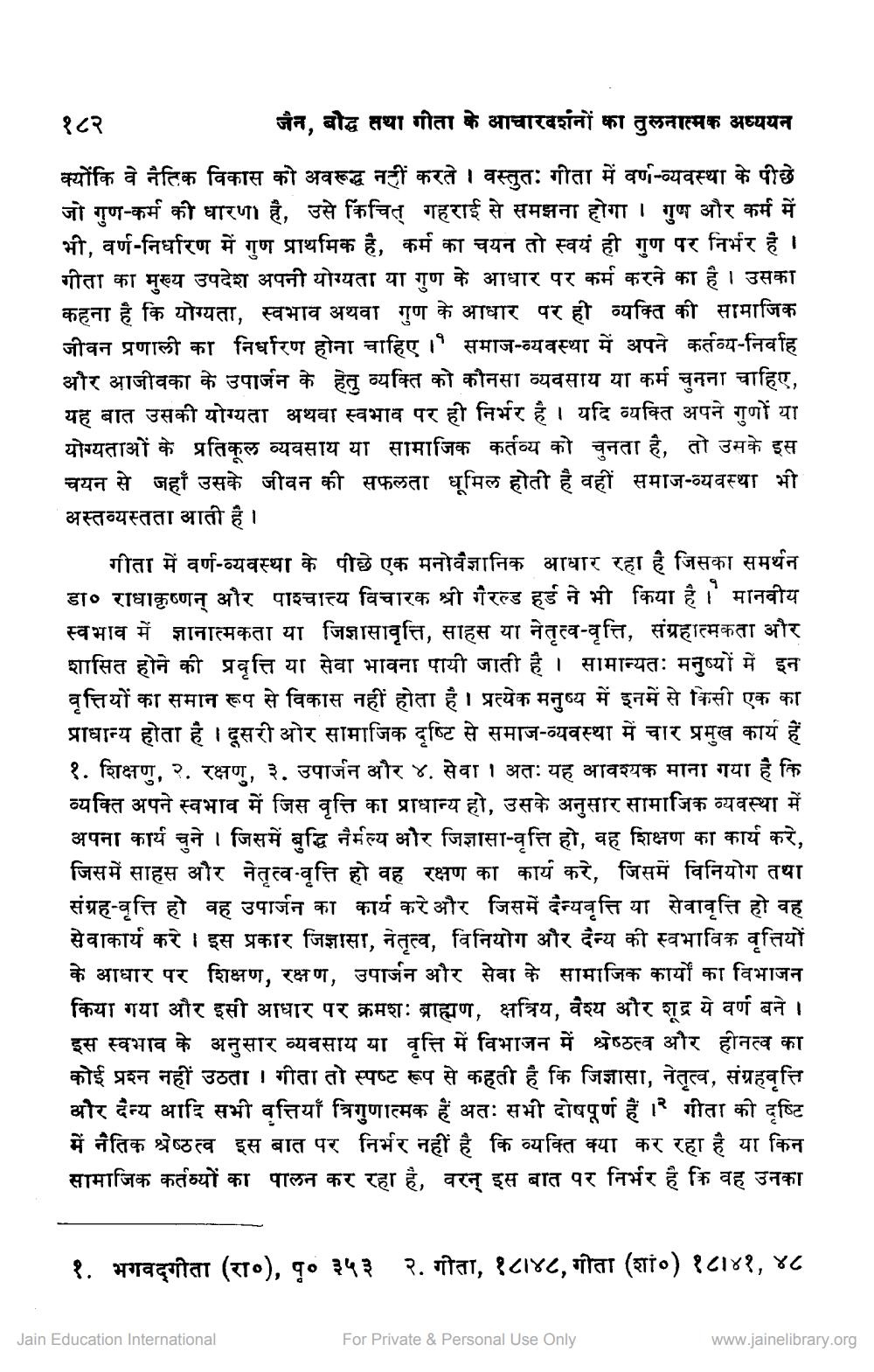________________
१८२
जैन, बौद्ध तथा गीता के आचारदर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन क्योंकि वे नैतिक विकास को अवरूद्ध नहीं करते । वस्तुतः गीता में वर्ण-व्यवस्था के पीछे जो गुण-कर्म की धारणा है, उसे किंचित् गहराई से समझना होगा । गुण और कर्म में भी, वर्ण-निर्धारण में गुण प्राथमिक है, कर्म का चयन तो स्वयं ही गुण पर निर्भर है । गीता का मुख्य उपदेश अपनी योग्यता या गुण के आधार पर कर्म करने का है । उसका कहना है कि योग्यता, स्वभाव अथवा गुण के आधार पर ही व्यक्ति की सामाजिक जीवन प्रणाली का निर्धारण होना चाहिए।' समाज-व्यवस्था में अपने कर्तव्य-निर्वाह
और आजीवका के उपार्जन के हेतु व्यक्ति को कौनसा व्यवसाय या कर्म चुनना चाहिए, यह बात उसकी योग्यता अथवा स्वभाव पर ही निर्भर है। यदि व्यक्ति अपने गुणों या योग्यताओं के प्रतिकूल व्यवसाय या सामाजिक कर्तव्य को चुनता है, तो उसके इस चयन से जहाँ उसके जीवन की सफलता धूमिल होती है वहीं समाज-व्यवस्था भी अस्तव्यस्तता आती है।
गीता में वर्ण-व्यवस्था के पीछे एक मनोवैज्ञानिक आधार रहा है जिसका समर्थन डा० राधाकृष्णन् और पाश्चात्त्य विचारक श्री गैरल्ड हर्ड ने भी किया है। मानवीय स्वभाव में ज्ञानात्मकता या जिज्ञासावृत्ति, साहस या नेतृत्व-वृत्ति, संग्रहात्मकता और शासित होने की प्रवृत्ति या सेवा भावना पायी जाती है । सामान्यतः मनुष्यों में इन वृत्तियों का समान रूप से विकास नहीं होता है। प्रत्येक मनुष्य में इनमें से किसी एक का प्राधान्य होता है । दूसरी ओर सामाजिक दृष्टि से समाज-व्यवस्था में चार प्रमुख कार्य हैं १. शिक्षणु, २. रक्षणु, ३. उपार्जन और ४. सेवा । अतः यह आवश्यक माना गया है कि व्यक्ति अपने स्वभाव में जिस वृत्ति का प्राधान्य हो, उसके अनुसार सामाजिक व्यवस्था में अपना कार्य चुने । जिसमें बुद्धि नैर्मल्य और जिज्ञासा-वृत्ति हो, वह शिक्षण का कार्य करे, जिसमें साहस और नेतृत्व-वृत्ति हो वह रक्षण का कार्य करे, जिसमें विनियोग तथा संग्रह-वृत्ति हो वह उपार्जन का कार्य करे और जिसमें दैन्यवृत्ति या सेवावृत्ति हो वह सेवाकार्य करे । इस प्रकार जिज्ञासा, नेतृत्व, विनियोग और दैन्य की स्वभाविक वृत्तियों के आधार पर शिक्षण, रक्षण, उपार्जन और सेवा के सामाजिक कार्यों का विभाजन किया गया और इसी आधार पर क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये वर्ण बने । इस स्वभाव के अनुसार व्यवसाय या वृत्ति में विभाजन में श्रेष्ठत्व और हीनत्व का कोई प्रश्न नहीं उठता । गीता तो स्पष्ट रूप से कहती है कि जिज्ञासा, नेतृत्व, संग्रहवृत्ति
और दैन्य आदि सभी वत्तियाँ त्रिगुणात्मक हैं अतः सभी दोषपूर्ण हैं ।२ गीता की दृष्टि में नैतिक श्रेष्ठत्व इस बात पर निर्भर नहीं है कि व्यक्ति क्या कर रहा है या किन सामाजिक कर्तव्यों का पालन कर रहा है, वरन् इस बात पर निर्भर है कि वह उनका
१. भगवद्गीता (रा०), पृ० ३५३ २. गीता, १८।४८, गीता (शां०) १८१४१, ४८
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org