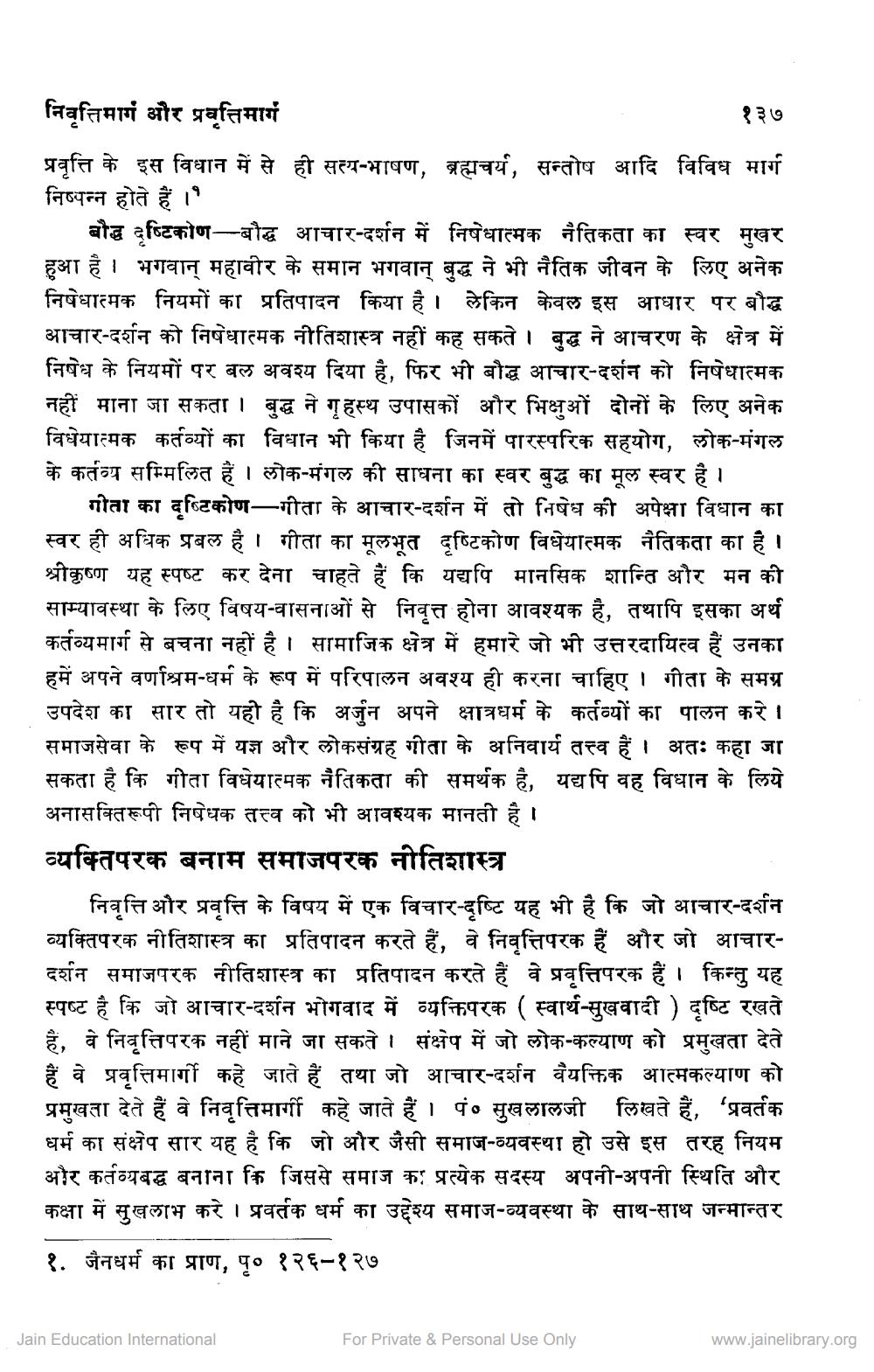________________
निवृत्तिमार्ग और प्रवृत्तिमार्ग
१३७ प्रवृत्ति के इस विधान में से ही सत्य-भाषण, ब्रह्मचर्य, सन्तोष आदि विविध मार्ग निष्पन्न होते हैं ।
बौद्ध दृष्टिकोण-बौद्ध आचार-दर्शन में निषेधात्मक नैतिकता का स्वर मुखर हुआ है । भगवान् महावीर के समान भगवान् बुद्ध ने भी नैतिक जीवन के लिए अनेक निषेधात्मक नियमों का प्रतिपादन किया है। लेकिन केवल इस आधार पर बौद्ध
आचार-दर्शन को निषेधात्मक नीतिशास्त्र नहीं कह सकते । बुद्ध ने आचरण के क्षेत्र में निषेध के नियमों पर बल अवश्य दिया है, फिर भी बौद्ध आचार-दर्शन को निषेधात्मक नहीं माना जा सकता। बुद्ध ने गृहस्थ उपासकों और भिक्षुओं दोनों के लिए अनेक विधेयात्मक कर्तव्यों का विधान भी किया है जिनमें पारस्परिक सहयोग, लोक-मंगल के कर्तव्य सम्मिलित हैं । लोक-मंगल की साधना का स्वर बुद्ध का मूल स्वर है।
गीता का दृष्टिकोण-गीता के आचार-दर्शन में तो निषेध की अपेक्षा विधान का स्वर ही अधिक प्रबल है । गीता का मूलभूत दृष्टिकोण विधेयात्मक नैतिकता का है । श्रीकृष्ण यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यद्यपि मानसिक शान्ति और मन की साम्यावस्था के लिए विषय-वासनाओं से निवृत्त होना आवश्यक है, तथापि इसका अर्थ कर्तव्यमार्ग से बचना नहीं है । सामाजिक क्षेत्र में हमारे जो भी उत्तरदायित्व हैं उनका हमें अपने वर्णाश्रम-धर्म के रूप में परिपालन अवश्य ही करना चाहिए । गीता के समग्र उपदेश का सार तो यही है कि अर्जुन अपने क्षात्रधर्म के कर्तव्यों का पालन करे । समाजसेवा के रूप में यज्ञ और लोकसंग्रह गीता के अनिवार्य तत्त्व हैं । अतः कहा जा सकता है कि गीता विधेयात्मक नैतिकता की समर्थक है, यद्यपि वह विधान के लिये अनासक्तिरूपी निषेधक तत्त्व को भी आवश्यक मानती है । व्यक्तिपरक बनाम समाजपरक नीतिशास्त्र
निवृत्ति और प्रवृत्ति के विषय में एक विचार-दृष्टि यह भी है कि जो आचार-दर्शन व्यक्तिपरक नीतिशास्त्र का प्रतिपादन करते हैं, वे निवृत्तिपरक हैं और जो आचारदर्शन समाजपरक नीतिशास्त्र का प्रतिपादन करते हैं वे प्रवृत्तिपरक हैं। किन्तु यह स्पष्ट है कि जो आचार-दर्शन भोगवाद में व्यक्तिपरक ( स्वार्थ-सुखवादी ) दृष्टि रखते हैं, वे निवृत्तिपरक नहीं माने जा सकते । संक्षेप में जो लोक-कल्याण को प्रमुखता देते हैं वे प्रवृत्तिमार्गी कहे जाते हैं तथा जो आचार-दर्शन वैयक्तिक आत्मकल्याण को प्रमुखता देते हैं वे निवृत्तिमार्गी कहे जाते हैं। पं० सुखलालजी लिखते हैं, 'प्रवर्तक धर्म का संक्षेप सार यह है कि जो और जैसी समाज-व्यवस्था हो उसे इस तरह नियम और कर्तव्यबद्ध बनाना कि जिससे समाज का प्रत्येक सदस्य अपनी-अपनी स्थिति और कक्षा में सुखलाभ करे । प्रवर्तक धर्म का उद्देश्य समाज-व्यवस्था के साथ-साथ जन्मान्तर १. जैनधर्म का प्राण, पृ० १२६-१२७
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org