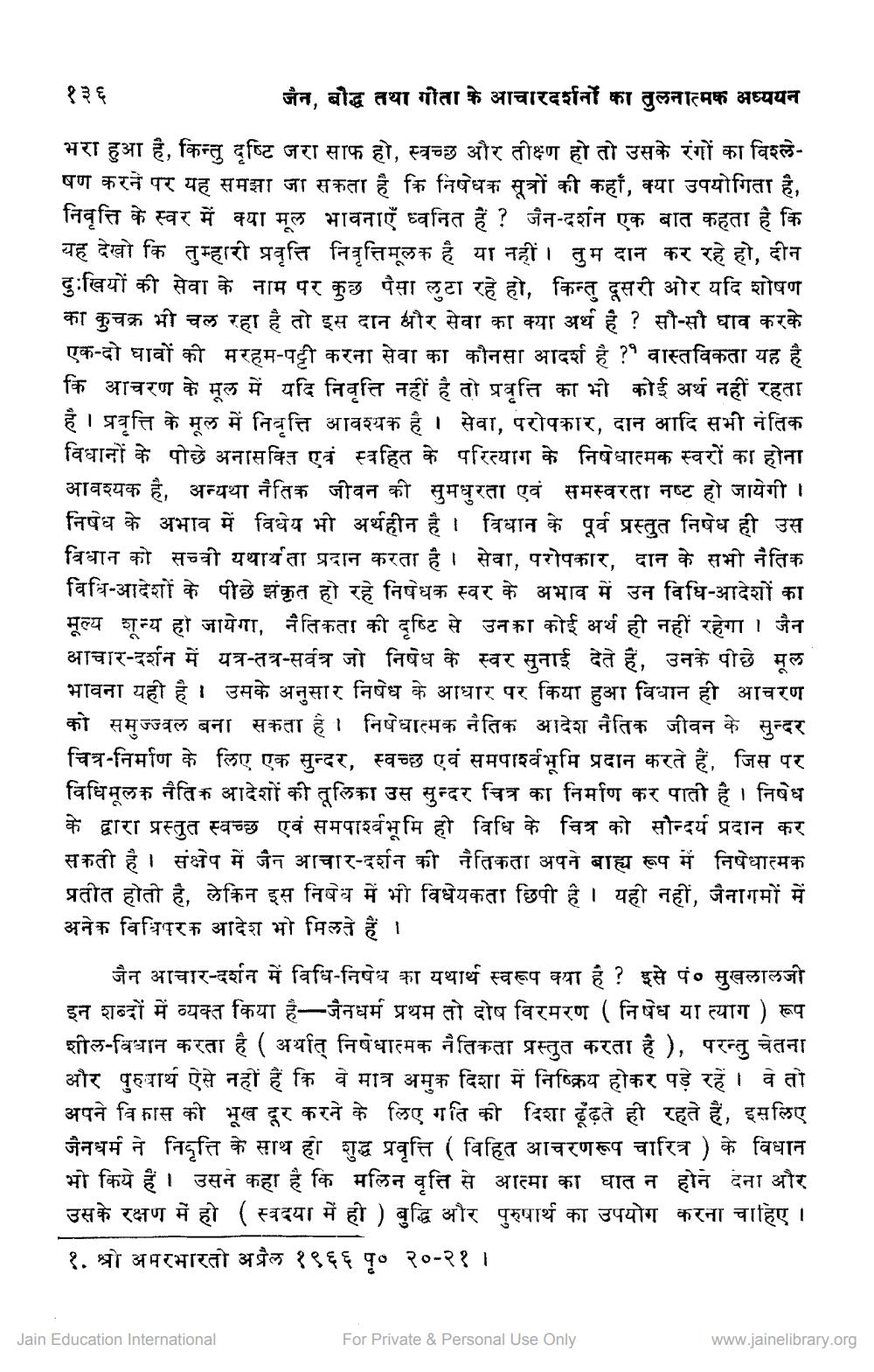________________
१३६
जैन, बौद्ध तथा गोता के आचारदर्शनों का तुलनात्मक अध्ययन
भरा हुआ है, किन्तु दृष्टि जरा साफ हो, स्वच्छ और तीक्ष्ण हो तो उसके रंगों का विश्लेषण करने पर यह समझा जा सकता है कि निषेधक सूत्रों की कहाँ, क्या उपयोगिता है, निवृत्ति के स्वर में क्या मूल भावनाएँ ध्वनित हैं ? जैन दर्शन एक बात कहता है कि यह देखो कि तुम्हारी प्रवृत्ति निवृत्तिमूलक है या नहीं। तुम दान कर रहे हो, दीन दुःखियों की सेवा के नाम पर कुछ पैसा लुटा रहे हो, किन्तु दूसरी ओर यदि शोषण का कुचक्र भी चल रहा है तो इस दान और सेवा का क्या अर्थ है ? सौ-सौ घाव करके एक-दो घावों की मरहम पट्टी करना सेवा का कौनसा आदर्श है ?" वास्तविकता यह है कि आचरण के मूल में यदि निवृत्ति नहीं है तो प्रवृत्ति का भी कोई अर्थ नहीं रहता है । प्रवृत्ति के मूल में निवृत्ति आवश्यक है । सेवा, परोपकार, दान आदि सभी नंतिक विधानों के पीछे अनासक्ति एवं स्वहित के परित्याग के निषेधात्मक स्वरों का होना आवश्यक है, अन्यथा नैतिक जीवन की सुमधुरता एवं समस्वरता नष्ट हो जायेगी । निषेध के अभाव में विधेय भी अर्थहीन है । विधान के पूर्व प्रस्तुत निषेध ही उस विधान को सच्ची यथार्थता प्रदान करता है । सेवा, परोपकार, दान के सभी नैतिक विधि-आदेशों के पीछे झंकृत हो रहे निषेधक स्वर के अभाव में उन विधि आदेशों का मूल्य शून्य हो जायेगा, नैतिकता की दृष्टि से उनका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा । जैन आचार -दर्शन में यत्र तत्र सर्वत्र जो निषेध के स्वर सुनाई देते हैं, उनके पीछे मूल भावना यही है । उसके अनुसार निषेध के आधार पर किया हुआ विधान ही आचरण को समुज्ज्वल बना सकता है । निषेधात्मक नैतिक आदेश नैतिक जीवन सुन्द चित्र निर्माण के लिए एक सुन्दर, स्वच्छ एवं समपार्श्वभूमि प्रदान करते हैं, जिस पर विधिमूलक नैतिक आदेशों की तूलिका उस सुन्दर चित्र का निर्माण कर पाती है । निषेध के द्वारा प्रस्तुत स्वच्छ एवं समपार्श्वभूमि हो विधि के चित्र को सौन्दर्य प्रदान कर सकती है । संक्षेप में जैन आचार-दर्शन की नैतिकता अपने बाह्य रूप में निषेधात्मक प्रतीत होती है, लेकिन इस निषेध में भी विधेयकता छिपी है । यही नहीं, जैनागमों में अनेक विधिपरक आदेश भी मिलते हैं ।
जैन आचार-दर्शन में विधि-निषेध का यथार्थ स्वरूप क्या है ? इसे पं० सुखलालजी इन शब्दों में व्यक्त किया है— जैनधर्म प्रथम तो दोष विरमरण (निषेध या त्याग ) रूप शील-विधान करता है ( अर्थात् निषेधात्मक नैतिकता प्रस्तुत करता है ), परन्तु चेतना और पुरुषार्थ ऐसे नहीं हैं कि वे मात्र अमुक दिशा में निष्क्रिय होकर पड़े रहें । वे तो अपने विकास की भूख दूर करने के लिए गति की दिशा ढूँढ़ते ही रहते हैं, इसलिए जैनधर्म ने निवृत्ति के साथ ही शुद्ध प्रवृत्ति ( विहित आचरणरूप चारित्र ) के विधान भो किये हैं । उसने कहा है कि मलिन वृत्ति से आत्मा का घात न होने देना और उसके रक्षण हो ( स्वदया में ही ) बुद्धि और पुरुषार्थ का उपयोग करना चाहिए । १. श्री अमरभारती अप्रैल १९६६ पृ० २०-२१ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org