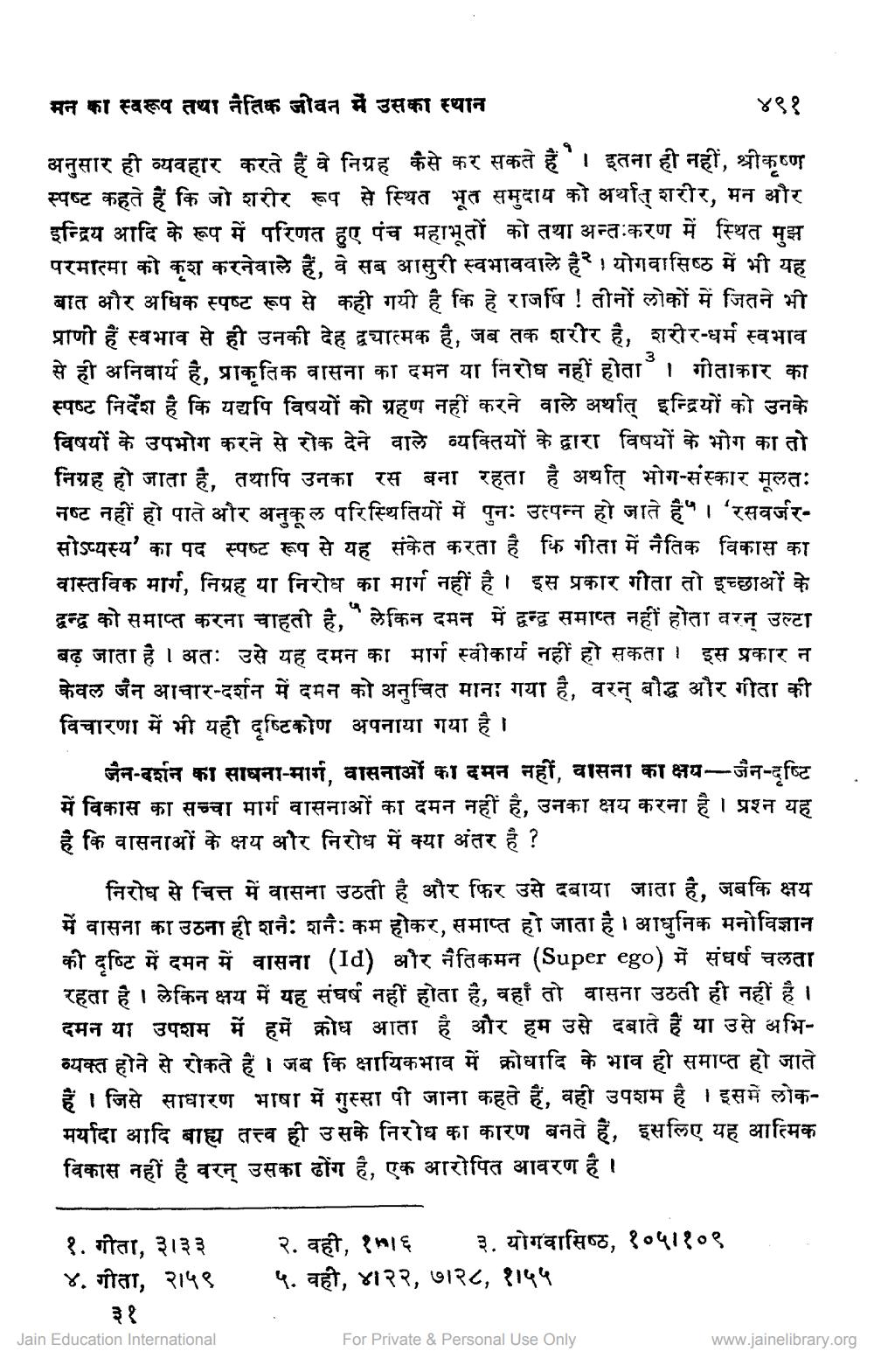________________
मन का स्वरूप तथा नैतिक जीवन में उसका स्थान
४९१
अनुसार ही व्यवहार करते हैं वे निग्रह कैसे कर सकते हैं। इतना ही नहीं, श्रीकृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को अर्थात् शरीर, मन और इन्द्रिय आदि के रूप में परिणत हुए पंच महाभूतों को तथा अन्तःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को कुश करनेवाले हैं, वे सब आसुरी स्वभाववाले है । योगवासिष्ठ में भी यह बात और अधिक स्पष्ट रूप से कही गयी है कि हे राजर्षि ! तीनों लोकों में जितने भी प्राणी हैं स्वभाव से ही उनकी देह द्वयात्मक है, जब तक शरीर है, शरीर-धर्म स्वभाव से ही अनिवार्य है, प्राकृतिक वासना का दमन या निरोध नहीं होता। गीताकार का स्पष्ट निर्देश है कि यद्यपि विषयों को ग्रहण नहीं करने वाले अर्थात् इन्द्रियों को उनके विषयों के उपभोग करने से रोक देने वाले व्यक्तियों के द्वारा विषयों के भोग का तो निग्रह हो जाता है, तथापि उनका रस बना रहता है अर्थात् भोग-संस्कार मूलतः नष्ट नहीं हो पाते और अनुकूल परिस्थितियों में पुनः उत्पन्न हो जाते है । 'रसवर्जरसोऽप्यस्य' का पद स्पष्ट रूप से यह संकेत करता है कि गीता में नैतिक विकास का वास्तविक मार्ग, निग्रह या निरोध का मार्ग नहीं है। इस प्रकार गीता तो इच्छाओं के द्वन्द्व को समाप्त करना चाहती है, लेकिन दमन में द्वन्द्व समाप्त नहीं होता वरन् उल्टा बढ़ जाता है । अतः उसे यह दमन का मार्ग स्वीकार्य नहीं हो सकता। इस प्रकार न केवल जैन आचार-दर्शन में दमन को अनुचित माना गया है, वरन् बौद्ध और गीता की विचारणा में भी यही दृष्टिकोण अपनाया गया है ।
जैन-दर्शन का साधना-मार्ग, वासनाओं का दमन नहीं, वासना का क्षय-जैन-दृष्टि में विकास का सच्चा मार्ग वासनाओं का दमन नहीं है, उनका क्षय करना है । प्रश्न यह है कि वासनाओं के क्षय और निरोध में क्या अंतर है ?
निरोध से चित्त में वासना उठती है और फिर उसे दबाया जाता है, जबकि क्षय में वासना का उठना ही शनैः शनैः कम होकर, समाप्त हो जाता है । आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि में दमन में वासना (Id) और नैतिकमन (Super ego) में संघर्ष चलता रहता है । लेकिन क्षय में यह संघर्ष नहीं होता है, वहाँ तो वासना उठती ही नहीं है । दमन या उपशम में हमें क्रोध आता है और हम उसे दबाते हैं या उसे अभिव्यक्त होने से रोकते हैं । जब कि क्षायिकभाव में क्रोधादि के भाव ही समाप्त हो जाते हैं । जिसे साधारण भाषा में गुस्सा पी जाना कहते हैं, वही उपशम है । इसमें लोकमर्यादा आदि बाह्य तत्त्व ही उसके निरोध का कारण बनते हैं, इसलिए यह आत्मिक विकास नहीं है वरन् उसका ढोंग है, एक आरोपित आवरण है।
१. गीता, ३।३३ ४. गीता, २।५९
२. वही, १११६ ३. योगवासिष्ठ, १०५।१०९ ५. वही, ४।२२, ७।२८, ११५५
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org