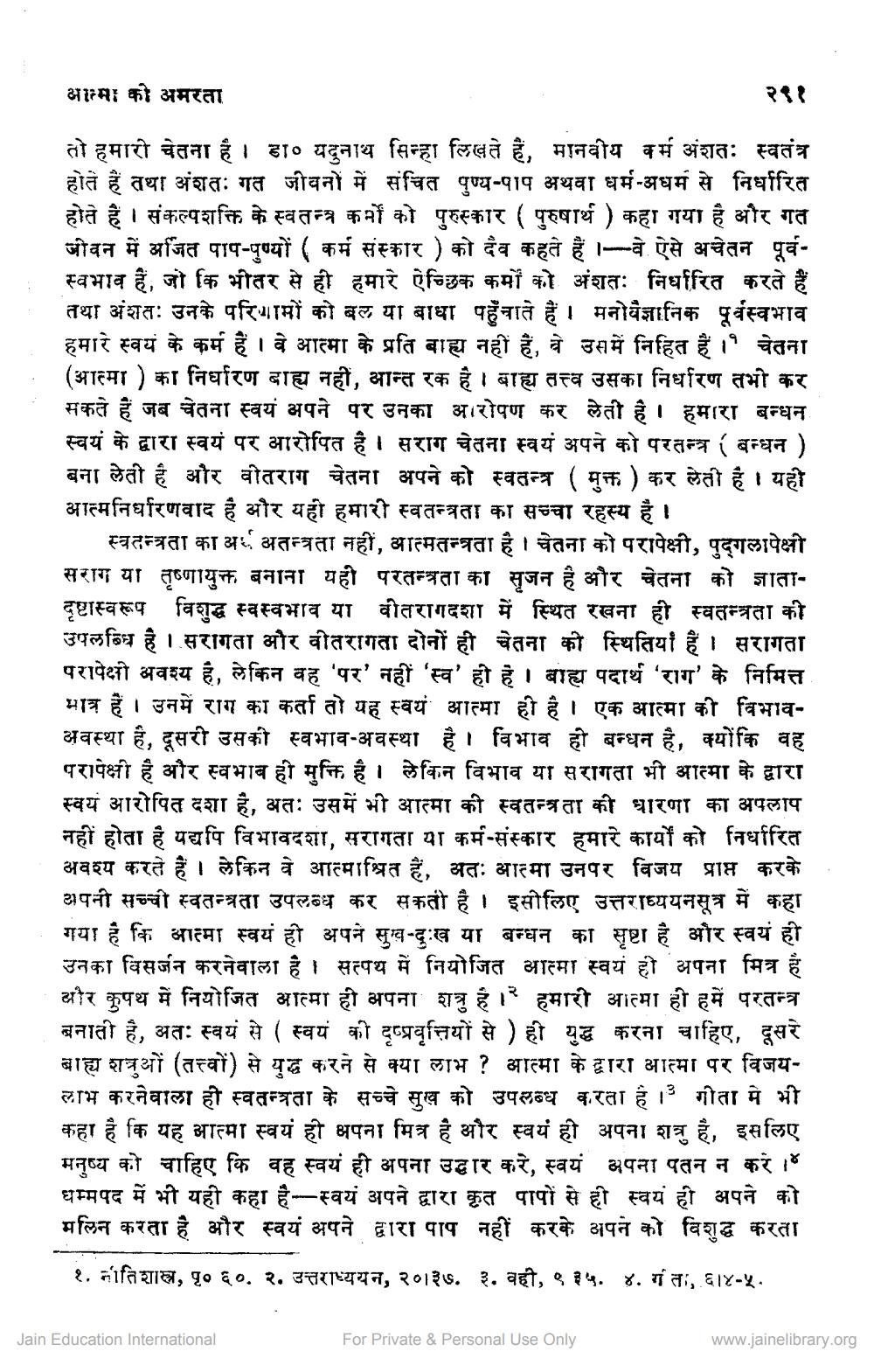________________
आत्मा को अमरता
२११
तो हमारी चेतना है । डा० यदुनाथ सिन्हा लिखते हैं, मानवीय कर्म अंशतः स्वतंत्र होते हैं तथा अंशतः गत जीवनों में संचित पुण्य-पाप अथवा धर्म-अधर्म से निर्धारित होते हैं । संकल्पशक्ति के स्वतन्त्र कर्मों को पुरुस्कार ( पुरुषार्थ ) कहा गया है और गत जीवन में अजित पाप-पुण्यों ( कर्म संस्कार ) को देव कहते हैं। वे ऐसे अचेतन पूर्वस्वभाव हैं, जो कि भीतर से ही हमारे ऐच्छिक कर्मों को अंशतः निर्धारित करते हैं तथा अंशतः उनके परिणामों को बल या बाधा पहुंचाते हैं। मनोवैज्ञानिक पूर्वस्वभाव हमारे स्वयं के कर्म हैं । वे आत्मा के प्रति बाह्य नहीं हैं, वे उसमें निहित हैं।' चेतना (आत्मा) का निर्धारण बाह्य नहीं, आन्त रक है । बाह्य तत्त्व उसका निर्धारण तभी कर सकते हैं जब चेतना स्वयं अपने पर उनका आरोपण कर लेती है। हमारा बन्धन स्वयं के द्वारा स्वयं पर आरोपित है। सराग चेतना स्वयं अपने को परतन्त्र (बन्धन ) बना लेती है और वीतराग चेतना अपने को स्वतन्त्र ( मुक्त ) कर लेती है । यही आत्मनिर्धारणवाद है और यही हमारी स्वतन्त्रता का सच्चा रहस्य है।
स्वतन्त्रता का अ. अतन्त्रता नहीं, आत्मतन्त्रता है । चेतना को परापेक्षी, पुद्गलापेक्षी सराग या तृष्णायुक्त बनाना यही परतन्त्रता का सृजन है और चेतना को ज्ञातादृष्टास्वरूप विशुद्ध स्वस्वभाव या वीतरागदशा में स्थित रखना ही स्वतन्त्रता की उपलब्धि है । सरागता और वीतरागता दोनों ही चेतना की स्थितियां हैं। सरागता परापेक्षी अवश्य है, लेकिन वह 'पर' नहीं 'स्व' ही है । बाह्य पदार्थ 'राग' के निमित्त मात्र हैं। उनमें राग का कर्ता तो यह स्वयं आत्मा ही है। एक आत्मा की विभावअवस्था है, दूसरी उसकी स्वभाव-अवस्था है। विभाव हो बन्धन है, क्योंकि वह परापेक्षी है और स्वभाव ही मुक्ति है। लेकिन विभाव या सरागता भी आत्मा के द्वारा स्वयं आरोपित दशा है, अतः उसमें भी आत्मा की स्वतन्त्रता की धारणा का अपलाप नहीं होता है यद्यपि विभावदशा, सरागता या कर्म-संस्कार हमारे कार्यों को निर्धारित अवश्य करते हैं । लेकिन वे आत्माश्रित हैं, अतः आत्मा उनपर विजय प्राप्त करके अपनी सच्ची स्वतन्त्रता उपलब्ध कर सकती है। इसीलिए उत्तराध्ययनसूत्र में कहा गया है कि आत्मा स्वयं ही अपने सुख-दुःख या बन्धन का सृष्टा है और स्वयं ही उनका विसर्जन करनेवाला है। सत्पथ में नियोजित आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और कुपथ में नियोजित आत्मा ही अपना शत्रु है। हमारी आत्मा ही हमें परतन्त्र बनाती है, अतः स्वयं से ( स्वयं की दृष्प्रवृत्तियों से ) ही युद्ध करना चाहिए, दूसरे बाह्य शत्रुओं (तत्त्वों) से युद्ध करने से क्या लाभ ? आत्मा के द्वारा आत्मा पर विजयलाभ करनेवाला ही स्वतन्त्रता के सच्चे सुख को उपलब्ध करता है। गीता मे भी कहा है कि यह आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं ही अपना उद्धार करे, स्वयं अपना पतन न करें। धम्मपद में भी यही कहा है-स्वयं अपने द्वारा कृत पापों से ही स्वयं ही अपने को मलिन करता है और स्वयं अपने द्वारा पाप नहीं करके अपने को विशुद्ध करता
१. नीतिशास्त्र, पृ० ६०. २. उत्तराध्ययन, २०१३७. ३. वही, ९३५. ४. गंता, ६।४-५.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org