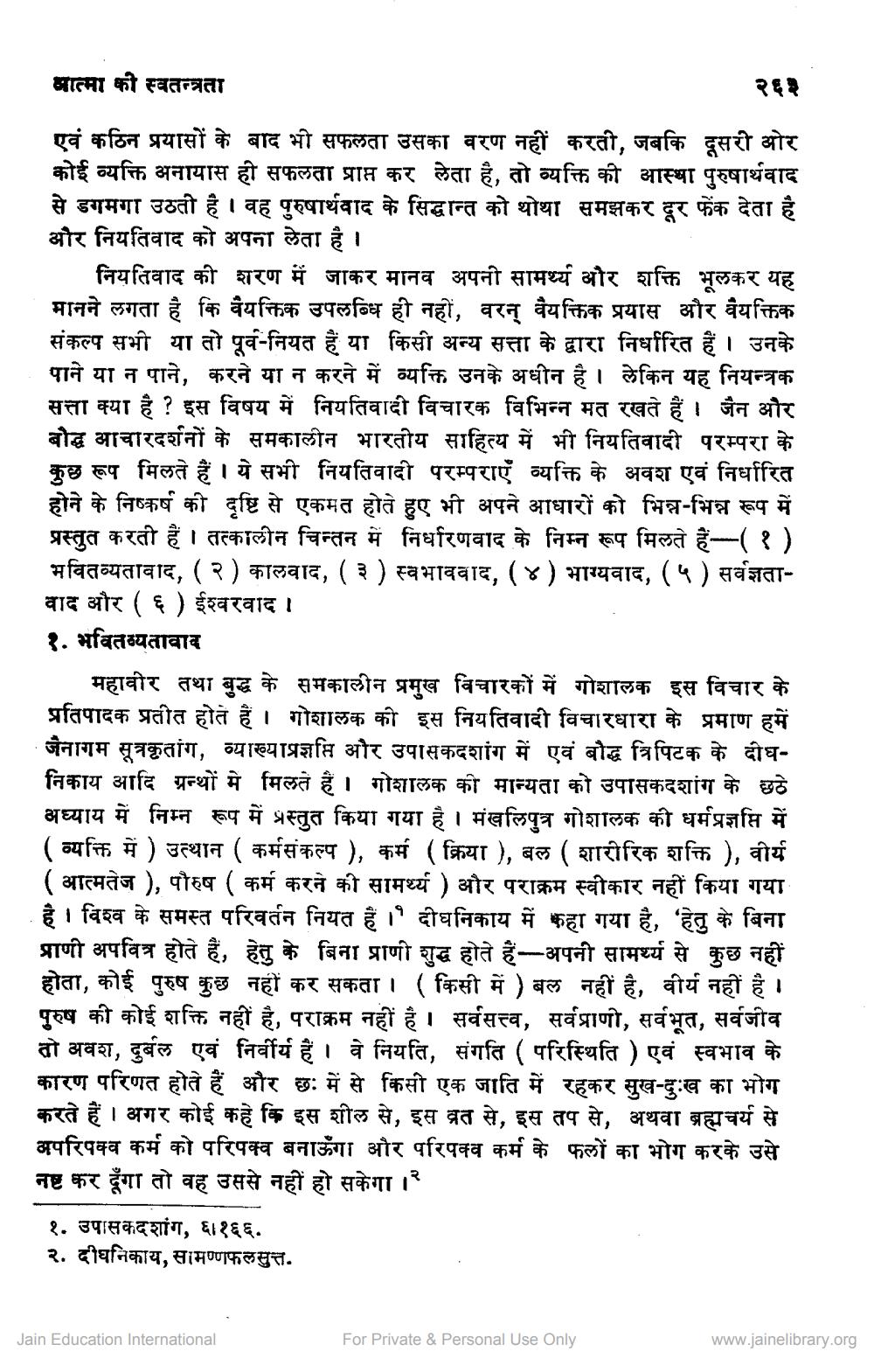________________
मात्मा को स्वतन्त्रता
२६३ एवं कठिन प्रयासों के बाद भी सफलता उसका वरण नहीं करती, जबकि दूसरी ओर कोई व्यक्ति अनायास ही सफलता प्राप्त कर लेता है, तो व्यक्ति की आस्था पुरुषार्थवाद से डगमगा उठती है । वह पुरुषार्थवाद के सिद्धान्त को थोथा समझकर दूर फेंक देता है और नियतिवाद को अपना लेता है ।
नियतिवाद की शरण में जाकर मानव अपनी सामर्थ्य और शक्ति भूलकर यह मानने लगता है कि वैयक्तिक उपलब्धि ही नहीं, वरन् वैयक्तिक प्रयास और वैयक्तिक संकल्प सभी या तो पूर्व-नियत हैं या किसी अन्य सत्ता के द्वारा निर्धारित हैं । उनके पाने या न पाने, करने या न करने में व्यक्ति उनके अधीन है। लेकिन यह नियन्त्रक सत्ता क्या है ? इस विषय में नियतिवादी विचारक विभिन्न मत रखते हैं। जैन और बौद्ध आचारदर्शनों के समकालीन भारतीय साहित्य में भी नियतिवादी परम्परा के कुछ रूप मिलते हैं । ये सभी नियतिवादी परम्पराएँ व्यक्ति के अवश एवं निर्धारित होने के निष्कर्ष की दृष्टि से एकमत होते हुए भी अपने आधारों को भिन्न-भिन्न रूप में प्रस्तुत करती हैं । तत्कालीन चिन्तन में निर्धारणवाद के निम्न रूप मिलते हैं-(१) भवितव्यतावाद, (२) कालवाद, ( ३ ) स्वभाववाद, (४) भाग्यवाद, (५) सर्वज्ञतावाद और ( ६ ) ईश्वरवाद । १. भवितव्यतावाद
महावीर तथा बुद्ध के समकालीन प्रमुख विचारकों में गोशालक इस विचार के प्रतिपादक प्रतीत होते हैं । गोशालक की इस नियतिवादी विचारधारा के प्रमाण हमें जैनागम सूत्रकृतांग, व्याख्याप्रज्ञप्ति और उपासकदशांग में एवं बौद्ध त्रिपिटक के दीघनिकाय आदि ग्रन्थों मे मिलते हैं। गोशालक की मान्यता को उपासकदशांग के छठे अध्याय में निम्न रूप में प्रस्तुत किया गया है । मंखलिपुत्र गोशालक की धर्मप्रज्ञप्ति में ( व्यक्ति में ) उत्थान ( कर्मसंकल्प ), कर्म (क्रिया ), बल ( शारीरिक शक्ति ), वीर्य ( आत्मतेज ), पौरुष ( कर्म करने की सामर्थ्य ) और पराक्रम स्वीकार नहीं किया गया है। विश्व के समस्त परिवर्तन नियत हैं ।' दीघनिकाय में कहा गया है, 'हेतु के बिना प्राणी अपवित्र होते हैं, हेतु के बिना प्राणी शुद्ध होते हैं-अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं होता, कोई पुरुष कुछ नहीं कर सकता। (किसी में ) बल नहीं है, वीर्य नहीं है । पुरुष की कोई शक्ति नहीं है, पराक्रम नहीं है। सर्वसत्त्व, सर्वप्राणी, सर्वभूत, सर्वजीव तो अवश, दुर्बल एवं निर्वीर्य हैं। वे नियति, संगति ( परिस्थिति ) एवं स्वभाव के कारण परिणत होते हैं और छः में से किसी एक जाति में रहकर सुख-दुःख का भोग करते हैं । अगर कोई कहे कि इस शील से, इस व्रत से, इस तप से, अथवा ब्रह्मचर्य से अपरिपक्व कर्म को परिपक्व बनाऊँगा और परिपक्व कर्म के फलों का भोग करके उसे नष्ट कर दूंगा तो वह उससे नहीं हो सकेगा। १. उपासकदशांग, ६।१६६. २. दीघनिकाय, सामण्णफलसुत्त.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org