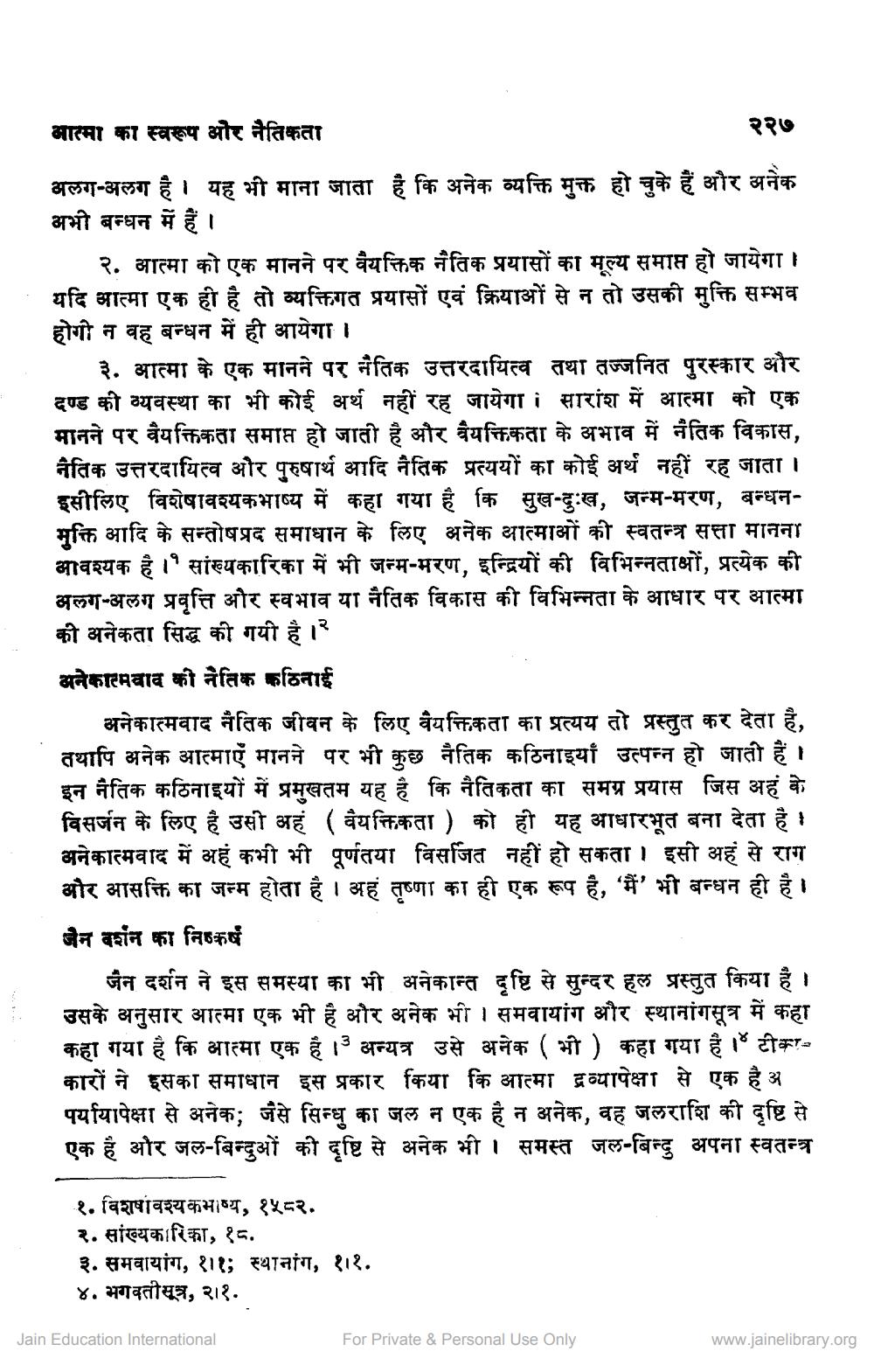________________
आत्मा का स्वरूप और नैतिकता
२२७
अलग-अलग है । यह भी माना जाता है कि अनेक व्यक्ति मुक्त हो चुके हैं और अनेक अभी बन्धन में हैं ।
२. आत्मा को एक मानने पर वैयक्तिक नैतिक प्रयासों का मूल्य समाप्त हो जायेगा । यदि आत्मा एक ही है तो व्यक्तिगत प्रयासों एवं क्रियाओं से न तो उसकी मुक्ति सम्भव होगी न वह बन्धन में ही आयेगा ।
३. आत्मा के एक मानने पर नैतिक उत्तरदायित्व तथा तज्जनित पुरस्कार और दण्ड की व्यवस्था का भी कोई अर्थ नहीं रह जायेगा । सारांश में आत्मा को एक मानने पर वैयक्तिकता समाप्त हो जाती है और वैयक्तिकता के अभाव में नैतिक विकास, नैतिक उत्तरदायित्व और पुरुषार्थ आदि नैतिक प्रत्ययों का कोई अर्थ नहीं रह जाता । इसीलिए विशेषावश्यकभाष्य में कहा गया है कि सुख-दुःख, जन्म-मरण, बन्धनमुक्ति आदि के सन्तोषप्रद समाधान के लिए अनेक आत्माओं की स्वतन्त्र सत्ता मानना आवश्यक है ।" सांख्यकारिका में भी जन्म-मरण, इन्द्रियों की विभिन्नताओं, प्रत्येक की अलग-अलग प्रवृत्ति और स्वभाव या नैतिक विकास की विभिन्नता के आधार पर आत्मा की अनेकता सिद्ध की गयी है । २
अनेकात्मवाद की नैतिक कठिनाई
अनेकात्मवाद नैतिक जीवन के लिए वैयक्तिकता का प्रत्यय तो प्रस्तुत कर देता है, तथापि अनेक आत्माएँ मानने पर भी कुछ नैतिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं । इन नैतिक कठिनाइयों में प्रमुखतम यह है कि नैतिकता का समग्र प्रयास जिस अहं के विसर्जन के लिए है उसी अहं ( वैयक्तिकता ) को ही यह आधारभूत बना देता है । अनेकात्मवाद में अहं कभी भी पूर्णतया विसर्जित नहीं हो सकता । इसी अहं से राग और आसक्ति का जन्म होता है । अहं तृष्णा का ही एक रूप है, 'मैं' भी बन्धन ही है । जैन दर्शन का निष्कर्ष
जैन दर्शन ने इस समस्या का भी अनेकान्त दृष्टि से सुन्दर हल प्रस्तुत किया है । उसके अनुसार आत्मा एक भी है और अनेक भी । समवायांग और स्थानांगसूत्र में कहा कहा गया है कि आत्मा एक है । अन्यत्र उसे अनेक ( भी ) कहा गया है । टीकाकारों ने इसका समाधान इस प्रकार किया कि आत्मा द्रव्यापेक्षा से एक है अ पर्यायापेक्षा से अनेक; जैसे सिन्धु का जल न एक है न अनेक, वह जलराशि की दृष्टि से एक है और जल - बिन्दुओं की दृष्टि से अनेक भी । समस्त जल - बिन्दु अपना स्वतन्त्र
१. विशेषांवश्यकभाष्य, १५८२. २. सांख्यकारिका, १८.
३. समवायांग, १११ स्थानांग, ११.
४. भगवती सूत्र, २१.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org