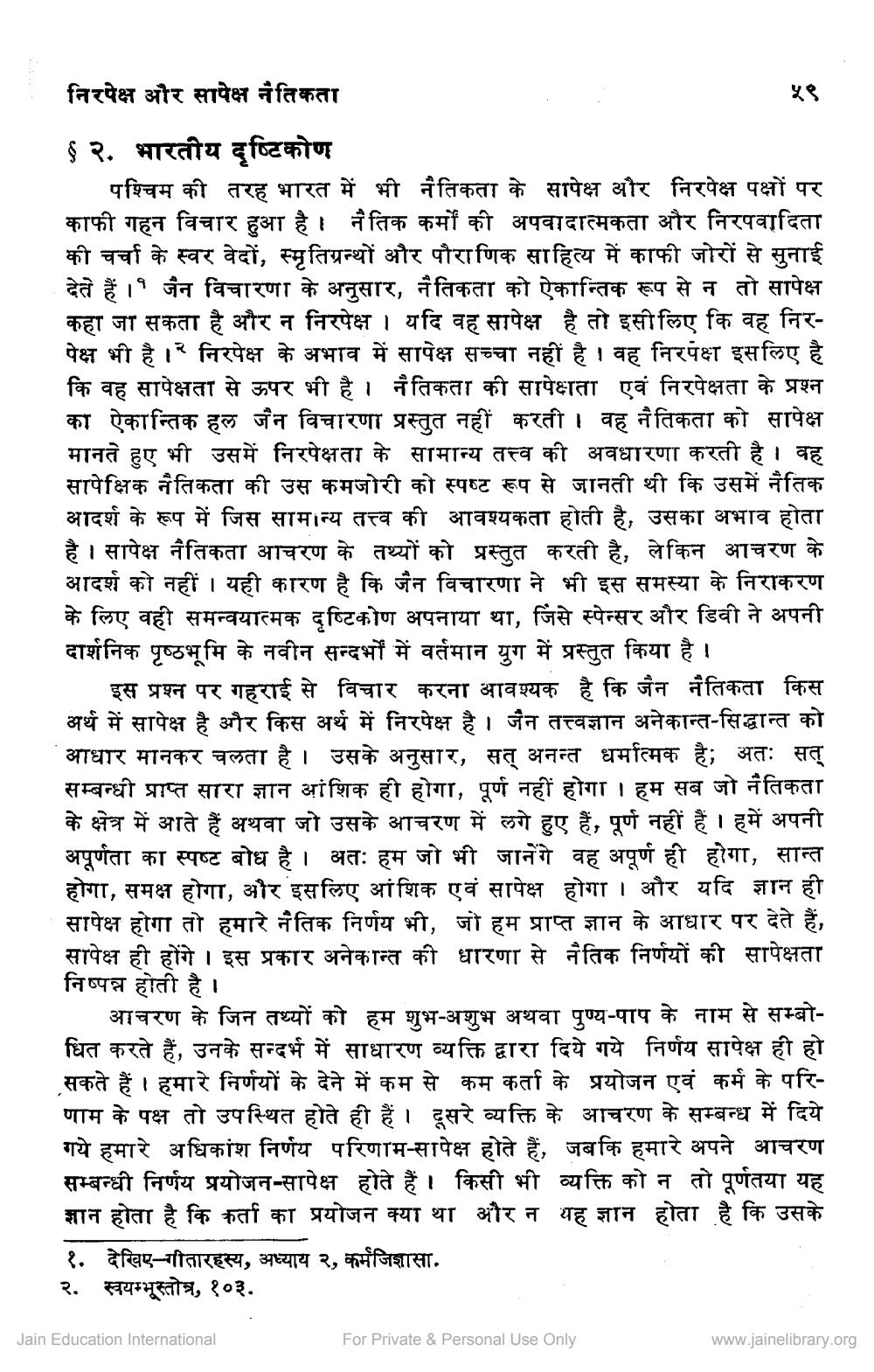________________
निरपेक्ष और सापेक्ष नैतिकता
६२. भारतीय दृष्टिकोण
पश्चिम की तरह भारत में भी नैतिकता के सापेक्ष और निरपेक्ष पक्षों पर काफी गहन विचार हुआ है। नैतिक कर्मों की अपवादात्मकता और निरपवादिता की चर्चा के स्वर वेदों, स्मृतिग्रन्थों और पौराणिक साहित्य में काफी जोरों से सुनाई देते हैं। जैन विचारणा के अनुसार, नैतिकता को ऐकान्तिक रूप से न तो सापेक्ष कहा जा सकता है और न निरपेक्ष । यदि वह सापेक्ष है तो इसीलिए कि वह निरपेक्ष भी है ।२ निरपेक्ष के अभाव में सापेक्ष सच्चा नहीं है । वह निरपेक्ष इसलिए है कि वह सापेक्षता से ऊपर भी है। नैतिकता की सापेक्षता एवं निरपेक्षता के प्रश्न का ऐकान्तिक हल जैन विचारणा प्रस्तुत नहीं करती। वह नैतिकता को सापेक्ष मानते हुए भी उसमें निरपेक्षता के सामान्य तत्त्व की अवधारणा करती है। वह सापेक्षिक नैतिकता की उस कमजोरी को स्पष्ट रूप से जानती थी कि उसमें नैतिक आदर्श के रूप में जिस सामान्य तत्त्व की आवश्यकता होती है, उसका अभाव होता है। सापेक्ष नैतिकता आचरण के तथ्यों को प्रस्तुत करती है, लेकिन आचरण के आदर्श को नहीं । यही कारण है कि जैन विचारणा ने भी इस समस्या के निराकरण के लिए वही समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाया था, जिसे स्पेन्सर और डिवी ने अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि के नवीन सन्दर्भो में वर्तमान युग में प्रस्तुत किया है। ___ इस प्रश्न पर गहराई से विचार करना आवश्यक है कि जैन नैतिकता किस अर्थ में सापेक्ष है और किस अर्थ में निरपेक्ष है। जैन तत्त्वज्ञान अनेकान्त-सिद्धान्त को आधार मानकर चलता है। उसके अनुसार, सत् अनन्त धर्मात्मक है; अतः सत् सम्बन्धी प्राप्त सारा ज्ञान आंशिक ही होगा, पूर्ण नहीं होगा। हम सब जो नैतिकता के क्षेत्र में आते हैं अथवा जो उसके आचरण में लगे हुए हैं, पूर्ण नहीं हैं । हमें अपनी अपूर्णता का स्पष्ट बोध है। अतः हम जो भी जानेंगे वह अपूर्ण ही होगा, सान्त होगा, समक्ष होगा, और इसलिए आंशिक एवं सापेक्ष होगा। और यदि ज्ञान ही सापेक्ष होगा तो हमारे नैतिक निर्णय भी, जो हम प्राप्त ज्ञान के आधार पर देते हैं, सापेक्ष ही होंगे। इस प्रकार अनेकान्त की धारणा से नैतिक निर्णयों की सापेक्षता निष्पन्न होती है।
आचरण के जिन तथ्यों को हम शुभ-अशुभ अथवा पुण्य-पाप के नाम से सम्बोधित करते हैं, उनके सन्दर्भ में साधारण व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्णय सापेक्ष ही हो सकते हैं। हमारे निर्णयों के देने में कम से कम कर्ता के प्रयोजन एवं कर्म के परिणाम के पक्ष तो उपस्थित होते ही हैं। दूसरे व्यक्ति के आचरण के सम्बन्ध में दिये गये हमारे अधिकांश निर्णय परिणाम सापेक्ष होते हैं, जबकि हमारे अपने आचरण सम्बन्धी निर्णय प्रयोजन-सापेक्ष होते हैं। किसी भी व्यक्ति को न तो पूर्णतया यह ज्ञान होता है कि कर्ता का प्रयोजन क्या था और न यह ज्ञान होता है कि उसके १. देखिए-गीतारहस्य, अध्याय २, कर्मजिज्ञासा. २. स्वयम्भूस्तोत्र, १०३.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org