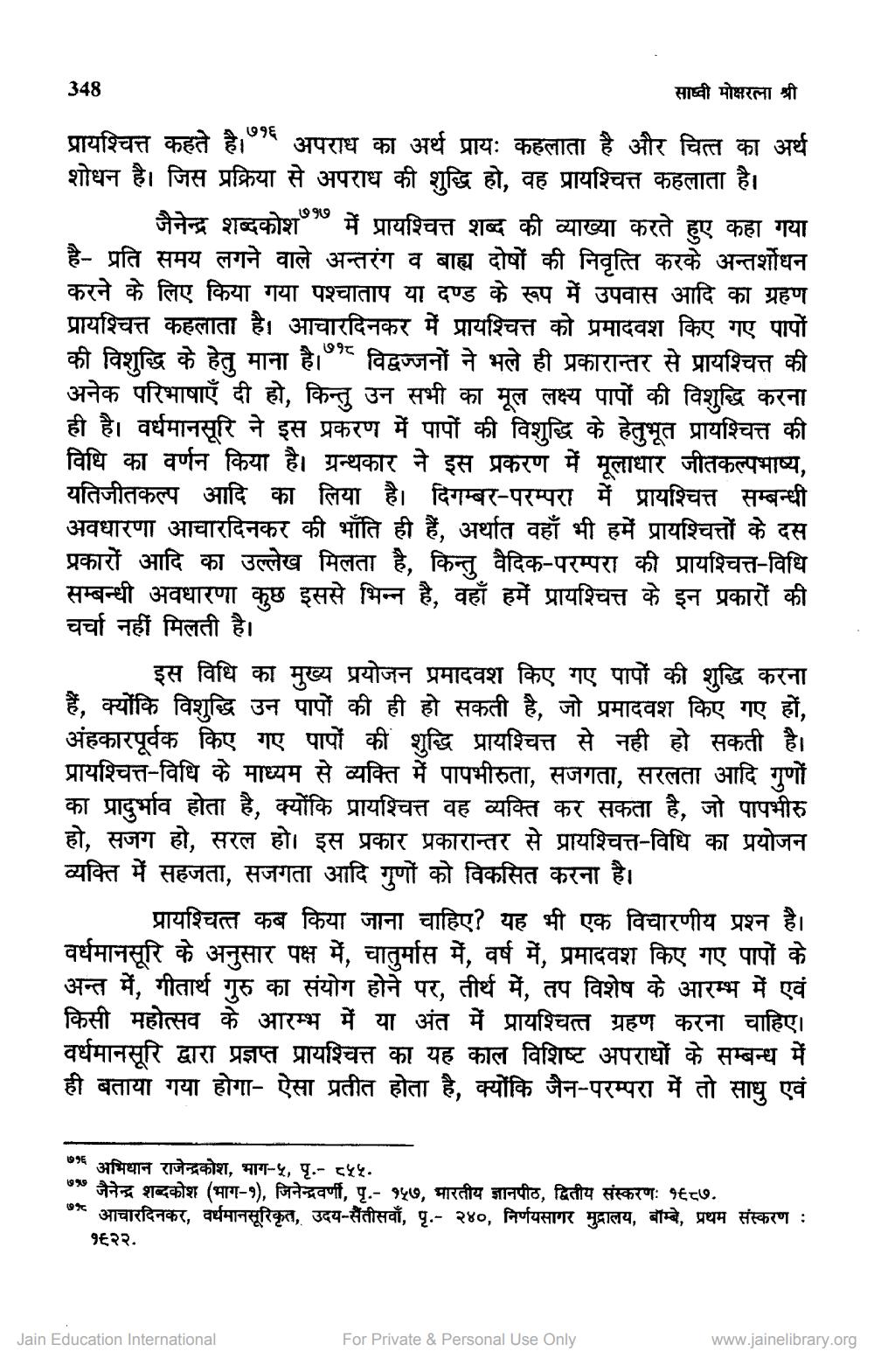________________
साध्वी मोक्षरत्ना श्री
७१६
प्रायश्चित्त कहते है। अपराध का अर्थ प्रायः कहलाता है और चित्त का अर्थ शोधन है। जिस प्रक्रिया से अपराध की शुद्धि हो, वह प्रायश्चित्त कहलाता है।
348
जैनेन्द्र शब्दकोश में प्रायश्चित्त शब्द की व्याख्या करते हुए कहा गया है- प्रति समय लगने वाले अन्तरंग व बाह्य दोषों की निवृत्ति करके अन्तर्शोधन करने के लिए किया गया पश्चाताप या दण्ड के रूप में उपवास आदि का ग्रहण प्रायश्चित्त कहलाता है। आचारदिनकर में प्रायश्चित्त को प्रमादवश किए गए पापों की विशुद्धि के हेतु माना है । ७१८ विद्वज्जनों ने भले ही प्रकारान्तर से प्रायश्चित्त की अनेक परिभाषाएँ दी हो, किन्तु उन सभी का मूल लक्ष्य पापों की विशुद्धि करना ही है। वर्धमानसूरि ने इस प्रकरण में पापों की विशुद्धि के हेतुभूत प्रायश्चित्त की विधि का वर्णन किया है । ग्रन्थकार ने इस प्रकरण में मूलाधार जीतकल्पभाष्य, यतिजीतकल्प आदि का लिया है। दिगम्बर- परम्परा में प्रायश्चित्त सम्बन्धी अवधारणा आचारदिनकर की भाँति ही हैं, अर्थात वहाँ भी हमें प्रायश्चित्तों के दस प्रकारों आदि का उल्लेख मिलता है, किन्तु वैदिक - परम्परा की प्रायश्चित्त-व सम्बन्धी अवधारणा कुछ इससे भिन्न है, वहाँ हमें प्रायश्चित्त के इन प्रकारों की चर्चा नहीं मिलती है।
इस विधि का मुख्य प्रयोजन प्रमादवश किए गए पापों की शुद्धि करना हैं, क्योंकि विशुद्धि उन पापों की ही हो सकती है, जो प्रमादवश किए गए हों, अंहकारपूर्वक किए गए पापों की शुद्धि प्रायश्चित्त से नही हो सकती है। प्रायश्चित्त - विधि के माध्यम से व्यक्ति में पापभीरुता, सजगता, सरलता आदि गुणों का प्रादुर्भाव होता है, क्योंकि प्रायश्चित्त वह व्यक्ति कर सकता है, जो पापभीरु हो, सजग हो, सरल हो। इस प्रकार प्रकारान्तर से प्रायश्चित्त - विधि का प्रयोजन व्यक्ति में सहजता, सजगता आदि गुणों को विकसित करना है ।
प्रायश्चित्त कब किया जाना चाहिए? यह भी एक विचारणीय प्रश्न है। वर्धमानसूरि के अनुसार पक्ष में, चातुर्मास में, वर्ष में, प्रमादवश किए गए पापों के अन्त में, गीतार्थ गुरु का संयोग होने पर, तीर्थ में, तप विशेष के आरम्भ में एवं किसी महोत्सव के आरम्भ में या अंत में प्रायश्चित्त ग्रहण करना चाहिए। वर्धमानसूरि द्वारा प्रज्ञप्त प्रायश्चित्त का यह काल विशिष्ट अपराधों के सम्बन्ध में ही बताया गया होगा- ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि जैन- परम्परा में तो साधु एवं
७१६ अभिधान राजेन्द्रकोश, भाग-५, पृ. ८५५.
जैनेन्द्र शब्दकोश (भाग - १), जिनेन्द्रवर्णी, पृ. १५७, भारतीय ज्ञानपीठ, द्वितीय संस्करणः १६८७. ७* आचारदिनकर, वर्धमानसूरिकृत, उदय सैंतीसवाँ, पृ. २४०, निर्णयसागर मुद्रालय, बॉम्बे, प्रथम संस्करण :
१६२२.
وری
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org