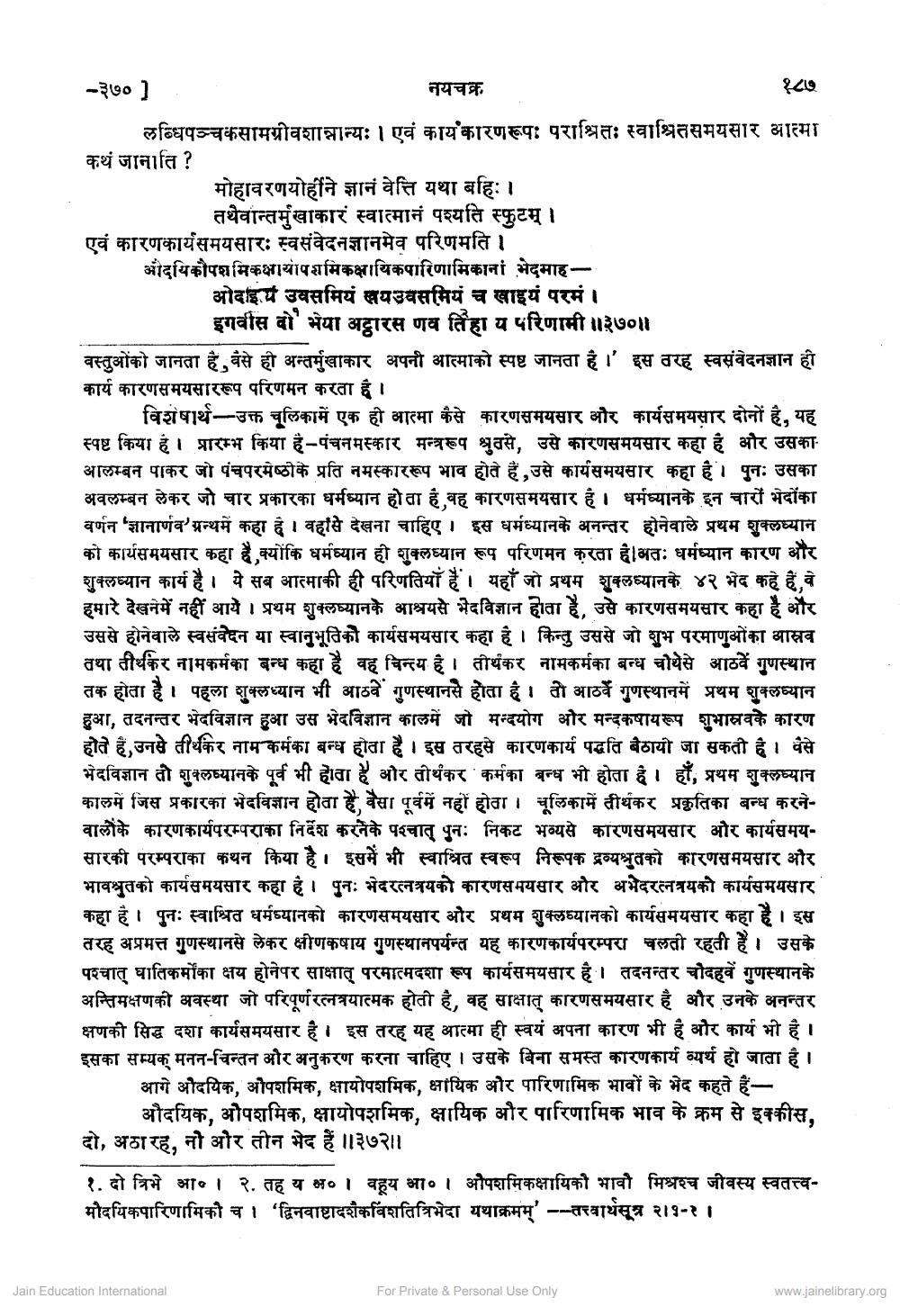________________
-३७० ] नयचक्र
१८७ लब्धिपञ्चकसामग्रीवशान्नान्यः । एवं कार्यकारणरूपः पराश्रितः स्वाश्रितसमयसार आत्मा कथं जानाति?
मोहावरणयोहीने ज्ञानं वेत्ति यथा बहिः ।
तथैवान्तर्मुखाकारं स्वात्मानं पश्यति स्फुटम् । एवं कारणकार्यसमयसारः स्वसंवेदनज्ञानमेव परिणमति । औदायिकौपशमिकक्षायोपशमिकक्षायिकपारिणामिकानां भेदमाह
ओदाइ.यं उवसमियं खयउवसमियं च खाइयं परमं ।
इगर्वीस वो' भेया अट्ठारस णव तिहा य परिणामी ॥३७०॥ वस्तुओंको जानता है, वैसे ही अन्तर्मुखाकार अपनी आत्माको स्पष्ट जानता है।' इस तरह स्वसंवेदनज्ञान ही कार्य कारणसमयसाररूप परिणमन करता है।
विशेषार्थ-उक्त चूलिकामें एक ही आत्मा कैसे कारणसमयसार और कार्यसमयसार दोनों है, यह स्पष्ट किया है। प्रारम्भ किया है-पंचनमस्कार मन्त्ररूप श्रुतसे, उसे कारणसमयसार कहा है और उसका आलम्बन पाकर जो पंचपरमेष्ठोके प्रति नमस्काररूप भाव होते हैं,उसे कार्यसमयसार कहा है। पुनः उसका अवलम्बन लेकर जो चार प्रकारका धर्मध्यान होता है वह कारणसमयसार है। धर्मध्यानके इन चारों भेदोंका वर्णन 'ज्ञानार्णव' ग्रन्थमें कहा है। वहाँसे देखना चाहिए। इस धर्मध्यानके अनन्तर होनेवाले प्रथम शुक्लध्यान
र कहा है क्योंकि धर्मध्यान ही शक्लध्यान रूप परिणमन करता है। अतः धर्मध्यान कारण और शुक्लध्यान कार्य है। ये सब आत्माकी ही परिणतियाँ हैं। यहाँ जो प्रथम शुक्लध्यानके ४२ भेद कहे हैं, वे हमारे देखनेमें नहीं आये । प्रथम शुक्लघ्यानके आश्रयसे भेदविज्ञान होता है, उसे कारणसमयसार कहा है और उससे होनेवाले स्वसंवेदन या स्वानुभूतिको कार्यसमयसार कहा है। किन्तु उससे जो शुभ परमाणुओंका आस्रव तथा तीर्थकर नामकर्मका बन्ध कहा है वह चिन्त्य है। तीर्थंकर नामकर्मका बन्ध चौथेसे आठवें गुणस्थान तक होता है। पहला शुक्लध्यान भी आठवें गुणस्थानसे होता है। तो आठवें गुणस्थानमें प्रथम शुक्लध्यान हुआ, तदनन्तर भेदविज्ञान हुआ उस भेदविज्ञान कालमें जो मन्दयोग और मन्दकषायरूप शुभास्रवके कारण होते हैं,उनसे तीर्थकर नाम कर्मका बन्ध होता है । इस तरहसे कारणकार्य पद्धति बैठायी जा सकती है। वैसे भेदविज्ञान तो शुक्लध्यानके पूर्व भी होता है और तीर्थंकर कर्मका बन्ध भी होता है। हाँ, प्रथम शुक्लध्यान कालमें जिस प्रकारका भेदविज्ञान होता है, वैसा पूर्वमें नहीं होता। चूलिकामें तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध करनेवालोंके कारणकार्यपरम्पराका निर्देश करनेके पश्चात् पुनः निकट भव्यसे कारणसमयसार और कार्यसमयसारकी परम्पराका कथन किया है। इसमें भी स्वाश्रित स्वरूप निरूपक द्रव्यश्रुतको कारणसमयसार और भावश्रुतको कार्यसमयसार कहा है। पुनः भेदरत्नत्रयको कारणसमयसार और अभेदरत्नत्रयको कार्यसमयसार कहा है। पुनः स्वाश्रित धर्मध्यानको कारणसमयसार और प्रथम शुक्लध्यानको कार्यसमयसार कहा है। इस तरह अप्रमत्त गुणस्थानसे लेकर क्षीणकषाय गुणस्थानपर्यन्त यह कारणकार्यपरम्परा चलती रहती है। उसके पश्चात् घातिकर्मोका क्षय होनेपर साक्षात् परमात्मदशा रूप कार्यसमयसार है। तदनन्तर चौदहवें गुणस्थानके अन्तिमक्षणको अवस्था जो परिपूर्णरत्नत्रयात्मक होती है, वह साक्षात् कारणसमयसार है और उनके अनन्तर क्षणकी सिद्ध दशा कार्यसमयसार है। इस तरह यह आत्मा ही स्वयं अपना कारण भी है और कार्य भी है । इसका सम्यक् मनन-चिन्तन और अनुकरण करना चाहिए। उसके बिना समस्त कारणकार्य व्यर्थ हो जाता है।
आगे औदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक और पारिणामिक भावों के भेद कहते हैं
औदयिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक और पारिणामिक भाव के क्रम से इक्कीस, दो, अठारह, नो और तीन भेद हैं ॥३७२।। १. दो त्रिभे आ० । २. तह य भ०। वहूय आ० । औपशमिकक्षायिको भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्त्वमौदयिकपारिणामिको च । “द्विनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमम्' --तत्त्वार्थसूत्र २।१-१ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org