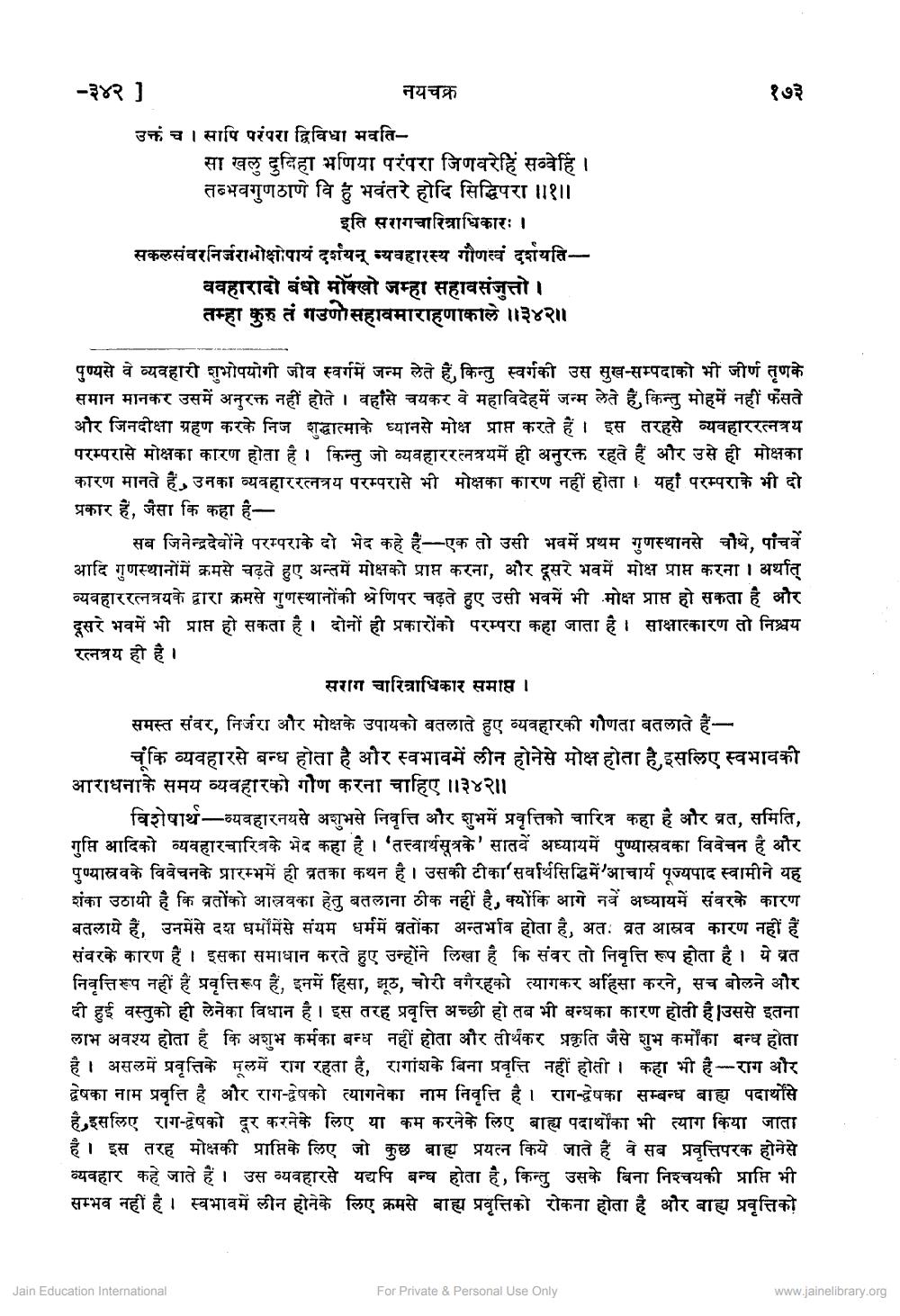________________
-३४२ ]
नयचक्र
१७३
उक्तं च । सापि परंपरा द्विविधा भवति
सा खलु दुदिहा भणिया परंपरा जिणवरेहिं सव्वेहि । तब्भवगुणठाणे वि हुँ भवंतरे होदि सिद्धिपरा ॥१॥
इति सरागचारित्राधिकारः । सकलसंवरनिर्जराभोक्षोपायं दर्शयन् न्यवहारस्य गौणत्वं दर्शयति
ववहारादो बंधो मोक्खो जम्हा सहावसंजुत्तो। तम्हा कुरु तं गउणोसहावमाराहणाकाले ॥३४२॥
पुण्यसे वे व्यवहारी शुभोपयोगी जीव स्वर्गमें जन्म लेते हैं, किन्तु स्वर्गकी उस सुख-सम्पदाको भी जीर्ण तृणके समान मानकर उसमें अनुरक्त नहीं होते । वहाँसे चयकर वे महाविदेहमें जन्म लेते हैं, किन्तु मोहमें नहीं फंसते और जिनदीक्षा ग्रहण करके निज शुद्धात्माके ध्यानसे मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस तरहसे व्यवहाररत्नत्रय परम्परासे मोक्षका कारण होता है। किन्तु जो व्यवहाररत्नत्रयमें ही अनुरक्त रहते हैं और उसे ही मोक्षका
रण मानते हैं, उनका व्यवहाररत्नत्रय परम्परासे भी मोक्षका कारण नहीं होता। यहां परम्पराके भी दो प्रकार हैं, जैसा कि कहा है
सब जिनेन्द्रदेवोंने परम्पराके दो भेद कहे हैं-एक तो उसी भवमें प्रथम गुणस्थानसे चौथे, पांचवें आदि गुणस्थानोंमें क्रमसे चढ़ते हुए अन्तमें मोक्षको प्राप्त करना, और दूसरे भवमें मोक्ष प्राप्त करना । अर्थात्
त्रयके द्वारा क्रमसे गणस्थानोंकी श्रेणिपर चढते हुए उसी भवमें भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है और दूसरे भवमें भी प्राप्त हो सकता है। दोनों ही प्रकारोंको परम्परा कहा जाता है। साक्षात्कारण तो निश्चय रत्नत्रय ही है।
सराग चारित्राधिकार समाप्त । समस्त संवर, निर्जरा और मोक्षके उपायको बतलाते हुए व्यवहारकी गौणता बतलाते हैं
चूंकि व्यवहारसे बन्ध होता है और स्वभावमें लीन होनेसे मोक्ष होता है, इसलिए स्वभावकी आराधनाके समय व्यवहारको गौण करना चाहिए ।।३४२॥
विशेषार्थ-व्यवहारनयसे अशुभसे निवृत्ति और शुभमें प्रवृत्तिको चारित्र कहा है और व्रत, समिति, गुप्ति आदिको व्यवहारचारित्रके भेद कहा है । 'तत्त्वार्थसूत्रके' सातवें अध्यायमें पुण्यास्रवका विवेचन है और पुण्यास्रवके विवेचनके प्रारम्भमें ही व्रतका कथन है। उसकी टीका सर्वार्थसिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामीने यह शंका उठायी है कि व्रतोंको आलवका हेतु बतलाना ठीक नहीं है, क्योंकि आगे नवें अध्यायमें संवरके व बतलाये हैं, उनमेंसे दश धर्मों मेंसे संयम धर्ममें व्रतोंका अन्तर्भाव होता है, अतः व्रत आस्रव कारण नहीं है संवरके कारण है। इसका समाधान करते हुए उन्होंने लिखा है कि संवर तो निवृत्ति रूप होता है। ये व्रत निवृत्तिरूप नहीं हैं प्रवृत्तिरूप हैं, इनमें हिंसा, झूठ, चोरी वगैरहको त्यागकर अहिंसा करने, सच बोलने और दी हुई वस्तुको ही लेनेका विधान है। इस तरह प्रवृत्ति अच्छी हो तब भी बन्धका कारण होती है उससे इतना लाभ अवश्य होता है कि अशुभ कर्मका बन्ध नहीं होता और तीर्थंकर प्रकृति जैसे शुभ कर्मोंका बन्ध होता है। असलमें प्रवृत्तिके मूलमें राग रहता है, रागांशके बिना प्रवृत्ति नहीं होती। कहा भी है-राग और द्वेषका नाम प्रवृत्ति है और राग-द्वेषको त्यागनेका नाम निवृत्ति है। राग-द्वेषका सम्बन्ध बाह्य पदार्थोंसे है,इसलिए राग-द्वेषको दूर करनेके लिए या कम करनेके लिए बाह्य पदार्थोंका भी त्याग किया जाता है। इस तरह मोक्षकी प्राप्तिके लिए जो कुछ बाह्य प्रयत्न किये जाते हैं वे सब प्रवृत्तिपरक होनेसे व्यवहार कहे जाते हैं। उस व्यवहारसे यद्यपि बन्ध होता है, किन्तु उसके बिना निश्चयकी प्राप्ति भी सम्भव नहीं है । स्वभावमें लीन होनेके लिए क्रमसे बाह्य प्रवृत्तिको रोकना होता है और बाह्य प्रवृत्तिको
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org