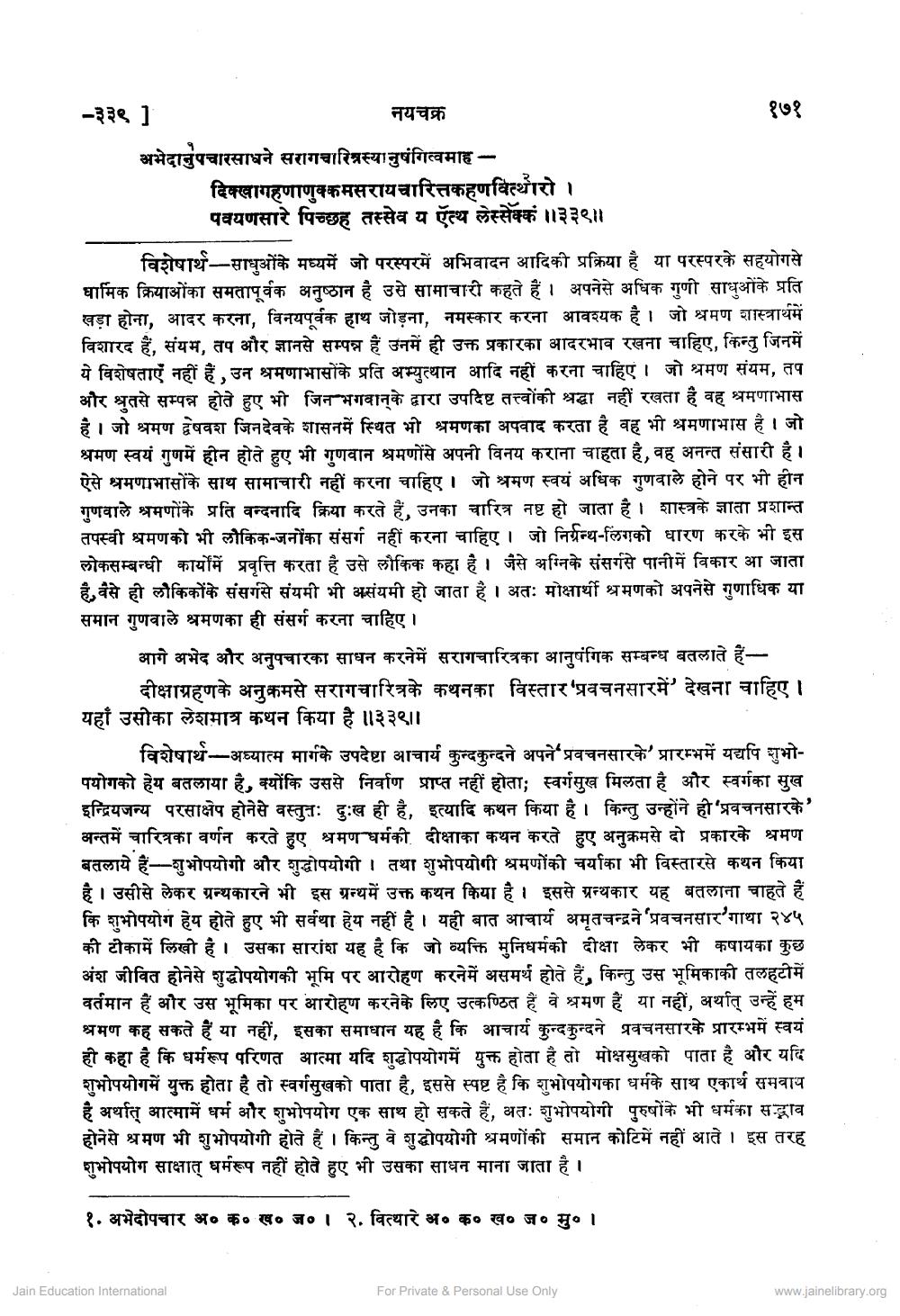________________
-३३९ ] नयचक्र
१७१ अभेदानुपचारसाधने सरागचारित्रस्यानुषंगित्वमाह -
दिक्खागहणाणुक्कमसरायचारित्तकहणवित्थोरो ।
पवयणसारे पिच्छह तस्सेव य ऍत्थ लेस्सैक्कं ॥३३९॥ विशेषार्थ-साधुओंके मध्यमें जो परस्परमें अभिवादन आदिकी प्रक्रिया है या परस्परके सहयोगसे धार्मिक क्रियाओंका समतापूर्वक अनुष्ठान है उसे सामाचारी कहते हैं। अपनेसे अधिक गुणी साधुओंके प्रति खड़ा होना, आदर करना, विनयपूर्वक हाथ जोड़ना, नमस्कार करना आवश्यक है। जो श्रमण शास्त्रार्थमें विशारद हैं, संयम, तप और ज्ञानसे सम्पन्न हैं उनमें ही उक्त प्रकारका आदरभाव रखना चाहिए, किन्तु जिनमें ये विशेषताएं नहीं हैं , उन श्रमणाभासोंके प्रति अभ्युत्थान आदि नहीं करना चाहिए। जो श्रमण संयम, तप और श्रुतसे सम्पन्न होते हुए भी जिन भगवान के द्वारा उपदिष्ट तत्त्वोंकी श्रद्धा नहीं रखता है वह श्रमणाभास है । जो श्रमण द्वेषवश जिनदेवके शासनमें स्थित भी श्रमणका अपवाद करता है वह भी श्रमणाभास है । जो श्रमण स्वयं गुणमें हीन होते हुए भी गुणवान श्रमणोंसे अपनी विनय कराना चाहता है, वह अनन्त संसारी है। ऐसे श्रमणाभासोंके साथ सामाचारी नहीं करना चाहिए। जो श्रमण स्वयं अधिक गुणवाले होने पर भी हीन गुणवाले श्रमणोंके प्रति वन्दनादि क्रिया करते हैं, उनका चारित्र नष्ट हो जाता है। शास्त्रके ज्ञाता प्रशान्त तपस्वी श्रमणको भी लौकिक-जनोंका संसर्ग नहीं करना चाहिए। जो निम्रन्थ-लिंगको धारण करके भी इस लोकसम्बन्धी कार्योंमें प्रवृत्ति करता है उसे लौकिक कहा है। जैसे अग्निके संसर्गसे पानी में विकार आ जाता है, वैसे ही लौकिकोंके संसर्गसे संयमी भी असंयमी हो जाता है। अतः मोक्षार्थी श्रमणको अपनेसे गुणाधिक या समान गुणवाले श्रमणका ही संसर्ग करना चाहिए।
आगे अभेद और अनुपचारका साधन करनेमें सरागचारित्रका आनुषंगिक सम्बन्ध बतलाते हैं
दीक्षाग्रहणके अनुकमसे सरागचारित्रके कथनका विस्तार 'प्रवचनसारमें' देखना चाहिए। यहाँ उसीका लेशमात्र कथन किया है ॥३३९।।
विशेषार्थ-अध्यात्म मार्गके उपदेष्टा आचार्य कुन्दकुन्दने अपने प्रवचनसारके' प्रारम्भमें यद्यपि शुभोपयोगको हेय बतलाया है, क्योंकि उससे निर्वाण प्राप्त नहीं होता; स्वर्गसुख मिलता है और स्वर्गका सुख इन्द्रियजन्य परसाक्षेप होनेसे वस्तुत: दुःख ही है, इत्यादि कथन किया है। किन्तु उन्होंने ही प्रवचनसारके' अन्तमें चारित्रका वर्णन करते हुए श्रमण धर्मकी दीक्षाका कथन करते हुए अनुक्रमसे दो प्रकारके श्रमण बतलाये हैं-शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी। तथा शुभोपयोगी श्रमणोंको चर्याका भी विस्तारसे कथन किया है । उसीसे लेकर ग्रन्थकारने भी इस ग्रन्थमें उक्त कथन किया है। इससे ग्रन्थकार यह बतलाना चाहते हैं कि शुभोपयोग हेय होते हुए भी सर्वथा हेय नहीं है। यही बात आचार्य अमतचन्द्र ने 'प्रवचनसारगाथा २४५ की टीकामें लिखी है। उसका सारांश यह है कि जो व्यक्ति मुनिधर्मको दीक्षा लेकर भी कषायका कुछ अंश जीवित होनेसे शुद्धोपयोगकी भूमि पर आरोहण करने में असमर्थ होते हैं, किन्तु उस भूमिकाकी तलहटीमें वर्तमान हैं और उस भूमिका पर आरोहण करनेके लिए उत्कण्ठित हैं वे श्रमण हैं या नहीं, अर्थात् उन्हें हम श्रमण कह सकते हैं या नहीं, इसका समाधान यह है कि आचार्य कुन्दकुन्दने प्रवचनसारके प्रारम्भमें स्वयं ही कहा है कि धर्मरूप परिणत आत्मा यदि शुद्धोपयोगमें युक्त होता है तो मोक्षसुखको पाता है और यदि शुभोपयोगमें युक्त होता है तो स्वर्गसुखको पाता है, इससे स्पष्ट है कि शुभोपयोगका धर्मके साथ एकार्थ समवाय है अर्थात् आत्मामें धर्म और शुभोपयोग एक साथ हो सकते हैं, अतः शुभोपयोगी पुरुषोंके भी धर्मका सद्भाव होनेसे श्रमण भी शुभोपयोगी होते हैं । किन्तु वे शुद्धोपयोगी श्रमणोंको समान कोटिमें नहीं आते। इस तरह शुभोपयोग साक्षात् धर्मरूप नहीं होते हुए भी उसका साधन माना जाता है ।
१. अभेदोपचार अ०० ख० ज०। २. वित्थारे अ.क० ख० ज०म० ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org