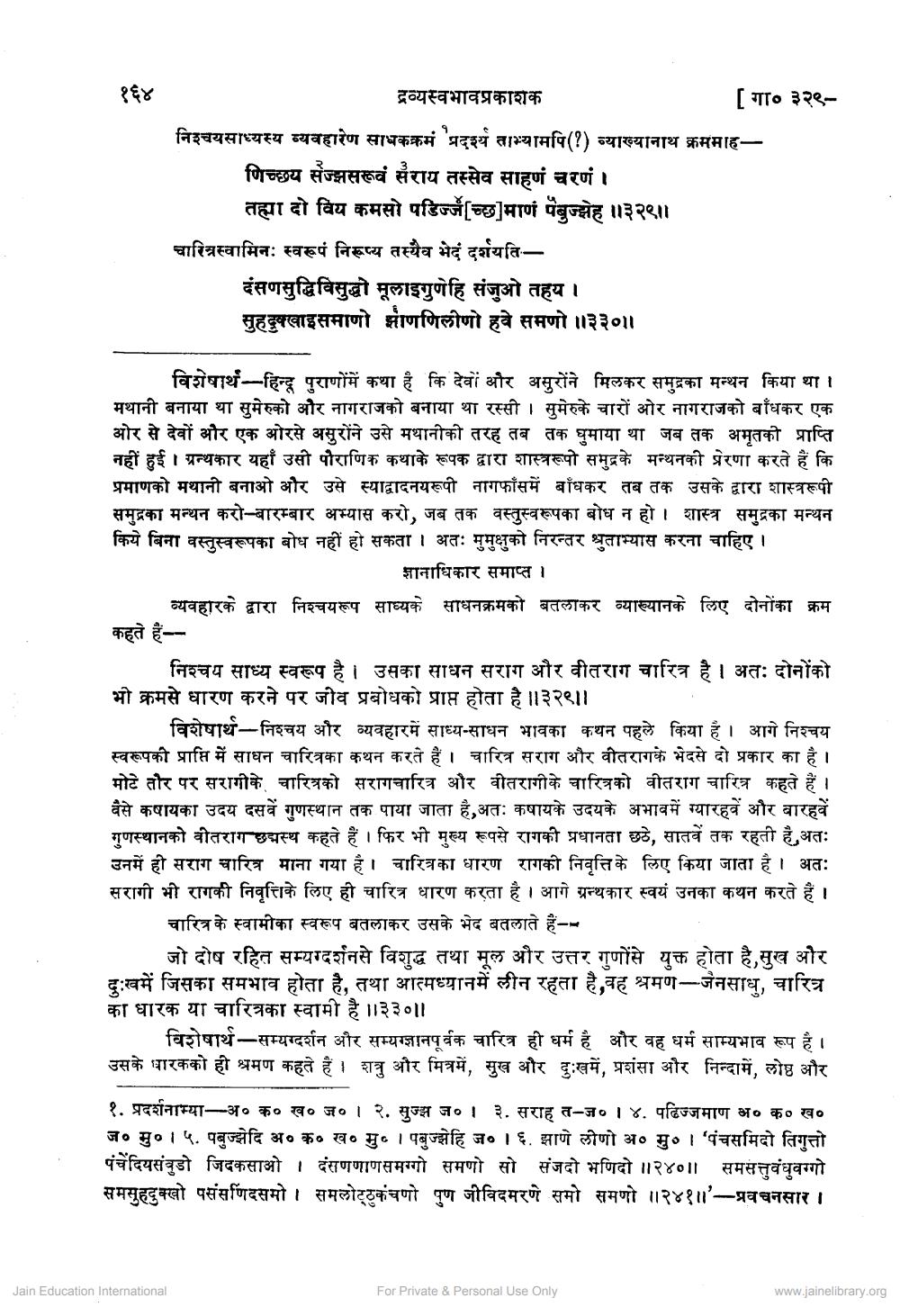________________
१६४
द्रव्यस्वभावप्रकाशक
[गा०३२९निश्चयसाध्यस्य व्यवहारेण साधकक्रम 'प्रदय ताभ्यामपि(?) व्याख्यानाथ क्रममाह
णिच्छय संज्झसरूवं सैराय तस्सेव साहणं चरणं ।
तह्मा दो विय कमसो पडिज[च्छ]माणं पेबुझेह ॥३२९॥ चारित्रस्वामिनः स्वरूपं निरूप्य तस्यैव भेदं दर्शयति
दसणसुद्धिविसुद्धो मूलाइगुणेहि संजुओ तहय । सुहदुक्खाइसमाणो झोणणिलीणो हवे समणो ॥३३०॥
विशेषार्थ-हिन्दू पुराणोंमें कथा है कि देवों और असुरोंने मिलकर समुद्रका मन्थन किया था। मथानी बनाया था सुमेरुको और नागराजको बनाया था रस्सी । सुमेरुके चारों ओर नागराजको बाँधकर एक ओर से देवों और एक ओरसे असुरोंने उसे मथानीको तरह तब तक घुमाया था जब तक अमृतको प्राप्ति नहीं हुई । ग्रन्थकार यहाँ उसी पौराणिक कथाके रूपक द्वारा शास्त्ररूपो समुद्रके मन्थनकी प्रेरणा करते हैं कि प्रमाणको मथानी बनाओ और उसे स्याद्वादनयरूपी नागफाँसमें बाँधकर तब तक उसके द्वारा शास्त्ररूपी समुद्रका मन्थन करो-बारम्बार अभ्यास करो, जब तक वस्तुस्वरूपका बोध न हो। शास्त्र समुद्रका मन्थन किये बिना वस्तुस्वरूपका बोध नहीं हो सकता । अतः मुमुक्षुको निरन्तर श्रुताभ्यास करना चाहिए।
ज्ञानाधिकार समाप्त । व्यवहारके द्वारा निश्चयरूप साध्यके साधनक्रमको बतलाकर व्याख्यानके लिए दोनोंका क्रम कहते हैं
निश्चय साध्य स्वरूप है। उसका साधन सराग और वीतराग चारित्र है । अतः दोनोंको भी क्रमसे धारण करने पर जीव प्रबोधको प्राप्त होता है॥३२९॥
विशेषार्थ-निश्चय और व्यवहार में साध्य-साधन भावका कथन पहले किया है। आगे निश्चय स्वरूपकी प्राप्ति में साधन चारित्रका कथन करते हैं। चारित्र सराग और वीतरागके भेदसे दो प्रकार का है। मोटे तौर पर सरागीके चारित्रको सरागचारित्र और वीतरागीके चारित्रको वीतराग चारित्र कहते हैं । वैसे कषायका उदय दसवें गुणस्थान तक पाया जाता है,अतः कषायके उदयके अभावमें ग्यारहवें और बारहवें गुणस्थानको वीतराग छद्मस्थ कहते हैं । फिर भी मुख्य रूपसे रागकी प्रधानता छठे, सातवें तक रहती है, अतः उनमें ही सराग चारित्र माना गया है। चारित्रका धारण रागकी निवृत्ति के लिए किया जाता है। अतः सरागी भी रागकी निवृत्तिके लिए ही चारित्र धारण करता है । आगे ग्रन्थकार स्वयं उनका कथन करते हैं ।
चारित्र के स्वामीका स्वरूप बतलाकर उसके भेद बतलाते हैं--
जो दोष रहित सम्यग्दर्शनसे विशुद्ध तथा मूल और उत्तर गुणोंसे युक्त होता है,सुख और दुःखमें जिसका समभाव होता है, तथा आत्मध्यानमें लीन रहता है,वह श्रमण-जैनसाधु, चारित्र का धारक या चारित्रका स्वामी है ॥३३०॥
विशेषार्थ-सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानपूर्वक चारित्र ही धर्म है और वह धर्म साम्यभाव रूप है। उसके धारकको ही श्रमण कहते हैं। शत्रु और मित्रमें, सुख और दुःखमें, प्रशंसा और निन्दामें, लोष्ठ और
१. प्रदर्शनाम्या-अ० क० ख० ज० । २. सुज्झ ज०। ३. सराह त-जः । ४. पढिज्जमाण अ. क० ख० ज० मु०। ५. पबुज्झेदि अ.क. ख० मु० । पबुज्झेहि ज०। ६. झाणे लोणो अ० मु.।'पंचसमिदो तिगुत्तो पंचेंदियसंवुडो जिदकसाओ । दसणणाणसमग्गो समणो सो संजदो भणिदो ॥२४०॥ समसत्तुवंधुवग्गो समसुहदुक्खो पसंसणिंदसमो। समलोट्ठकंचणो पुण जीविदमरणे समो समणो ॥२४१॥'-प्रवचनसार ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org