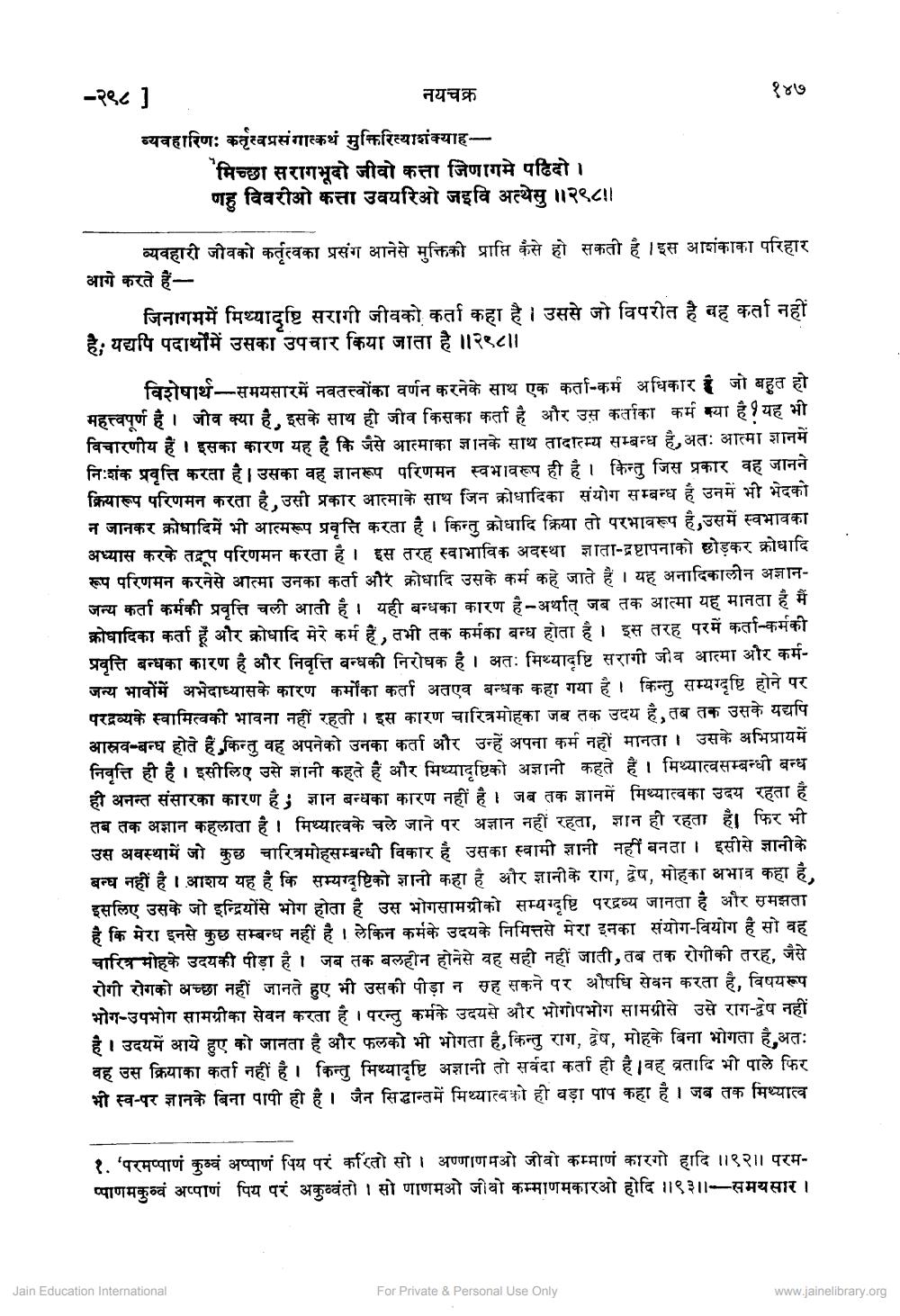________________
—२९८ ]
नयचक्र
व्यवहारिण: कर्तृत्वप्रसंगात्कथं मुक्तिरित्याशंक्याह"मिच्छा सरागभूदो जीवो कत्ता जिणागमे पढिदो ।
हु विवरीओ कत्ता उवयरिओ जइवि अत्थेसु ॥ २९८ ॥
व्यवहारी जीवको कर्तृत्वका प्रसंग आनेसे मुक्तिकी प्राप्ति कैसे हो सकती है । इस आशंकाका परिहार आगे करते हैं
१४७
निगम मिथ्यादृष्टि सरागी जीवको कर्ता कहा है। उससे जो विपरीत है वह कर्ता नहीं है; यद्यपि पदार्थों में उसका उपचार किया जाता है ॥२९८ ||
विशेषार्थ - समयसार में नवतत्त्वोंका वर्णन करनेके साथ एक कर्ता-कर्म अधिकार है जो बहुत हो महत्त्वपूर्ण है । जीव क्या है, इसके साथ ही जीव किसका कर्ता है और उस कर्ताका कर्म क्या यह भी विचारणीय हैं । इसका कारण यह है कि जैसे आत्माका ज्ञानके साथ तादात्म्य सम्बन्ध है, अतः आत्मा ज्ञानमें निःशंक प्रवृत्ति करता है। उसका वह ज्ञानरूप परिणमन स्वभावरूप ही है। किन्तु जिस प्रकार वह जानने क्रियारूप परिणमन करता है, उसी प्रकार आत्माके साथ जिन क्रोधादिका संयोग सम्बन्ध हैं उनमें भी भेदको न जानकर क्रोधादिमें भी आत्मरूप प्रवृत्ति करता । किन्तु क्रोधादि क्रिया तो परभावरूप है, उसमें स्वभावका अध्यास करके तद्रूप परिणमन करता है । इस तरह स्वाभाविक अवस्था ज्ञाता द्रष्टापनाको छोड़कर क्रोधादि रूप परिणमन करनेसे आत्मा उनका कर्ता और क्रोधादि उसके कर्म कहे जाते हैं । यह अनादिकालीन अज्ञानजन्य कर्ता कर्मकी प्रवृत्ति चली आती है । यही बन्धका कारण है - अर्थात् जब तक आत्मा यह मानता है मैं क्रोधादिका कर्ता हूँ और क्रोधादि मेरे कर्म हैं, तभी तक कर्मका बन्ध होता है । इस तरह परमें कर्ता - कर्म की प्रवृत्ति बन्धका कारण है और निवृत्ति बन्धकी निरोधक है । अतः मिथ्यादृष्टि सरागी जीव आत्मा और कर्मजन्य भावोंमें अभेदाध्यासके कारण कर्मोंका कर्ता अतएव बन्धक कहा गया है। किन्तु सम्यग्दृष्टि होने पर परद्रव्यके स्वामित्वकी भावना नहीं रहती । इस कारण चारित्रमोहका जब तक उदय है, तब तक उसके यद्यपि आस्रव - बन्ध होते हैं, किन्तु वह अपनेको उनका कर्ता और उन्हें अपना कर्म नहीं मानता। उसके अभिप्राय में निवृत्ति ही है । इसीलिए उसे ज्ञानी कहते हैं और मिथ्यादृष्टिको अज्ञानी कहते हैं । मिथ्यात्वसम्बन्धी बन्ध ही अनन्त संसारका कारण है; ज्ञान बन्धका कारण नहीं है । जब तक ज्ञानमें मिथ्यात्वका उदय रहता है। तब तक अज्ञान कहलाता है । मिथ्यात्वके चले जाने पर अज्ञान नहीं रहता, ज्ञान ही रहता है। फिर भी उस अवस्थामें जो कुछ चारित्रमोहसम्बन्धी विकार है उसका स्वामी ज्ञानी नहीं बनता । इसीसे ज्ञानी के बन्घ नहीं है । आशय यह है कि सम्यग्दृष्टिको ज्ञानी कहा है और ज्ञानीके राग, द्वेष, मोहका अभाव कहा है, इसलिए उसके जो इन्द्रियोंसे भोग होता है उस भोगसामग्रीको सम्यग्दृष्टि परद्रव्य जानता है और समझता है कि मेरा इनसे कुछ सम्बन्ध नहीं है । लेकिन कर्मके उदयके निमित्तसे मेरा इनका संयोग-वियोग है सो वह चारित्र मोहके उदयकी पीड़ा है। जब तक बलहीन होनेसे वह सही नहीं जाती, तब तक रोगी की तरह, जैसे रोगी रोगको अच्छा नहीं जानते हुए भी उसकी पीड़ा न सह सकने पर औषधि सेवन करता है, विषयरूप भोग-उपभोग सामग्रीका सेवन करता है । परन्तु कर्मके उदयसे और भोगोपभोग सामग्री से उसे राग-द्वेष नहीं है । उदयमें आये हुए को जानता है और फलको भी भोगता है, किन्तु राग, द्वेष, मोहके बिना भोगता है, अतः वह उस क्रियाका कर्ता नहीं है । किन्तु मिथ्यादृष्टि अज्ञानी तो सर्वदा कर्ता ही है । वह व्रतादि भी पाले फिर भी स्व-पर ज्ञानके बिना पापी हो है । जैन सिद्धान्तमें मिथ्यात्वको ही बड़ा पाप कहा है । जब तक मिथ्यात्व
Jain Education International
१. 'परमप्पाणं कुब्वं अप्पाणं पिय परं करितो सो । अण्णाणमओ जीवो कम्माणं कारगो हादि ॥ ९२ ॥ परमप्पाणमकुब्वं अप्पाणं पिय परं अकुव्वतो । सो णाणमओ जीवो कम्माणमकारओ होदि ॥९३॥ -- समयसार ।
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org