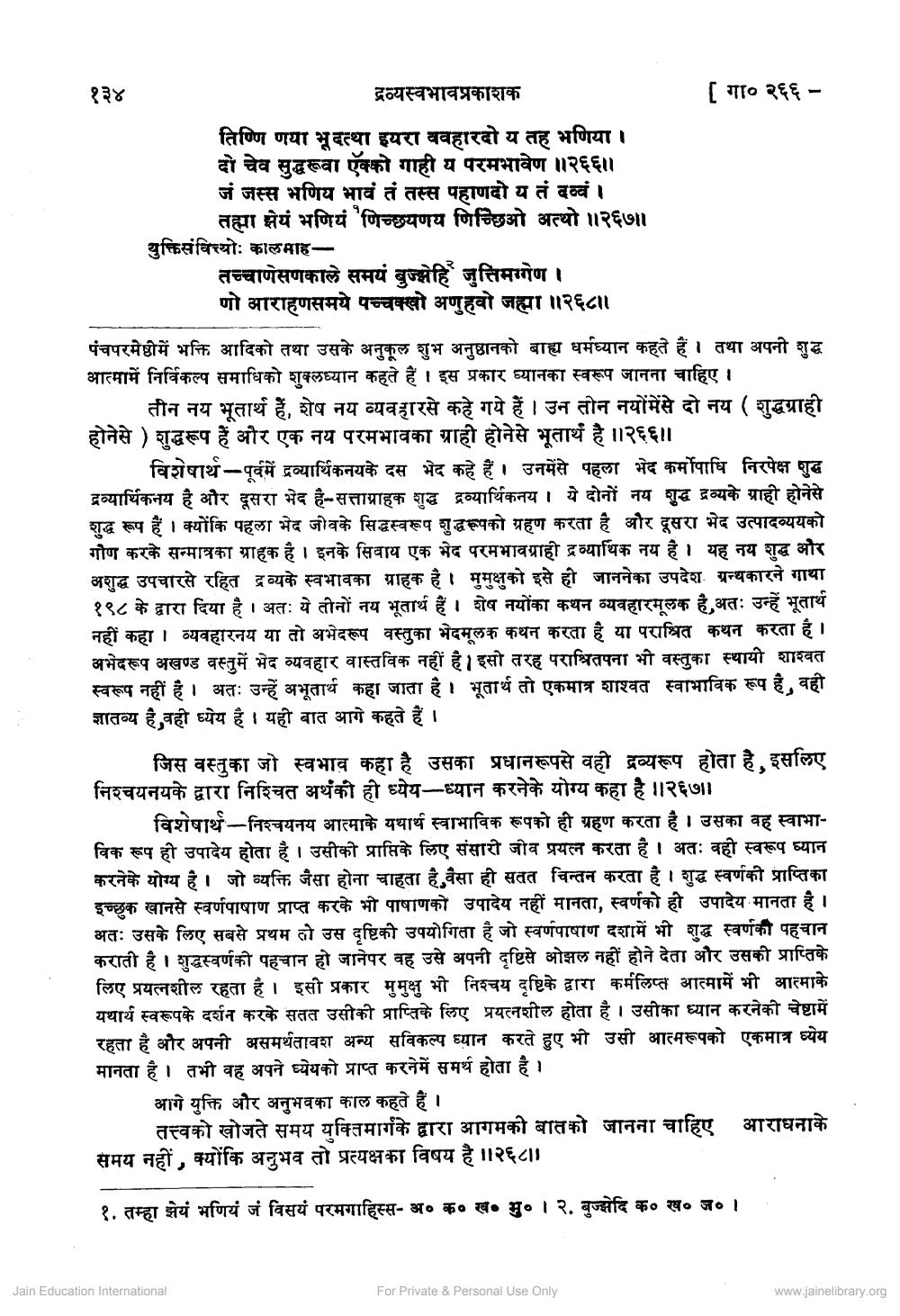________________
१३४ द्रव्यस्वभावप्रकाशक
[ गा०२६६ - तिण्णि णया भूदत्था इयरा ववहारदो य तह भणिया। दो चेव सुद्धरूवा ऍक्को गाही य परमभावेण ॥२६६॥ जं जस्स भणिय भावं तं तस्स पहाणदो य तं दव्वं ।
तह्मा झेयं भणियं णिच्छयणय णिच्छिओ अत्यो ॥२६७॥ युक्तिसंवित्योः कालमाह
तच्चाणेसणकाले समयं बुज्झेहि जुत्तिमग्गेण ।
णो आराहणसमये पच्चक्खो अणुहवो जह्मा ॥२६८॥ पंचपरमेष्ठीमें भक्ति आदिको तथा उसके अनुकूल शुभ अनुष्ठानको बाह्य धर्मध्यान कहते हैं। तथा अपनी शुद्ध आत्मामें निर्विकल्प समाधिको शुक्लध्यान कहते हैं । इस प्रकार ध्यानका स्वरूप जानना चाहिए ।
तीन नय भूतार्थ हैं, शेष नय व्यवहारसे कहे गये हैं। उन तीन नयोंमेंसे दो नय ( शुद्धग्राही होनेसे ) शुद्धरूप हैं और एक नय परमभावका ग्राही होनेसे भूतार्थ है ॥२६६॥
विशेषार्थ-पूर्वमें द्रव्यार्थिकनयके दस भेद कहे हैं। उनमेंसे पहला भेद कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिकनय है और दूसरा भेद है-सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिकनय । ये दोनों नय शुद्ध द्रव्यके ग्राही होनेसे शुद्ध रूप है। क्योंकि पहला भेद जोवके सिद्धस्वरूप शुद्धरूपको ग्रहण करता है और दूसरा भेद उत्पादव्ययको गौण करके सन्मात्रका ग्राहक है । इनके सिवाय एक भेद परमभावग्राही द्रव्याथिक नय है। यह नय शुद्ध और अशुद्ध उपचारसे रहित द्रव्यके स्वभावका ग्राहक है। मुमुक्षुको इसे हो जाननेका उपदेश ग्रन्थकारने गाथा १९८ के द्वारा दिया है । अतः ये तीनों नय भूतार्थ हैं। शेष नयोंका कथन व्यवहारमूलक है,अतः उन्हें भूतार्थ नहीं कहा। व्यवहारनय या तो अभेदरूप वस्तुका भेदमूलक कथन करता है या पराश्रित कथन करता है। अभेदरूप अखण्ड वस्तुमें भेद व्यवहार वास्तविक नहीं है। इसी तरह पराश्रितपना भी वस्तुका स्थायी शाश्वत स्वरूप नहीं है । अतः उन्हें अभूतार्थ कहा जाता है। भूतार्थ तो एकमात्र शाश्वत स्वाभाविक रूप है, वही ज्ञातव्य है,वही ध्येय है । यही बात आगे कहते हैं ।
जिस वस्तुका जो स्वभाव कहा है उसका प्रधानरूपसे वही द्रव्यरूप होता है, इसलिए निश्चयनयके द्वारा निश्चित अर्थकी ही ध्येय-ध्यान करनेके योग्य कहा है ।।२६७॥
विशेषार्थ-निश्चयनय आत्माके यथार्थ स्वाभाविक रूपको ही ग्रहण करता है । उसका वह स्वाभाविक रूप ही उपादेय होता है । उसीको प्राप्तिके लिए संसारी जीव प्रयत्न करता है । अतः वही स्वरूप ध्यान करनेके योग्य है। जो व्यक्ति जैसा होना चाहता है, वैसा ही सतत चिन्तन करता है । शुद्ध स्वर्णकी प्राप्तिका इच्छुक खानसे स्वर्णपाषाण प्राप्त करके भो पाषाणको उपादेय नहीं मानता, स्वर्णको ही उपादेय मानता है। अतः उसके लिए सबसे प्रथम तो उस दृष्टिको उपयोगिता है जो स्वर्णपाषाण दशामें भी शुद्ध स्वर्णकी पहचान कराती है। शुद्धस्वर्णकी पहचान हो जानेपर वह उसे अपनी दृष्टिसे ओझल नहीं होने देता और उसकी प्राप्तिके लिए प्रयत्नशील रहता है। इसी प्रकार मुमुक्ष भी निश्चय दष्टिके द्वारा कर्मलिप्त आत्मामें भी आत्माके यथार्य स्वरूपके दर्शन करके सतत उसीकी प्राप्तिके लिए प्रयत्नशील होता है। उसीका ध्यान करनेकी चेष्टामें रहता है और अपनी असमर्थतावश अन्य सविकल्प ध्यान करते हुए भी उसी आत्मरूपको एकमात्र ध्येय मानता है। तभी वह अपने ध्येयको प्राप्त करने में समर्थ होता है।
आगे युक्ति और अनुभवका काल कहते हैं।
तत्त्वको खोजते समय युक्तिमार्गके द्वारा आगमको बातको जानना चाहिए आराधनाके समय नहीं, क्योंकि अनुभव तो प्रत्यक्षका विषय है ।।२६८।।
१. तम्हा झेयं भणियं जं विसयं परमगाहिस्स- अ० क० ख० मु० । २. बुझेदि क० ख० ज०।।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org