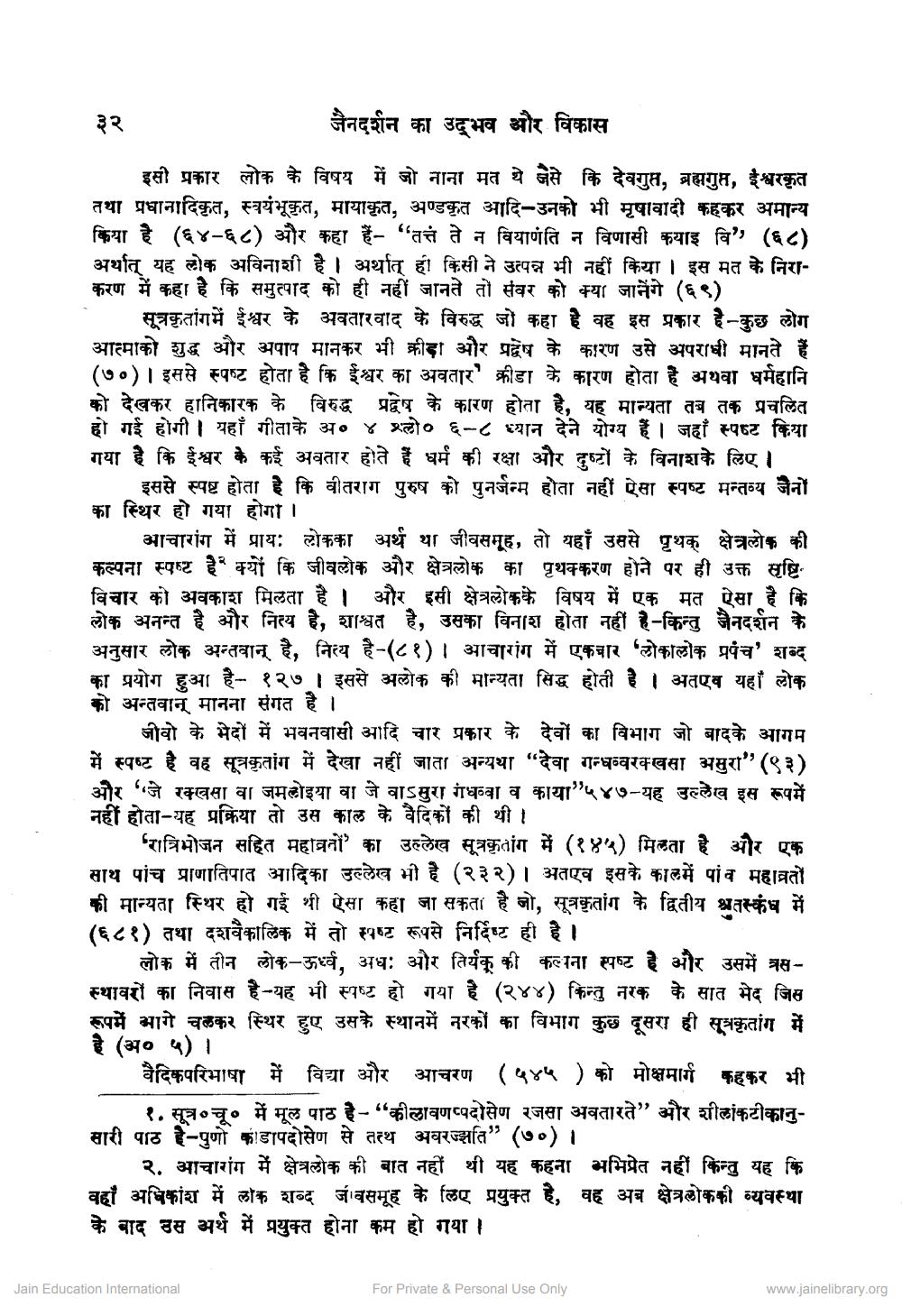________________
जैनदर्शन का उद्भव और विकास
इसी प्रकार लोक के विषय में जो नाना मत थे जैसे कि देवगुप्त, ब्रह्मगुप्त, ईश्वरकृत तथा प्रधानादिकृत, स्वयंभूकृत, मायाकृत, अण्डकृत आदि-उनको भी मृषावादी कहकर अमान्य किया है (६४-६८) और कहा हैं- "तत्तं ते न वियाणंति न विणासी कयाइ वि" (६८) अर्थात् यह लोक अविनाशी है। अर्थात् ही किसी ने उत्पन्न भी नहीं किया। इस मत के निराकरण में कहा है कि समुत्पाद को ही नहीं जानते तो संवर को क्या जानेंगे (६९) - सूत्रकृतांगमें ईश्वर के अवतारवाद के विरुद्ध जो कहा है वह इस प्रकार है-कुछ लोग
आत्माको शुद्ध और अपाप मानकर भी क्रीड़ा और प्रद्वेष के कारण उसे अपराधी मानते हैं (७०)। इससे स्पष्ट होता है कि ईश्वर का अवतार' क्रीडा के कारण होता है अथवा धर्महानि को देखकर हानिकारक के विरुद्ध प्रद्वेष के कारण होता है, यह मान्यता तब तक प्रचलित हो गई होगी। यहाँ गीताके अ० ४ श्लो० ६-८ ध्यान देने योग्य हैं । जहाँ स्पष्ट किया गया है कि ईश्वर के कई अवतार होते हैं धर्म की रक्षा और दुष्टों के विनाशके लिए।
इससे स्पष्ट होता है कि वीतराग पुरुष को पुनर्जन्म होता नहीं ऐसा स्पष्ट मन्तव्य जैनों का स्थिर हो गया होगा।
आचारांग में प्रायः लोकका अर्थ था जीवसमूह, तो यहाँ उससे पृथक् क्षेत्रलोक की कल्पना स्पष्ट है क्यों कि जीवलोक और क्षेत्रलोक का पृथक्करण होने पर ही उक्त सृष्टिः विचार को अवकाश मिलता है। और इसी क्षेत्रलोकके विषय में एक मत । लोक अनन्त है और नित्य है, शाश्वत है, उसका विनाश होता नहीं है-किन्तु जैनदर्शन के अनुसार लोक अन्तवान् है, नित्य है-(८१)। आचागंग में एकचार 'लोकालोक प्रपंच' शब्द का प्रयोग हुआ है- १२७ । इससे अलोक की मान्यता सिद्ध होती है । अतएव यहाँ लोक को अन्तवान् मानना संगत है।
जीवो के भेदों में भवनवासी आदि चार प्रकार के देवों का विभाग जो बादके आगम में स्पष्ट है वह सूत्रकृतांग में देखा नहीं जाता अन्यथा “देवा गन्धवरक्खसा असुरा" (९३)
और 'जे रक्खसा वा जमलोइया वा जे वाऽसुरा गंधवा व काया"५४७-यह उल्लेख इस रूप में नहीं होता-यह प्रक्रिया तो उस काल के वैदिकों की थी।
'रात्रिभोजन सहित महाव्रतों' का उल्लेख सूत्रकृतांग में (१४५) मिलता है और एक साथ पांच प्राणातिपात आदिका उल्लेख भी है (२३२)। अतएव इसके कालमें पांव महाव्रतो की मान्यता स्थिर हो गई थी ऐसा कहा जा सकता है जो, सूत्रकृतांग के द्वितीय श्रुतस्कंध में (६८१) तथा दशवकालिक में तो स्पष्ट रूपसे निर्दिष्ट ही है।
लोक में तीन लोक-ऊर्ध्व, अधः और तिर्यक् की कल्पना स्पष्ट है और उसमें सस्थावरों का निवास है-यह भी स्पष्ट हो गया है (२४४) किन्तु नरक के सात भेद जिस रूपमें आगे चलकर स्थिर हुए उसके स्थानमें नरकों का विभाग कुछ दूसरा ही सूत्रकृतांग में है (अ० ५)।
वैदिकपरिभाषा में विद्या और आचरण (५४५ ) को मोक्षमार्ग कहकर भी
१. सूत्र चू. में मूल पाठ है- “कीलावणप्पदोसेण रजसा अवतारते" और शीलांकटीकानुसारी पाठ है-पुणो कोडापदोसेण से तत्थ अवरज्झति” (७०)।
२. आचारांग में क्षेत्रलोक की बात नहीं थी यह कहना अभिप्रेत नहीं किन्तु यह कि वहाँ अधिकांश में लोक शब्द जीवसमूह के लिए प्रयुक्त है, वह अब क्षेत्रलोककी व्यवस्था के बाद उस अर्थ में प्रयुक्त होना कम हो गया।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org