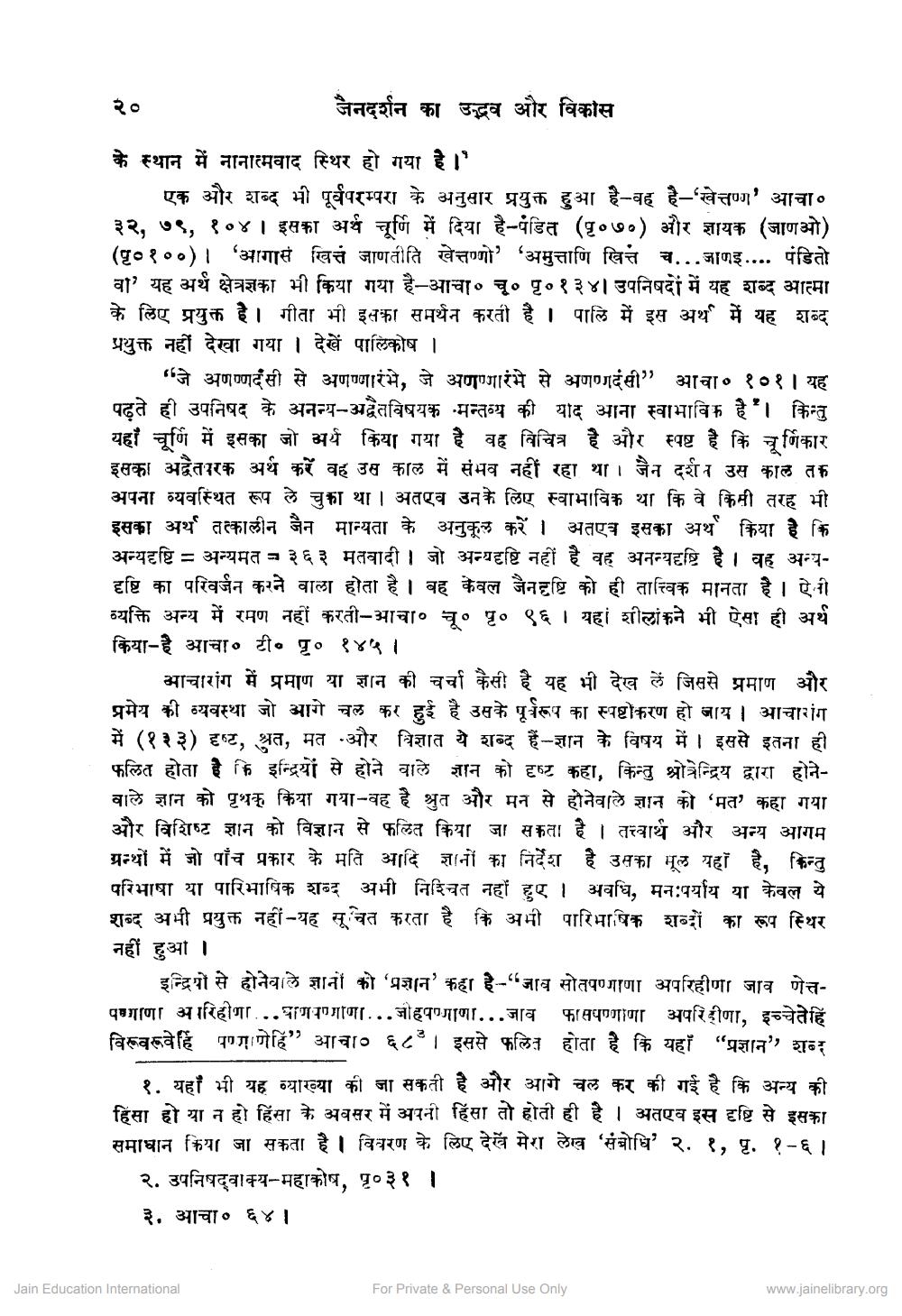________________
२०
जैनदर्शन का उद्भव और विकास के स्थान में नानात्मवाद स्थिर हो गया है।'
एक और शब्द भी पूर्वपरम्परा के अनुसार प्रयुक्त हुआ है-वह है-'खेत्तण्ण' आचा० ३२, ७९, १०४ । इसका अर्थ चूर्णि में दिया है-पंडित (पृ०७०) और ज्ञायक (जाणओ) (पृ०१००)। 'आगासं खित्तं जाणतीति खेत्तण्णो' 'अमुत्ताणि खित्तं च...जाणइ.... पंडितो वा' यह अर्थ क्षेत्रज्ञका भी किया गया है-आचा० चू० पृ० १३४। उपनिषदों में यह शब्द आत्मा के लिए प्रयुक्त है। गीता भी इसका समर्थन करती है । पालि में इस अर्थ में यह शब्द प्रयुक्त नहीं देखा गया । देखें पालिकोष ।
"जे अणण्णदंसी से अणण्णारंभे, जे अणण्णारंभे से अणण्णदंसी” आचा० १०१। यह पढ़ते ही उपनिषद के अनन्य-अद्वैतविषयक मन्तव्य की याद आना स्वाभाविक है। किन्तु यहाँ चूर्णि में इसका जो अर्थ किया गया है वह विचित्र है और स्पष्ट है कि चूर्णिकार इसका अद्वैतपरक अर्थ करें वह उस काल में संभव नहीं रहा था। जैन दर्शन उस काल तक अपना व्यवस्थित रूप ले चका था। अतएव उनके लिए स्वाभाविक था कि वे किमी तरह इसका अर्थ तत्कालीन जैन मान्यता के अनुकूल करें। अतएव इसका अर्थ किया है कि अन्यदृष्टि = अन्यमत - ३६३ मतवादी। जो अन्यदृष्टि नहीं है वह अनन्यदृष्टि है। वह अन्यदृष्टि का परिवर्जन करने वाला होता है । वह केवल जैन दृष्टि को ही तात्त्विक मानता है । ऐनी व्यक्ति अन्य में रमण नहीं करती-आचा० चू० पृ० ९६ । यहां शीलांकने भी ऐसा ही अर्थ किया-है आचा० टी० पृ० १४५।
आचारांग में प्रमाण या ज्ञान की चर्चा कैसी है यह भी देख लें जिससे प्रमाण और प्रमेय की व्यवस्था जो आगे चल कर हुई है उसके पूर्वरूप का स्पष्टोकरण हो जाय । आचागंग में (१३३) दृष्ट, श्रुत, मत और विज्ञात ये शब्द हैं-ज्ञान के विषय में । इससे इतना ही फलित होता है कि इन्द्रियों से होने वाले ज्ञान को दृष्ट कहा, किन्तु श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा होनेवाले ज्ञान को पृथक किया गया-वह है श्रुत और मन से होनेवाले ज्ञान को 'मत' कहा गया
और विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान से फलित किया जा सकता है । तत्त्वार्थ और अन्य आगम ग्रन्थों में जो पाँच प्रकार के मति आदि ज्ञानों का निर्देश है उसका मूल यहाँ है, किन्तु परिभाषा या पारिभाषिक शब्द अभी निश्चित नहीं हुए । अवधि, मन:पर्याय या केवल ये शब्द अभी प्रयुक्त नहीं-यह सूचित करता है कि अभी पारिभाषिक शब्दों का रूप स्थिर नहीं हुआ।
इन्द्रियों से होनेवाले ज्ञानों को 'प्रज्ञान' कहा है-“जाव सोतपण्णाणा अपरिहीणा जाव णेत्तपणाणा आरिहोणा...पाणपणाणा...जोहपण्णाणा...जाव फासपण्णाणा अपरिहीणा, इच्चेतेहिं विरूवरूवेहिं पागणेहिं” आचा० ६८। इससे फलित होता है कि यहाँ “प्रज्ञान' शब्द
१. यहाँ भी यह व्याख्या की जा सकती है और आगे चल कर की गई है कि अन्य की हिंसा हो या न हो हिंसा के अवसर में अपनी हिंसा तो होती ही है । अतएव इस दृष्टि से इसका समाधान किया जा सकता है । विवरण के लिए देखें मेरा लेख 'संबोधि' २. १, पृ. १-६ ।
२. उपनिषद्वाक्य-महाकोष, पृ०३१ । ३. आचा०६४।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org