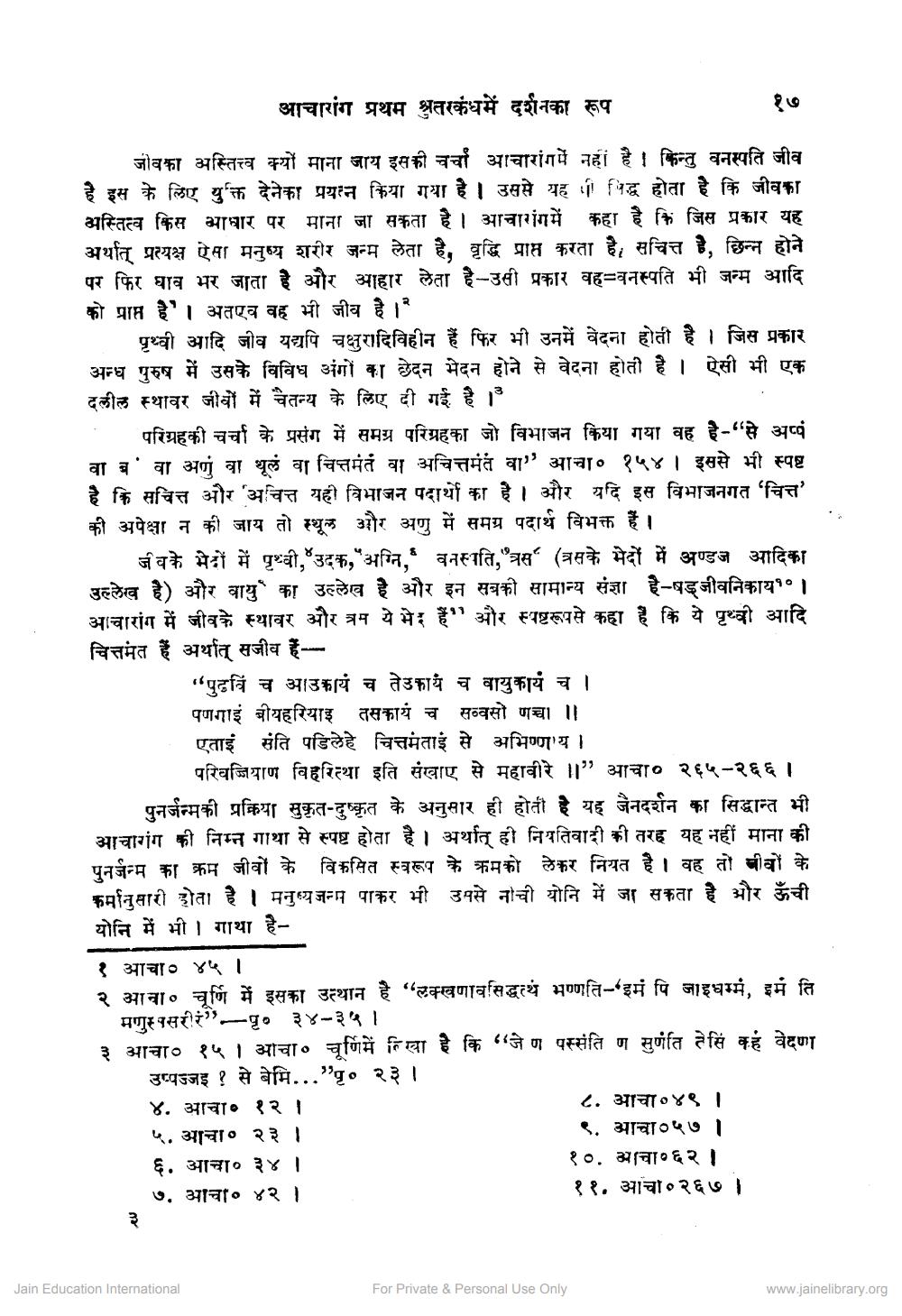________________
आचारांग प्रथम श्रुतरकंधमें दर्शनका रूप
जीवका अस्तित्त्व क्यों माना जाय इसकी चर्चा आचारांगमें नहीं है। किन्तु वनस्पति जीव है इस के लिए युक्ति देनेका प्रयत्न किया गया है। उससे यह पी पिद्ध होता है कि जीवका अस्तित्व किस आधार पर माना जा सकता है। आचागंगमें कहा है कि जिस प्रकार यह अर्थात् प्रत्यक्ष ऐसा मनुष्य शरीर जन्म लेता है, वृद्धि प्राप्त करता है। सचित्त है, छिन्न होने पर फिर घाव भर जाता है और आहार लेता है-उसी प्रकार वह वनस्पति भी जन्म आदि को प्राप्त है। अतएव वह भी जीव है । _ पृथ्वी आदि जीव यद्यपि चक्षुरादिविहीन हैं फिर भी उनमें वेदना होती है । जिस प्रकार अन्ध पुरुष में उसके विविध अंगों का छेदन भेदन होने से वेदना होती है । ऐसी भी एक दलील स्थावर जीवों में चैतन्य के लिए दी गई. है ।।
परिग्रहकी चर्चा के प्रसंग में समग्र परिग्रहका जो विभाजन किया गया वह है-"से अप्पं वा ब वा अणुं वा थूलं वा चित्तमंतं वा अचित्तमंत वा" आचा० १५४ । इससे भी स्पष्ट है कि सचित्त और 'अचित्त यही विभाजन पदार्थो का है। और यदि इस विभाजनगत 'चित्त' की अपेक्षा न की जाय तो स्थूल और अणु में समग्र पदार्थ विभक्त हैं।
जवके भेदों में पृथ्वी, उदक, अग्नि, वनस्पति,"त्रस' (त्रसके भेदों में अण्डज आदिका उल्लेख है) और वायु का उल्लेख है और इन सबको सामान्य संज्ञा है-षड्जीवनिकाय१० । आचारांग में जीवके स्थावर और त्रम ये भेद हैं" और स्पष्टरूपसे कहा है कि ये पृथ्वी आदि चित्तमंत हैं अर्थात् सजीव हैं---
"पुढविं च आउकायं च तेउकाय च वायुकायं च । पणगाइं बीयहरियाइ तसकायं च सव्वसो णच्च। ॥ एताई संति पडिलेहे चित्तमंताई से अभिण्ण' य ।
परिवज्जियाण विहरित्था इति संखाए से महावीरे ॥" आचा० २६५-२६६। पुनर्जन्मकी प्रक्रिया सुकृत-दुष्कृत के अनुसार ही होती है यह जैनदर्शन का सिद्धान्त भी आचागंग की निम्न गाथा से स्पष्ट होता है । अर्थात् ही नियतिवादी की तरह यह नहीं माना की पुनर्जन्म का क्रम जीवों के विकसित स्वरूप के क्रमको लेकर नियत है। वह तो बीवों के कर्मानुसारी होता है । मनुष्य जन्म पाकर भी उससे नोची योनि में जा सकता है और ऊँची योनि में भी। गाथा है१ आचा० ४५ ।। २ आना० चर्णि में इसका उत्थान है "लक्खणावसिद्धत्थं भण्णति-'इमं पि जाइधम्मं. इमं ति
मणुस्ससरीरं"-पृ. ३४-३५ । ३ आचा० १५ । आचा० चूर्णिमें लिखा है कि "जे ण पस्संति ण सुगंति तेसिं कहं वेदणा
उप्पज्जइ ? से बेमि..."पृ० २३ । ४. आचा० १२ ।
८. आचा०४९ । ५. आचा० २३ ।
९. आचा०५७ । ६. आचा० ३४ ।
१०. आचा०६२। ७. आचा० ४२ ।
११. आचा०२६७ ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org