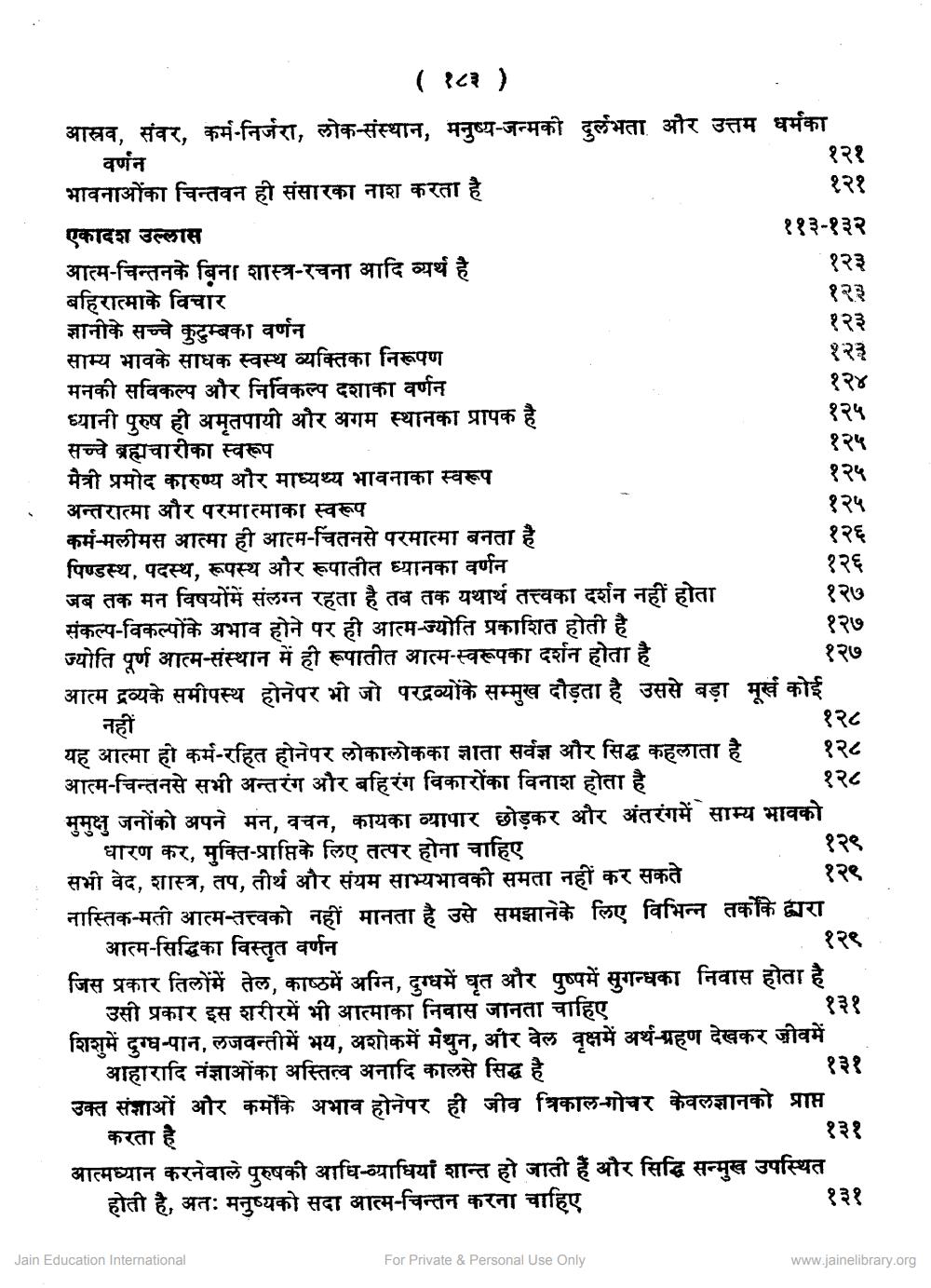________________
( १८३ ) आस्रव, संवर, कर्म-निर्जरा, लोक-संस्थान, मनुष्य-जन्मको दुर्लभता और उत्तम धर्मका वर्णन
१२१ भावनाओंका चिन्तवन ही संसारका नाश करता है
१२१ एकादश उल्लास
११३-१३२ आत्म-चिन्तनके बिना शास्त्र-रचना आदि व्यर्थ है
१२३ बहिरात्माके विचार ज्ञानीके सच्चे कुटुम्बका वर्णन
१२३ साम्य भावके साधक स्वस्थ व्यक्तिका निरूपण
१२३ मनकी सविकल्प और निर्विकल्प दशाका वर्णन
१२४ ध्यानी पुरुष ही अमृतपायी और अगम स्थानका प्रापक है
१२५ सच्चे ब्रह्मचारीका स्वरूप
१२५ मैत्री प्रमोद कारुण्य और माध्यथ्य भावनाका स्वरूप
१२५ अन्तरात्मा और परमात्माका स्वरूप
१२५ कर्म-मलीमस आत्मा ही आत्म-चिंतनसे परमात्मा बनता है
१२६ पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यानका वर्णन
१२६ जब तक मन विषयोंमें संलग्न रहता है तब तक यथार्थ तत्त्वका दर्शन नहीं होता
१२७ संकल्प-विकल्पोंके अभाव होने पर ही आत्म-ज्योति प्रकाशित होती है।
१२७ ज्योति पूर्ण आत्म-संस्थान में ही रूपातीत आत्म-स्वरूपका दर्शन होता है
१२७ आत्म द्रव्यके समीपस्थ होनेपर भी जो परद्रव्योंके सम्मुख दौड़ता है उससे बड़ा मूर्ख कोई
१२८ यह आत्मा हो कर्म-रहित होनेपर लोकालोकका ज्ञाता सर्वज्ञ और सिद्ध कहलाता है १२८ आत्म-चिन्तनसे सभी अन्तरंग और बहिरंग विकारोंका विनाश होता है
१२८ मुमुक्षु जनोंको अपने मन, वचन, कायका व्यापार छोड़कर और अंतरंगमें साम्य भावको ___ धारण कर, मुक्ति-प्राप्तिके लिए तत्पर होना चाहिए सभी वेद, शास्त्र, तप, तीर्थ और संयम साभ्यभावकी समता नहीं कर सकते नास्तिक-मती आत्म-तत्त्वको नहीं मानता है उसे समझानेके लिए विभिन्न तर्कोके द्वारा आत्म-सिद्धिका विस्तृत वर्णन
. १२९ जिस प्रकार तिलोंमें तेल, काष्ठमें अग्नि, दुग्धमें घृत और पुष्पमें सुगन्धका निवास होता है।
उसी प्रकार इस शरीरमें भी आत्माका निवास जानता चाहिए शिशुमें दुग्ध-पान, लजवन्तीमें भय, अशोकमें मथुन, और वेल वृक्षमें अर्थ-ग्रहण देखकर जीवमें आहारादि नंज्ञाओंका अस्तित्व अनादि कालसे सिद्ध है
१३१ उक्त संज्ञाओं और कर्मोंके अभाव होनेपर ही जीव त्रिकाल-गोचर केवलज्ञानको प्राप्त _करता है आत्मध्यान करनेवाले पुरुषकी आधि-व्याधियां शान्त हो जाती हैं और सिद्धि सन्मुख उपस्थित होती है, अतः मनुष्यको सदा आत्म-चिन्तन करना चाहिए
१३१
नहीं
१२९
१३१
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org