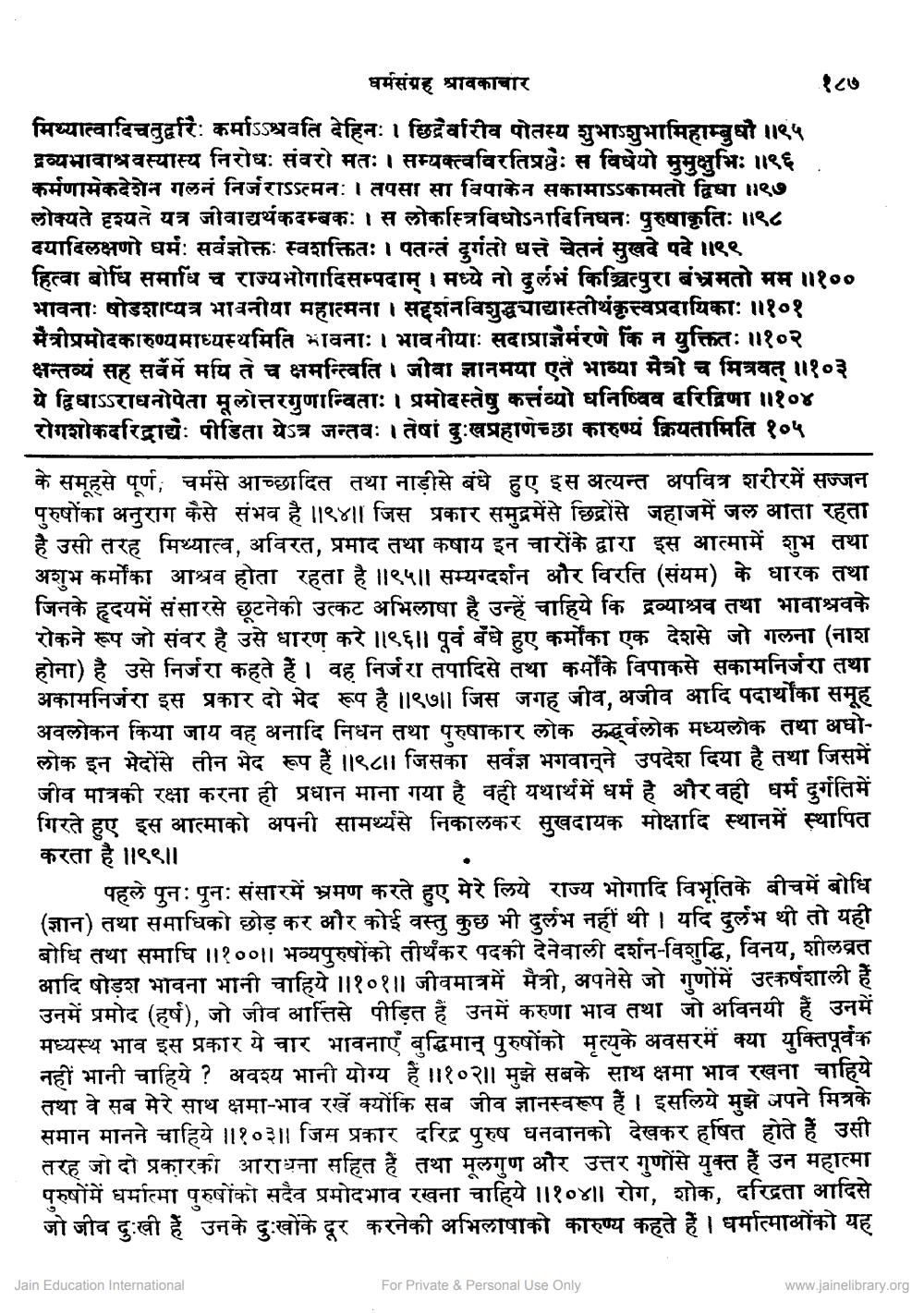________________
१८७
धर्मसंग्रह श्रावकाचार मिथ्यात्वादिचतुरैः कर्माऽऽश्रवति देहिनः । छिट्टैारीव पोतस्य शुभाशुभामिहाम्बुधौ ॥९५ द्रव्यभावाश्रवस्यास्य निरोधः संवरो मतः । सम्यक्त्वविरतिप्रष्टैः स विधेयो मुमुक्षुभिः ॥९६ . कर्मणामेकदेशेन गलनं निर्जराऽऽत्मनः । तपसा सा विपाकेन सकामाऽऽकामतो द्विधा ॥९७ लोक्यते दृश्यते यत्र जीवाद्यर्थकदम्बकः । स लोकस्त्रिविधोऽनादिनिधनः पुरुषाकृतिः ॥९८ दयादिलक्षणो धर्मः सर्वज्ञोक्तः स्वशक्तितः । पतन्तं दुर्गतो धत्ते चेतनं सुखदे पदे ॥९९ हित्वा बोधि समाधि च राज्यभोगादिसम्पदाम् । मध्ये नो दुर्लभं किञ्चित्पुरा बंभ्रमतो मम ॥१०० भावनाः षोडशाप्यत्र भावनीया महात्मना । सद्दर्शनविशुद्धयाद्यास्तीथंकृत्त्वप्रदायिकाः ॥१०१ मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थमिति भावनाः । भावनीयाः सदाप्राज्ञैर्मरणे किं न युक्तितः ॥१०२ क्षन्तव्यं सह सर्वैर्मे मयि ते च क्षमन्त्विति । जीवा ज्ञानमया एते भाव्या मैत्री च मित्रवत् ॥१०३ ये द्विधाऽऽराधनोपेता मूलोत्तरगुणान्विताः। प्रमोदस्तेषु कर्तव्यो धनिष्विव दरिद्रिणा ॥१०४ रोगशोकदरिद्रायः पीडिता येऽत्र जन्तवः । तेषां दुःखप्रहाणेच्छा कारुण्यं क्रियतामिति १०५ के समूहसे पूर्ण, चर्मसे आच्छादित तथा नाड़ीसे बंधे हुए इस अत्यन्त अपवित्र शरीरमें सज्जन पुरुषोंका अनुराग कैसे संभव है ।।१४।। जिस प्रकार समुद्रमेंसे छिद्रोंसे जहाजमें जल आता रहता है उसी तरह मिथ्यात्व, अविरत, प्रमाद तथा कषाय इन चारोंके द्वारा इस आत्मामें शुभ तथा अशुभ कर्मोंका आश्रव होता रहता है ।।९५।। सम्यग्दर्शन और विरति (संयम) के धारक तथा जिनके हृदयमें संसारसे छूटनेको उत्कट अभिलाषा है उन्हें चाहिये कि द्रव्याश्रव तथा भावाश्रवके रोकने रूप जो संवर है उसे धारण करे ॥९६|| पूर्व बँधे हुए कर्मोका एक देशसे जो गलना (नाश होना) है उसे निर्जरा कहते हैं। वह निर्जरा तपादिसे तथा कर्मोंके विपाकसे सकामनिर्जरा तथा अकामनिर्जरा इस प्रकार दो भेद रूप है ॥९७|| जिस जगह जीव, अजीव आदि पदार्थीका समूह अवलोकन किया जाय वह अनादि निधन तथा परुषाकार लोक उद्धर्वलोक मध्यलोक तथा अधोलोक इन भेदोंसे तीन भेद रूप हैं ॥९८। जिसका सर्वज्ञ भगवान्ने उपदेश दिया है तथा जिसमें जीव मात्रकी रक्षा करना ही प्रधान माना गया है वही यथार्थ में धर्म है और वही धर्म दुर्गतिमें गिरते हुए इस आत्माको अपनी सामर्थ्य से निकालकर सुखदायक मोक्षादि स्थानमें स्थापित करता है ॥१९॥
पहले पुनः पुनः संसारमें भ्रमण करते हुए मेरे लिये राज्य भोगादि विभूतिके बीच में बोधि (ज्ञान) तथा समाधिको छोड़ कर और कोई वस्तु कुछ भी दुर्लभ नहीं थी। यदि दुर्लभ थी तो यही बोधि तथा समाधि ॥१००।। भव्यपुरुषोंको तीर्थंकर पदकी देनेवाली दर्शन-विशुद्धि, विनय, शीलव्रत आदि षोड़श भावना भानी चाहिये ॥१०१॥ जीवमात्रमें मैत्री, अपनेसे जो गुणोंमें उत्कर्षशाली हैं उनमें प्रमोद (हर्ष), जो जीव आत्तिसे पीड़ित हैं उनमें करुणा भाव तथा जो अविनयी हैं उनमें मध्यस्थ भाव इस प्रकार ये चार भावनाएँ बुद्धिमान् पुरुषोंको मृत्युके अवसरमें क्या युक्तिपूर्वक नहीं भानी चाहिये ? अवश्य भानी योग्य हैं ॥१०२॥ मुझे सबके साथ क्षमा भाव रखना चाहिये तथा वे सब मेरे साथ क्षमा-भाव रखें क्योंकि सब जीव ज्ञानस्वरूप हैं । इसलिये मुझे अपने मित्रके समान मानने चाहिये ॥१०३।। जिस प्रकार दरिद्र पुरुष धनवानको देखकर हर्षित होते हैं उसी तरह जो दो प्रकारको आराधना सहित हैं तथा मूलगुण और उत्तर गुणोंसे युक्त हैं उन महात्मा पुरुषोंमें धर्मात्मा पुरुषोंको सदैव प्रमोदभाव रखना चाहिये ।।१०४॥ रोग, शोक, दरिद्रता आदिसे जो जीव दुःखी हैं उनके दुःखोंके दूर करनेकी अभिलाषाको कारुण्य कहते हैं । धर्मात्माओंको यह
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org