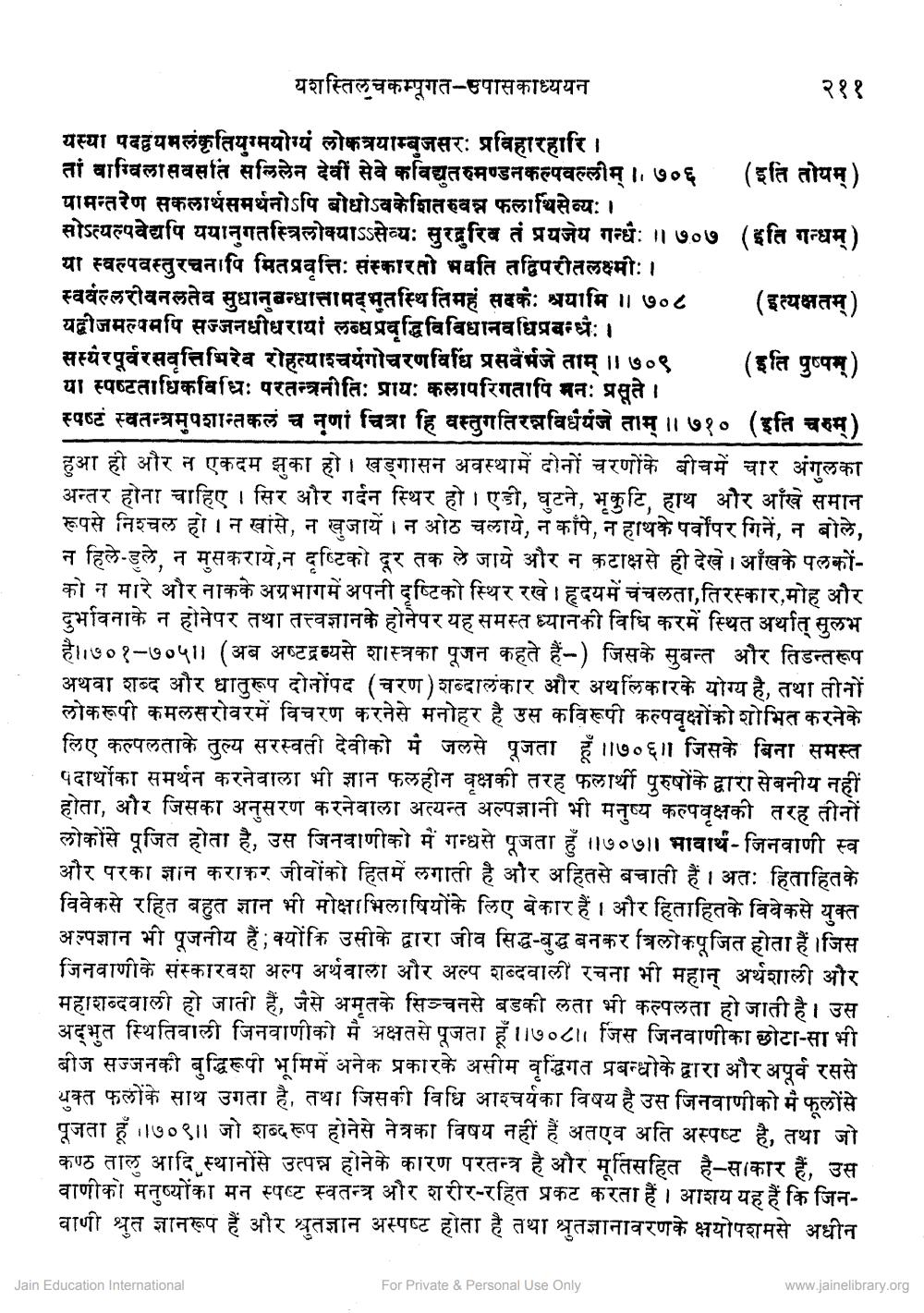________________
यशस्तिलचकम्पूगत - उपासकाध्ययन
यस्यापदद्वयमलंकृतियुग्मयोग्यं लोकत्रयाम्बुजसरः प्रविहारहारि ।
( इति तोयम् )
तां वाग्विलासवसति सलिलेन देवीं सेवे कविद्युतरुमण्डन कल्पवल्लीम् । ७०६ यामन्तरेण सकलार्थसमर्थनोऽपि बोधोऽव केशितरुवन्न फलाथिसेव्यः । सोऽत्यल्पवेद्यपि ययानुगतस्त्रिलोक्याऽऽसेव्यः सुरनुरिव तं प्रयजेय गन्धैः ।। ७०७ ( इति गन्धम् ) या स्वल्पवस्तुरचनापि मितप्रवृत्तिः संस्कारतो भवति तद्विपरीतलक्ष्मीः । स्वयंल्लरीवनलतेव सुधानुबन्धात्तामद्भुत स्थितिमहं सदकैः श्रयामि ।। ७०८ यद्वीजमल्पमपि सज्जनधीधरायां लब्ध प्रवृद्धि विविधानवधिप्रबन्धैः ।
( इत्यक्षतम् )
( इति पुष्पम् )
( इति चरुम् )
सस्यैर पूर्व रसवृत्तिभिरेव रोहत्याश्चयंगोचरणविधि प्रसवैर्भजे ताम् ।। ७०९ या स्पष्टताधिकविधिः परतन्त्रनीतिः प्रायः कलापरिगतापि मनः प्रसूते । स्पष्टं स्वतन्त्रमुपशान्तकलं च नृणां चित्रा हि वस्तुगतिरन्नविर्धयंजे ताम् ।। ७१० हुआ हो और न एकदम झुका हो । खड्गासन अवस्थामें दोनों चरणोंके बीच में चार अंगुलका अन्तर होना चाहिए । सिर और गर्दन स्थिर हो । एडी, घुटने, भृकुटि, हाथ और आँखे समान रूपसे निश्चल हो । न खांसे, न खुजायें। न ओठ चलाये, न काँपे, न हाथ के पर्वोपर गिनें, न बोले, न हिले-डुले, न मुसकराये, न दृष्टिको दूर तक ले जाये और न कटाक्षसे ही देखे । आँखके पलकोंको न मारे और नाकके अग्रभाग में अपनी दृष्टिको स्थिर रखे। हृदय में चंचलता, तिरस्कार, मोह और दुर्भावनाके न होनेपर तथा तत्त्वज्ञानके होनेपर यह समस्त ध्यानकी विधि करमें स्थित अर्थात् सुलभ है । । ७०१ - ७०५ ।। ( अब अष्टद्रव्यसे शास्त्रका पूजन कहते हैं -) जिसके सुबन्त और तिङन्तरूप अथवा शब्द और धातुरूप दोनोंपद (चरण) शब्दालंकार और अथलिकारके योग्य है, तथा तीनों लोकरूपी कमलसरोवरमें विचरण करनेसे मनोहर है उस कविरूपी कल्पवृक्षों को शोभित करने के लिए कल्पलताके तुल्य सरस्वती देवीको में जलसे पूजता हूँ ||७०६ || जिसके बिना समस्त पदार्थो का समर्थन करनेवाला भी ज्ञान फलहीन वृक्षकी तरह फलार्थी पुरुषोंके द्वारा सेबनीय नहीं होता, और जिसका अनुसरण करनेवाला अत्यन्त अल्पज्ञानी भी मनुष्य कल्पवृक्षकी तरह तीनों लोकोंसे पूजित होता है, उस जिनवाणीको में गन्धसे पूजता हूँ ।। ७०७ ।। भावार्थ - जिनवाणी स्व और परका ज्ञान कराकर जीवोंको हितमें लगाती है और अहितसे बचाती हैं। अतः हिताहित के विवेकसे रहित बहुत ज्ञान भी मोक्षाभिलाषियोंके लिए बेकार हैं । और हिताहितके विवेकसे युक्त अल्पज्ञान भी पूजनीय हैं; क्योंकि उसीके द्वारा जीव सिद्ध-बुद्ध बनकर त्रिलोकपूजित होता हैं । जिस जिनवाणी के संस्कारवश अल्प अर्थवाला और अल्प शब्दवाली रचना भी महान् अर्थशाली और महाशब्दवाली हो जाती हैं, जैसे अमृतके सिञ्चनसे बडकी लता भी कल्पलता हो जाती है । उस अद्भुत स्थितिवाली जिनवाणीको मै अक्षतसे पूजता हूँ ।। ७०८ || जिस जिनवाणीका छोटा-सा भी बीज सज्जनकी बुद्धिरूपी भूमिमें अनेक प्रकारके असीम वृद्धिंगत प्रबन्धोके द्वारा और अपूर्व रससे युक्त फलोंके साथ उगता है, तथा जिसकी विधि आश्चर्यका विषय है उस जिनवाणीको में फूलोंसे पूजता हूँ ।। ७०९ || जो शब्दरूप होनेसे नेत्रका विषय नहीं हैं अतएव अति अस्पष्ट है, तथा जो कण्ठ तालु आदि स्थानोंसे उत्पन्न होनेके कारण परतन्त्र है और मूर्तिसहित है- साकार हैं, उस वाणीको मनुष्यों का मन स्पष्ट स्वतन्त्र और शरीर - रहित प्रकट करता हैं। आशय यह हैं कि जिनवाणी श्रुत ज्ञानरूप हैं और श्रुतज्ञान अस्पष्ट होता है तथा श्रुतज्ञानावरण के क्षयोपशमसे अधीन
Jain Education International
२११
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org