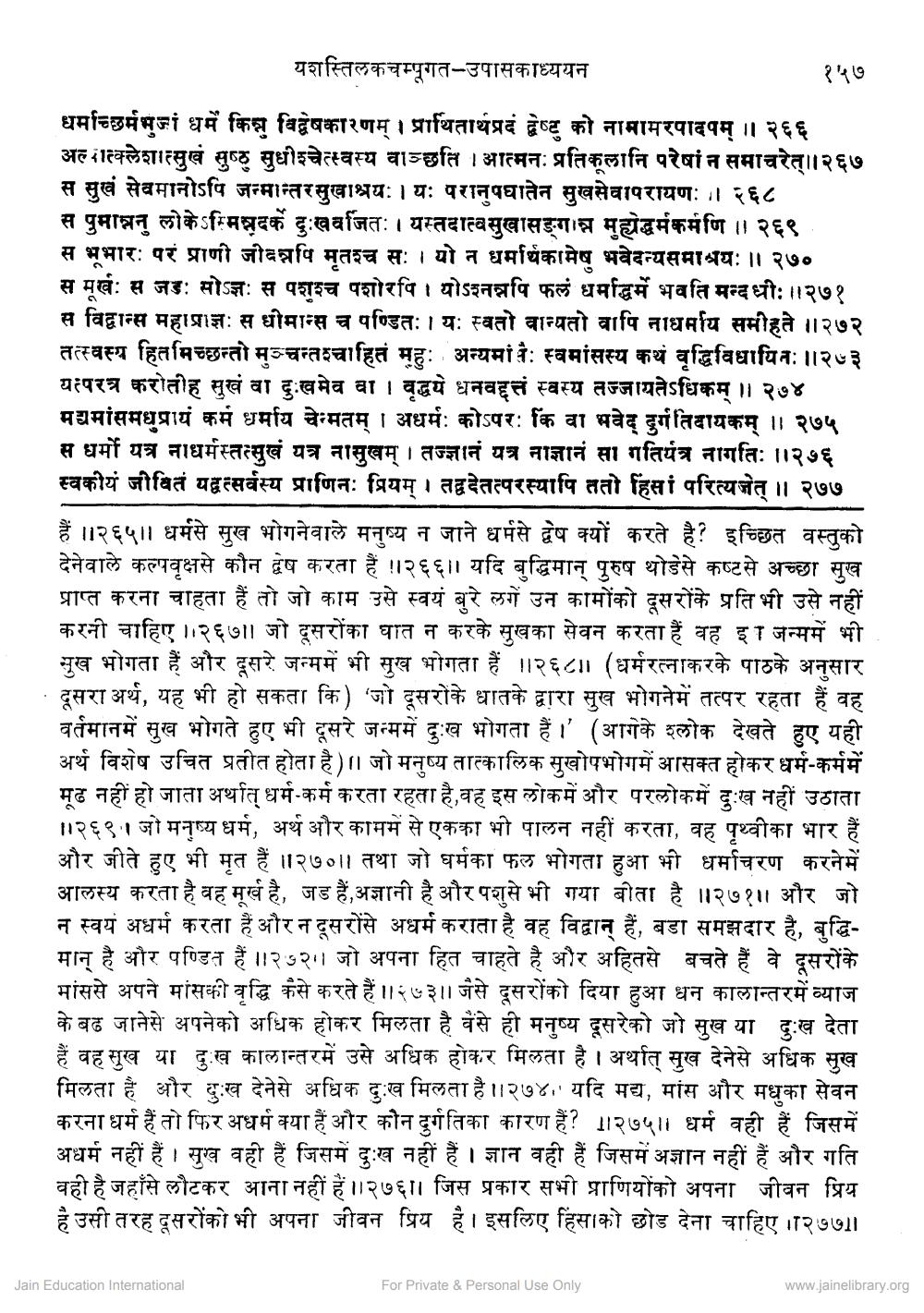________________
१५७
यशस्तिलकचम्पूगत-उपासकाध्ययन धर्माच्छमभुजां धर्म किन्न विद्वेषकारणम् । प्राथितार्थप्रदं द्वेष्टु को नामामरपादपम् ।। २६६ अल्वात्क्लेशात्सुखं सुष्ठ सुधीश्चेत्स्वस्य वाञ्छति । आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्।।२६७ स सुखं सेवमानोऽपि जन्मान्तरसुखाश्रयः । यः परानुपघातेन सुखसेवापरायणः ।। २६८ स पुमान्ननु लोकेऽस्मिन्नदर्के दुःखजितः । यस्तदात्वसुखासगान मुह्येद्धर्मकर्मणि ।। २६९ स भूभारः परं प्राणी जीवन्नपि मृतश्च सः । यो न धर्मार्थकामेषु भवेदन्यसमाश्रयः ।। २७० स मूर्खः स जड: सोऽज्ञः स पशश्च पशोरपि । योऽश्नन्नपि फलं धर्माद्धर्मे भवति मन्दधीः ॥२७१ स विद्वान्स महाप्राज्ञः स धीमान्स च पण्डितः । यः स्वतो वान्यतो वापि नाधर्माय समीहते ॥२७२ तत्स्वस्य हितमिच्छन्तो मुञ्चन्तश्चाहितं महः अन्यमांः स्वमांसस्य कथं वृद्धिविधायिनः ॥२७३ यत्परत्र करोतीह सुखं वा दुःखमेव वा । वृद्धये धनवद्दत्तं स्वस्य तज्जायतेऽधिकम् ।। २७४ मद्यमांसमधुप्रायं कर्म धर्माय चेन्मतम् । अधर्मः कोऽपर: किं वा भवेद् दुर्गतिदायकम् ।। २७५ स धर्मो यत्र नाधर्मस्तत्सुखं यत्र नासुखम् । तज्ज्ञानं यत्र नाज्ञानं सा गतिर्यत्र नागतिः ।।२७६ स्वकीयं जीवितं यद्वत्सर्वस्य प्राणिनः प्रियम् । तदेतत्परस्यापि ततो हिसां परित्यजेत् ।। २७७ हैं ॥२६५।। धर्मसे सुख भोगनेवाले मनुष्य न जाने धर्मसे द्वेष क्यों करते है? इच्छित वस्तुको देनेवाले कल्पवृक्षसे कौन द्वेष करता हैं !।२६६।। यदि बुद्धिमान् पुरुष थोडेसे कष्ट से अच्छा सुख प्राप्त करना चाहता हैं तो जो काम उसे स्वयं बुरे लगें उन कामोंको दूसरोंके प्रति भी उसे नहीं करनी चाहिए ।२६७।। जो दूसरोंका घात न करके सुखका सेवन करता हैं वह इा जन्ममें भी सुख भोगता हैं और दूसरे जन्ममें भी सुख भोगता हैं ॥२६८।। (धर्मरत्नाकरके पाठके अनुसार दूसरा अर्थ, यह भी हो सकता कि) 'जो दूसरोंके धातके द्वारा सुख भोगनेमें तत्पर रहता हैं वह वर्तमानमें सुख भोगते हुए भी दूसरे जन्ममें दुःख भोगता हैं।' (आगेके श्लोक देखते हुए यही अर्थ विशेष उचित प्रतीत होता है)।। जो मनुष्य तात्कालिक सुखोपभोगमें आसक्त होकर धर्म-कर्ममें मूढ नहीं हो जाता अर्थात् धर्म-कर्म करता रहता है,वह इस लोकमें और परलोकमें दुःख नहीं उठाता ॥२६९ । जो मनुष्य धर्म, अर्थ और काममें से एकका भी पालन नहीं करता, वह पृथ्वीका भार हैं और जीते हुए भी मृत हैं ।।२७०।। तथा जो धर्मका फल भोगता हुआ भी धर्माचरण करने में आलस्य करता है वह मूर्ख है, जड हैं,अज्ञानी है और पशुसे भी गया बीता है ॥२७१।। और जो न स्वयं अधर्म करता हैं और न दूसरोंसे अधर्म कराता है वह विद्वान् हैं, बडा समझदार है, बुद्धिमान् है और पण्डित हैं ।।२७२।। जो अपना हित चाहते है और अहितसे बचते हैं वे दूसरोंके मांससे अपने मांसकी वृद्धि कैसे करते हैं ।।२७३।। जैसे दूसरोंको दिया हुआ धन कालान्तरमें व्याज के बढ जानेसे अपनेको अधिक होकर मिलता है वैसे ही मनुष्य दूसरेको जो सुख या दुःख देता हैं वह सूख या दुःख कालान्तरमें उसे अधिक होकर मिलता है। अर्थात सुख देनेसे अधिक सख मिलता है और दुःख देनेसे अधिक दुःख मिलता है।।२७४.' यदि मद्य, मांस और मधुका सेवन करना धर्म हैं तो फिर अधर्म क्या हैं और कौन दुर्गतिका कारण हैं? ॥२७५।। धर्म वही हैं जिसमें अधर्म नहीं हैं। सुख वही हैं जिसमें दुःख नहीं हैं । ज्ञान वही हैं जिसमें अज्ञान नहीं हैं और गति वही है जहाँसे लौटकर आना नहीं हैं।२७६।। जिस प्रकार सभी प्राणियोंको अपना जीवन प्रिय है उसी तरह दूसरोंको भी अपना जीवन प्रिय है। इसलिए हिंसाको छोड देना चाहिए ।।२७७॥
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org