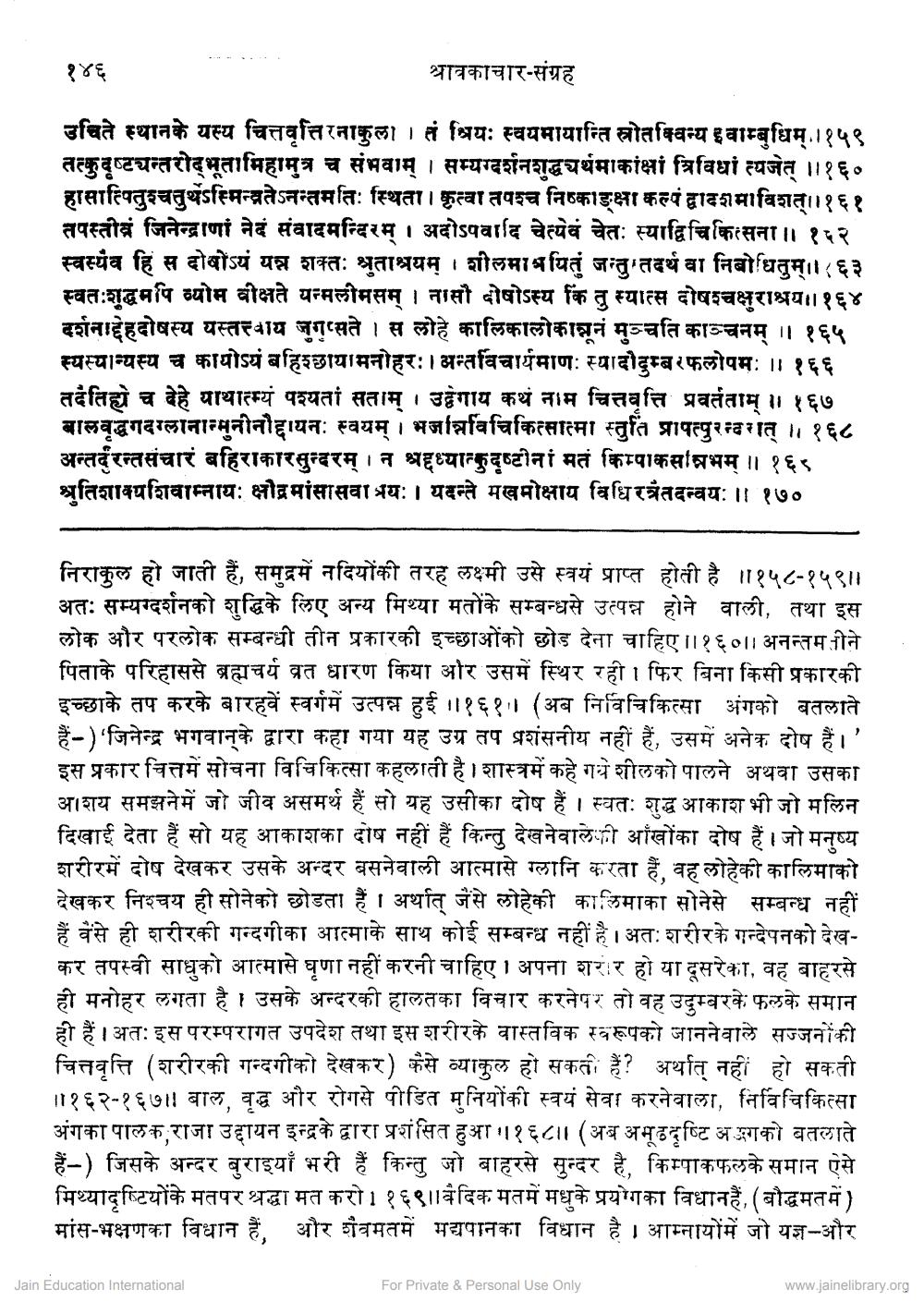________________
१४६
श्रावकाचार-संग्रह
उचिते स्थानके यस्य चित्तवृत्तिरनाकुला । तं श्रियः स्वयमायान्ति स्रोतक्विन्य इवाम्बुधिम् । १५९ तत्कुदृष्टयन्तरोद्भूतामिहामुत्र च संभवाम् । सम्यग्दर्शनशुद्धयर्थमाकांक्षां विविधां त्यजेत् ।।१६० हासास्पितुश्चतुर्थेऽस्मिन्व्रतेऽनन्तमतिः स्थिता। कृत्वा तपश्च निष्काक्षा कल्पं द्वादशमाविशत्।।१६१ तपस्तीवं जिनेन्द्राणां नेदं संवादमन्दिरम् । अदोऽपवादि चेत्येवं चेतः स्याद्विचिकित्सना ।। १६२ स्वस्यैव हि स दोवोऽयं यन्न शक्तः श्रुताश्रयम् । शीलमाश्रयितुं जन्तु तदर्थ वा निबोधितुम्।।१६३ स्वतःशद्धमपि व्योम वीक्षते यन्मलीमसम् । नासौ दोषोऽस्य किं तु स्यात्स दोषश्चक्षुराश्रय।।१६४ दर्शनाद्देहदोषस्य यस्तत्त्वाय जगप्सते । स लोहे कालिकालोकानूनं मुञ्चति काञ्चनम् ।। १६५ स्यस्यान्यस्य च कायोऽयं बहिश्छायामनोहरः । अन्तविचार्यमाणः स्यादोदुम्बरफलोपमः ।। १६६ तदैतिह्ये च देहे याथात्म्यं पश्यतां सताम् । उद्वेगाय कथं नाम चित्तवृत्ति प्रवर्तताम् ।। १६७ बालवृद्धगदग्लानान्मुनीनौद्दायनः स्वयम् । भन्निविचिकित्सात्मा स्तुति प्रापत्पुरत्वगत् ।। १६८ अन्तर्दुरन्तसंचारं बहिराकारसुन्दरम् । न श्रद्दध्यात्कुदृष्टीनां मतं किम्पाकसन्निभम् ।। १६९ श्रुतिशाक्यशिवाम्नायः क्षौद्रमांसासवा प्रयः । यदन्ते मखमोक्षाय विधिरत्रैतदन्वयः ॥ १७०
निराकुल हो जाती हैं, समुद्र में नदियोंकी तरह लक्ष्मी उसे स्वयं प्राप्त होती है ॥१५८-१५९॥ अतः सम्यग्दर्शनको शुद्धिके लिए अन्य मिथ्या मतोंके सम्बन्धसे उत्पन्न होने वाली, तथा इस लोक और परलोक सम्बन्धी तीन प्रकारकी इच्छाओंको छोड देना चाहिए ।।१६०।। अनन्तम तीने पिताके परिहाससे ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया और उसमें स्थिर रही। फिर बिना किसी प्रकारकी इच्छाके तप करके बारहवें स्वर्गमें उत्पन्न हुई ।।१६१ । (अब निविचिकित्सा अंगको बतलाते हैं-) जिनेन्द्र भगवान्के द्वारा कहा गया यह उग्र तप प्रशंसनीय नहीं हैं, उसमें अनेक दोष हैं।' इस प्रकार चित्तमें सोचना विचिकित्सा कहलाती है। शास्त्रमें कहे गये शीलको पालने अथवा उसका आशय समझने में जो जीव असमर्थ हैं सो यह उसीका दोष हैं । स्वतः शुद्ध आकाश भी जो मलिन दिखाई देता हैं सो यह आकाशका दोष नहीं हैं किन्तु देखनेवालेकी आँखोंका दोष हैं। जो मनुष्य शरीरमें दोष देखकर उसके अन्दर बसनेवाली आत्मासे ग्लानि करता हैं, वह लोहेकी कालिमाको देखकर निश्चय ही सोनेको छोडता हैं । अर्थात् जैसे लोहेकी कालिमाका सोनेसे सम्बन्ध नहीं हैं वैसे ही शरीरकी गन्दगीका आत्माके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । अतः शरीरके गन्देपनको देखकर तपस्वी साधुको आत्मासे घृणा नहीं करनी चाहिए । अपना शरीर हो या दूसरेका, वह बाहरसे ही मनोहर लगता है। उसके अन्दरकी हालतका विचार करने पर तो वह उदुम्बरके फलके समान ही हैं । अतः इस परम्परागत उपदेश तथा इस शरीरके वास्तविक स्वरूपको जाननेवाले सज्जनोंकी चित्तवृत्ति (शरीरकी गन्दगीको देखकर) कैसे व्याकुल हो सकती हैं? अर्थात् नहीं हो सकती ॥१६२-१६७।। बाल, वृद्ध और रोगसे पीडित मुनियोंकी स्वयं सेवा करनेवाला, निर्विचिकित्सा अंगका पालक,राजा उद्दायन इन्द्रके द्वारा प्रशंसित हुआ।।१६८।। (अब अमूढदृष्टि अङ्गको बतलाते हैं-) जिसके अन्दर बुराइयाँ भरी हैं किन्तु जो बाहरसे सुन्दर है, किम्पाकफलके समान ऐसे मिथ्यादृष्टियोंके मतपर श्रद्धा मत करो। १६९।।वैदिक मतमें मधुके प्रयोगका विधान हैं, (बौद्धमतमें) मांस-भक्षणका विधान हैं, और शैवमतमें मद्यपानका विधान है । आम्नायोंमें जो यज्ञ-और
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org