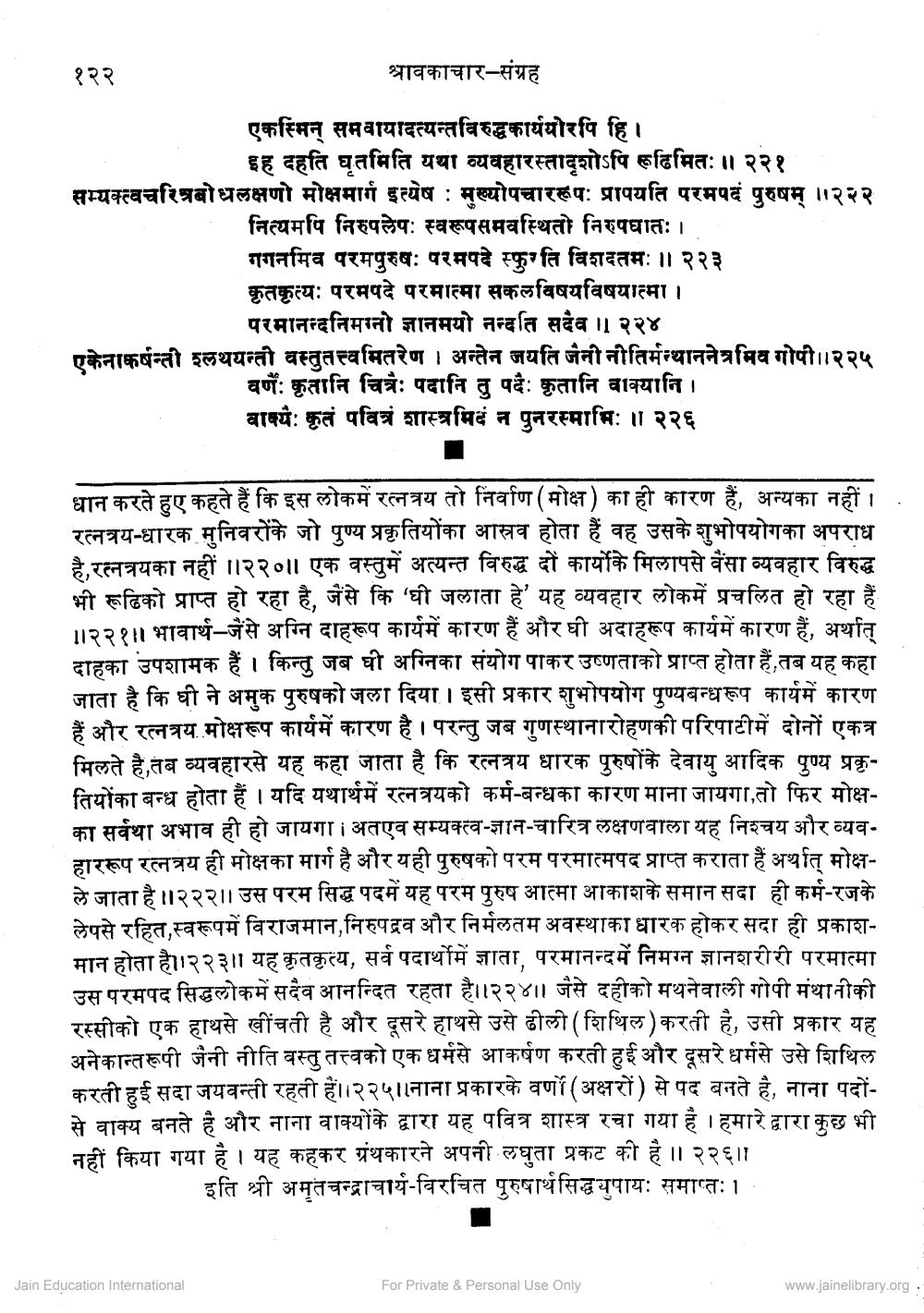________________
१२२
श्रावकाचार-संग्रह
एकस्मिन् समवायादत्यन्तविरुद्धकार्ययोरपि हि।
इह दहति घृतमिति यथा व्यवहारस्तादृशोऽपि रूढिमितः ।। २२१ सम्यक्त्वचरित्रबोधलक्षणो मोक्षमार्ग इत्येष : मुख्योपचाररूपः प्रापयति परमपदं पुरुषम् ।।२२२
नित्यमपि निरुपलेप: स्वरूपसमवस्थितो निरपघातः।। गगनमिव परमपुरुषः परमपदे स्फुरति विशदतमः ।। २२३ कृतकृत्यः परमपदे परमात्मा सकलविषयविषयात्मा ।
परमानन्दनिमग्नो ज्ञानमयो नन्दति सदैव ।। २२४ एकनाकर्षन्ती श्लथयन्ती वस्तुतत्त्वमितरेण । अन्तेन जयति जैनी नीतिर्मन्थाननेत्रमिव गोपी।।२२५
वणः कृतानि चित्रैः पदानि तु पदैः कृतानि वाक्यानि । वाक्यैः कृतं पवित्र शास्त्रमिदं न पुनरस्माभिः ।। २२६
धान करते हुए कहते हैं कि इस लोकमें रत्नत्रय तो निर्वाण (मोक्ष) का ही कारण हैं, अन्यका नहीं। रत्नत्रय-धारक मुनिवरोंके जो पुण्य प्रकृतियोंका आस्रव होता हैं वह उसके शुभोपयोगका अपराध है,रत्नत्रयका नहीं ।।२२०।। एक वस्तुमें अत्यन्त विरुद्ध दो कार्योके मिलापसे वैसा व्यवहार विरुद्ध भी रूढिको प्राप्त हो रहा है, जैसे कि 'घी जलाता है' यह व्यवहार लोकमें प्रचलित हो रहा हैं ॥२२१॥ भावार्थ-जैसे अग्नि दाहरूप कार्यमें कारण हैं और घी अदाहरूप कार्य में कारण हैं, अर्थात् दाहका उपशामक हैं। किन्तु जब घी अग्निका संयोग पाकर उष्णताको प्राप्त होता हैं,तब यह कहा जाता है कि धी ने अमुक पुरुषको जला दिया। इसी प्रकार शुभोपयोग पुण्यबन्धरूप कार्यमें कारण हैं और रत्नत्रय मोक्षरूप कार्यमें कारण है । परन्तु जब गुणस्थानारोहणकी परिपाटीमें दोनों एकत्र मिलते है,तब व्यवहारसे यह कहा जाता है कि रत्नत्रय धारक पुरुषोंके देवायु आदिक पुण्य प्रकृतियोंका बन्ध होता हैं । यदि यथार्थमें रत्नत्रयको कर्म-बन्धका कारण माना जायगा,तो फिर मोक्षका सर्वथा अभाव ही हो जायगा। अतएव सम्यक्त्व-ज्ञान-चारित्र लक्षणवाला यह निश्चय और व्यवहाररूप रत्नत्रय ही मोक्षका मार्ग है और यही पुरुषको परम परमात्मपद प्राप्त कराता है अर्थात् मोक्षले जाता है।।२२२।। उस परम सिद्ध पदमें यह परम पुरुष आत्मा आकाशके समान सदा ही कर्म-रजके लेपसे रहित,स्वरूप में विराजमान,निरुपद्रव और निर्मलतम अवस्थाका धारक होकर सदा ही प्रकाशमान होता है।।२२३।। यह कृतकृत्य, सर्व पदार्थोमें ज्ञाता, परमानन्दमें निमग्न ज्ञानशरीरी परमात्मा उस परमपद सिद्धलोकमें सदैव आनन्दित रहता है।।२२४।। जैसे दहीको मथनेवाली गोपी मथानीकी रस्सीको एक हाथसे खींचती है और दूसरे हाथसे उसे ढीली (शिथिल) करती है, उसी प्रकार यह अनेकान्तरूपी जैनी नीति वस्तु तत्त्वको एक धर्मसे आकर्षण करती हुई और दूसरे धर्मसे उसे शिथिल करती हुई सदा जयवन्ती रहती हैं।।२२५॥नाना प्रकारके वर्णो (अक्षरों) से पद बनते है, नाना पदोंसे वाक्य बनते है और नाना वाक्योंके द्वारा यह पवित्र शास्त्र रचा गया है । हमारे द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। यह कहकर ग्रंथकारने अपनी लघुता प्रकट की है ।। २२६।।
इति श्री अमृतचन्द्राचार्य-विरचित पुरुषार्थसिद्धयुपायः समाप्तः । ..
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org: