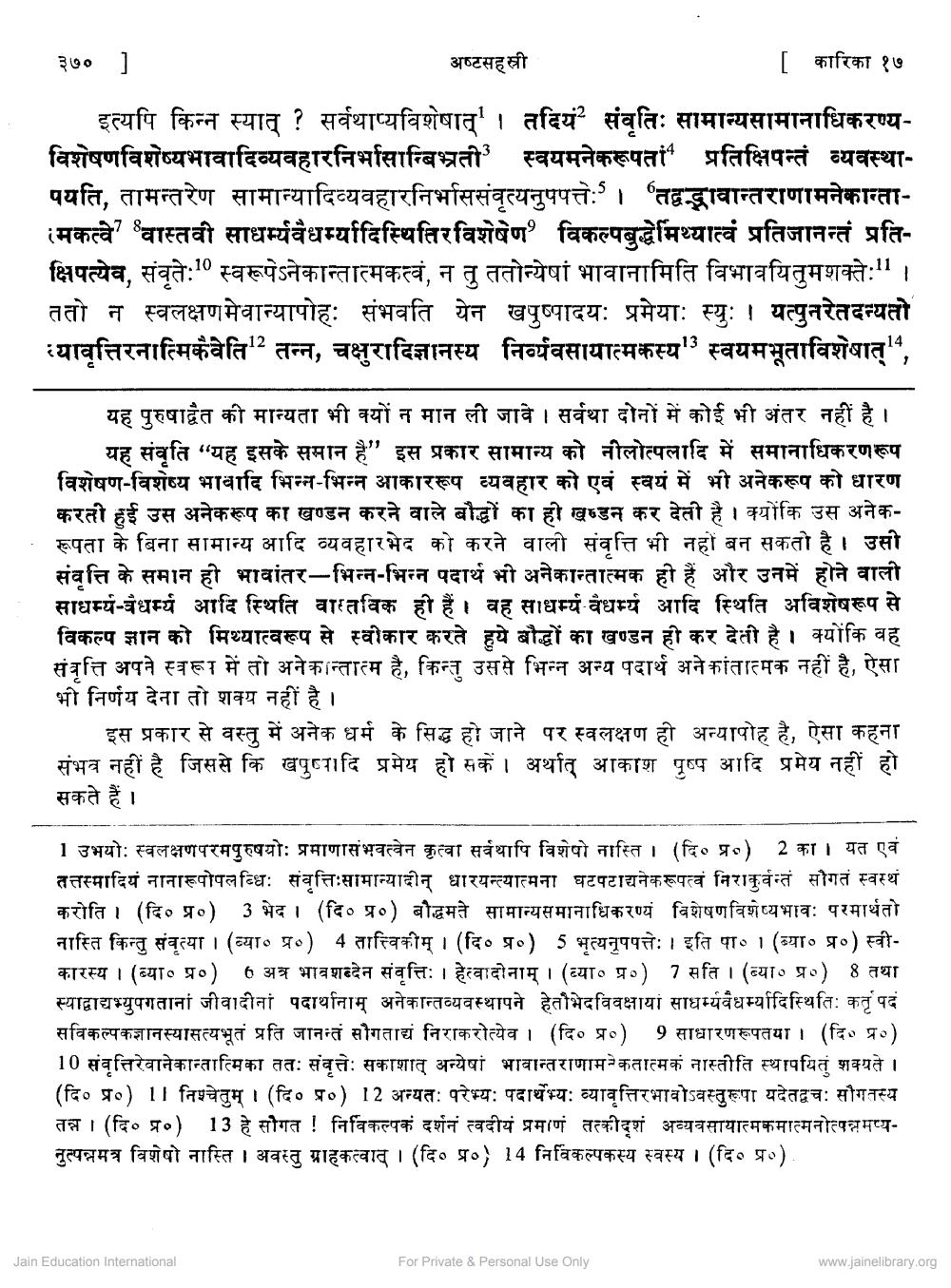________________
३७० ]
अष्टसहस्री
[ कारिका १७
___ इत्यपि किन्न स्यात् ? सर्वथाप्यविशेषात् । तदियं संवृतिः सामान्यसामानाधिकरण्यविशेषणविशेष्यभावादिव्यवहारनिर्भासाबिभ्रती' स्वयमनेकरूपता प्रतिक्षिपन्तं व्यवस्थापयति, तामन्तरेण सामान्यादिव्यवहारनिर्भाससंवृत्यनुपपत्तेः । तद्वद्भावान्तराणामनेकान्ता(मकत्वे वास्तवी साधर्म्यवैधादिस्थितिरविशेषेण' विकल्पबुद्धमिथ्यात्वं प्रतिजानन्तं प्रतिक्षिपत्येव, संवृते:10 स्वरूपेऽनेकान्तात्मकत्वं, न तु ततोन्येषां भावानामिति विभावयितुमशक्तेः । ततो न स्वलक्षणमेवान्यापोहः संभवति येन खपुष्पादयः प्रमेयाः स्युः । यत्पुनरेतदन्यतो प्यावृत्तिरनात्मिकैवेति तन्न, चक्षुरादिज्ञानस्य निर्व्यवसायात्मकस्य स्वयमभूताविशेषात्,
यह पुरुषाद्वैत की मान्यता भी क्यों न मान ली जावे । सर्वथा दोनों में कोई भी अंतर नहीं है।
यह संवृति “यह इसके समान है" इस प्रकार सामान्य को नीलोत्पलादि में समानाधिकरणरूप विशेषण-विशेष्य भावादि भिन्न-भिन्न आकाररूप व्यवहार को एवं स्वयं में भी अनेकरूप को धारण करती हुई उस अनेकरूप का खण्डन करने वाले बौद्धों का ही खण्डन कर देती है। क्योंकि उस अनेकरूपता के बिना सामान्य आदि व्यवहार भेद को करने वाली संवृत्ति भी नहीं बन सकतो है। उसी संवृत्ति के समान ही भावांतर-भिन्न-भिन्न पदार्थ भी अनेकान्तात्मक ही हैं और उनमें होने वाली साधर्म्य-वैधर्म्य आदि स्थिति वास्तविक ही हैं। वह साधर्म्य वैधर्म्य आदि स्थिति अविशेषरूप से विकल्प ज्ञान को मिथ्यात्वरूप से स्वीकार करते हुये बौद्धों का खण्डन ही कर देती है। क्योंकि वह संवृत्ति अपने स्वरूप में तो अनेकान्तात्म है, किन्तु उससे भिन्न अन्य पदार्थ अनेकांतात्मक नहीं है, ऐसा भी निर्णय देना तो शक्य नहीं है।
इस प्रकार से वस्तु में अनेक धर्म के सिद्ध हो जाने पर स्वलक्षण ही अन्यापोह है, ऐसा कहना संभव नहीं है जिससे कि खपुष्यादि प्रमेय हो सकें। अर्थात् आकाश पुष्प आदि प्रमेय नहीं हो सकते हैं।
1 उभयोः स्वलक्षणपरमपुरुषयोः प्रमाणासंभवत्वेन कृत्वा सर्वथापि विशेषो नास्ति । (दि० प्र०) 2 का । यत एवं तत्तस्मादियं नानारूपोपलब्धिः संवृत्तिःसामान्यादीन् धारयन्त्यात्मना घटपटाद्यनेकरूपत्वं निराकुर्वन्तं सौगतं स्वस्थं करोति । (दि० प्र०) 3 भेद । (दि० प्र०) बौद्धमते सामान्यसमानाधिकरण्यं विशेषणविशेष्यभावः परमार्थतो नास्ति किन्तु संवृत्या । (ब्या० प्र०) 4 तात्त्विकीम् । (दि० प्र०) 5 भृत्यनुपपत्तेः । इति पा० । (ब्या० प्र०) स्वीकारस्य । (ब्या० प्र०) 6 अत्र भावशब्देन संवृत्तिः । हेत्वादोनाम् । (व्या० प्र०) 7 सति । (ब्या० प्र०) 8 तथा स्याद्वाद्यभ्युपगतानां जीवादीनां पदार्थानाम् अनेकान्तव्यवस्थापने हेतीभेदविवक्षायां साधर्म्यवैधादिस्थिति: कत पदं सविकल्पकज्ञानस्यासत्यभूतं प्रति जानन्तं सौगताद्यं निराकरोत्येव । (दि० प्र०) 9 साधारणरूपतया। (दि० प्र०) 10 संवृत्तिरेवानेकान्तात्मिका ततः संवृत्तेः सकाशात् अन्येषां भावान्तराणामने कतात्मकं नास्तीति स्थापयितुं शक्यते । (दि० प्र०) || निश्चेतुम् । (दि० प्र०) 12 अन्यत: परेभ्यः पदार्थेभ्यः व्यावृत्तिरभावोऽवस्तुरूपा यदेत तन्न । (दि० प्र०) 13 हे सौगत ! निर्विकल्पकं दर्शनं त्वदीयं प्रमाणं तत्कीदृशं अव्यवसायात्मकमात्मनोत्पन्नमप्यनुत्पन्नमत्र विशेषो नास्ति । अवस्तु ग्राहकत्वात् । (दि० प्र०) 14 निर्विकल्पकस्य स्वस्य । (दि० प्र०).
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org