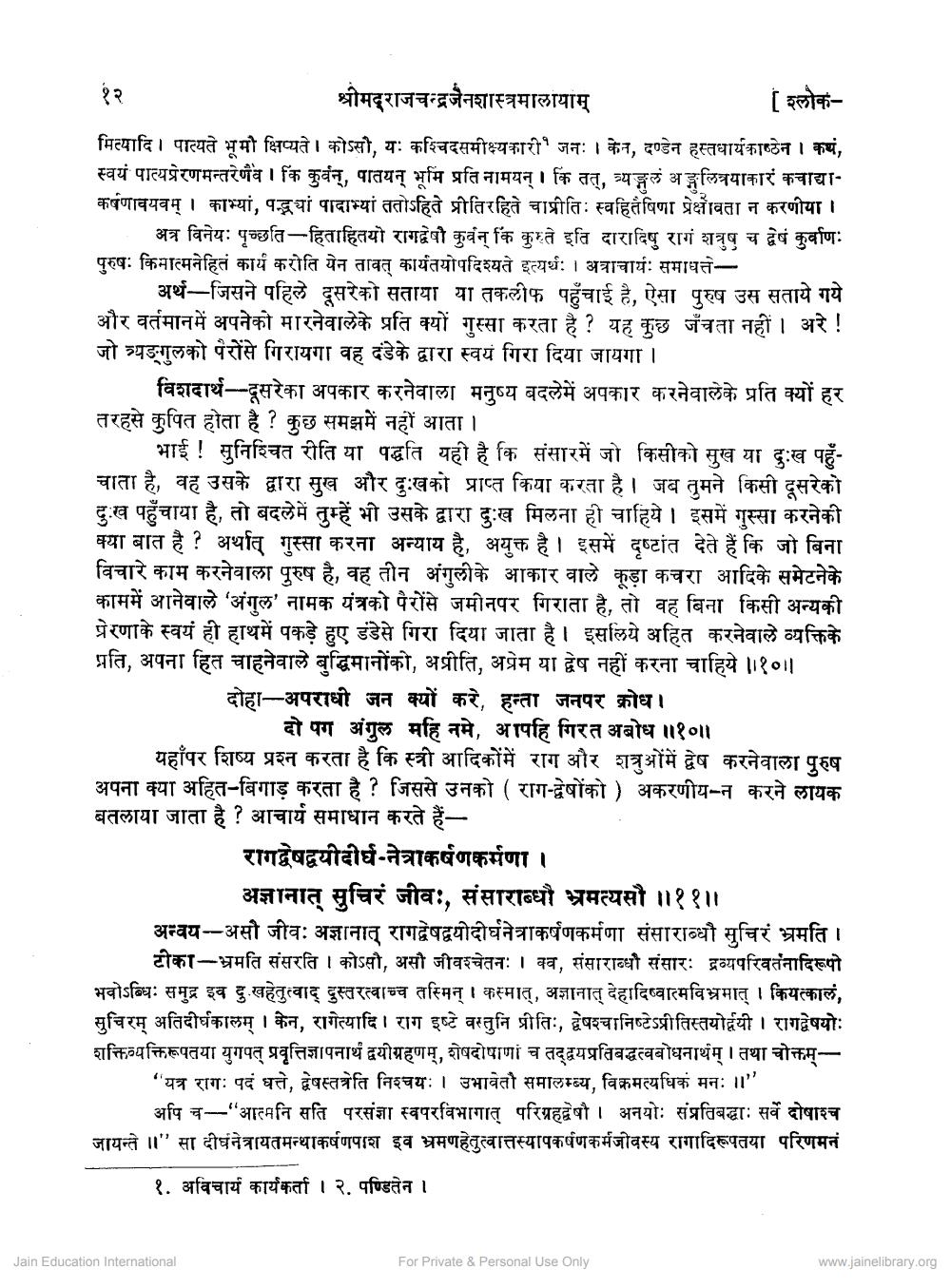________________
१२ श्रीमद्राजचन्द्रजैनशास्त्रमालायाम्
[ श्लोकमित्यादि। पात्यते भूमौ क्षिप्यते । कोऽसौ, यः कश्चिदसमीक्ष्यकारी' जनः । केन, दण्डेन हस्तधार्यकाष्ठेन । कथं, स्वयं पात्यप्रेरणमन्तरेणैव । किं कुर्वन्, पातयन् भूमि प्रति नामयन् । कि तत्, व्यङ्गलं अङ्गलित्रयाकारं कचाद्याकर्षणावयवम् । काभ्यां, पद्भयां पादाभ्यां ततोऽहिते प्रीतिरहिते चाप्रीतिः स्वहितैषिणा प्रेक्षावता न करणीया ।
अत्र विनेयः पृच्छति-हिताहितयो रागद्वेषौ कुर्वन् किं कुरुते इति दारादिषु रागं शत्रुषु च द्वेषं कुर्वाणः पुरुषः किमात्मनेहितं कार्य करोति येन तावत् कार्यतयोपदिश्यते इत्यर्थः । अत्राचार्यः समाधत्ते
अर्थ-जिसने पहिले दूसरेको सताया या तकलीफ पहुँचाई है, ऐसा पुरुष उस सताये गये और वर्तमान में अपनेको मारनेवालेके प्रति क्यों गुस्सा करता है ? यह कुछ जचता नहीं। अरे ! जो व्यङ्गुलको पैरोंसे गिरायगा वह दंडेके द्वारा स्वयं गिरा दिया जायगा।
विशदार्थ-दूसरेका अपकार करनेवाला मनुष्य बदलेमें अपकार करनेवालेके प्रति क्यों हर तरहसे कुपित होता है ? कुछ समझमें नहीं आता।
__भाई ! सुनिश्चित रीति या पद्धति यही है कि संसारमें जो किसीको सुख या दुःख पहुँचाता है, वह उसके द्वारा सुख और दुःखको प्राप्त किया करता है। जब तुमने किसी दूसरेको दुःख पहुँचाया है, तो बदले में तुम्हें भी उसके द्वारा दुःख मिलना ही चाहिये । इसमें गुस्सा करनेकी क्या बात है ? अर्थात् गुस्सा करना अन्याय है, अयुक्त है। इसमें दृष्टांत देते हैं कि जो बिना विचारे काम करनेवाला पुरुष है, वह तीन अंगुलीके आकार वाले कूड़ा कचरा आदिके समेटनेके काममें आनेवाले 'अंगुल' नामक यंत्रको पैरोंसे जमीनपर गिराता है, तो वह बिना किसी अन्यकी प्रेरणाके स्वयं ही हाथमें पकड़े हुए डंडेसे गिरा दिया जाता है। इसलिये अहित करनेवाले व्यक्तिके प्रति, अपना हित चाहनेवाले बुद्धिमानोंको, अप्रीति, अप्रेम या द्वेष नहीं करना चाहिये ॥१०॥
दोहा-अपराधी जन क्यों करे, हन्ता जनपर क्रोध।
दो पग अंगुल महि नमे, आपहि गिरत अबोध ॥१०॥ यहाँपर शिष्य प्रश्न करता है कि स्त्री आदिकोंमें राग और शत्रुओंमें द्वेष करनेवाला पुरुष अपना क्या अहित-बिगाड़ करता है ? जिससे उनको ( राग-द्वेषोंको) अकरणीय-न करने लायक बतलाया जाता है ? आचार्य समाधान करते हैं
रागद्वेषद्वयीदीर्घ-नेत्राकर्षणकर्मणा ।
अज्ञानात् सुचिरं जीवः, संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ ॥११॥ अन्वय-असौ जीवः अज्ञानात् रागद्वेषद्वयोदीर्घनेत्राकर्षणकर्मणा संसाराब्धौ सुचिरं भ्रमति ।
टीका-भ्रमति संसरति । कोऽसौ, असौ जीवश्चेतनः । क्व, संसाराब्धौ संसारः द्रव्यपरिवर्तनादिरूपो भवोऽब्धिः समुद्र इव दु.खहेतुत्वाद् दुस्तरत्वाच्च तस्मिन् । कस्मात्, अज्ञानात् देहादिष्वात्मविभ्रमात् । कियत्कालं, सुचिरम् अतिदीर्घकालम् । केन, रागेत्यादि । राग इष्टे वस्तुनि प्रीतिः, द्वेषश्चानिष्टेऽप्रीतिस्तयोर्द्वयी । रागद्वेषयोः शक्तिव्यक्तिरूपतया युगपत् प्रवृत्तिज्ञापनार्थं द्वयीग्रहणम्, शेषदोषाणां च तवयप्रतिबद्धत्वबोधनार्थम् । तथा चोक्तम्
“यत्र रागः पदं धत्ते, द्वेषस्तत्रेति निश्चयः । उभावेतौ समालम्ब्य, विक्रमत्यधिक मनः ॥"
अपि च-"आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात् परिग्रहद्वेषौ । अनयोः संप्रतिबद्धाः सर्वे दोषाश्च जायन्ते ॥" सा दीर्घनेत्रायतमन्थाकर्षणपाश इव भ्रमणहेतुत्वात्तस्यापकर्षणकर्मजीवस्य रागादिरूपतया परिणमनं
१. अविचार्य कार्यकर्ता । २. पण्डितेन ।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org