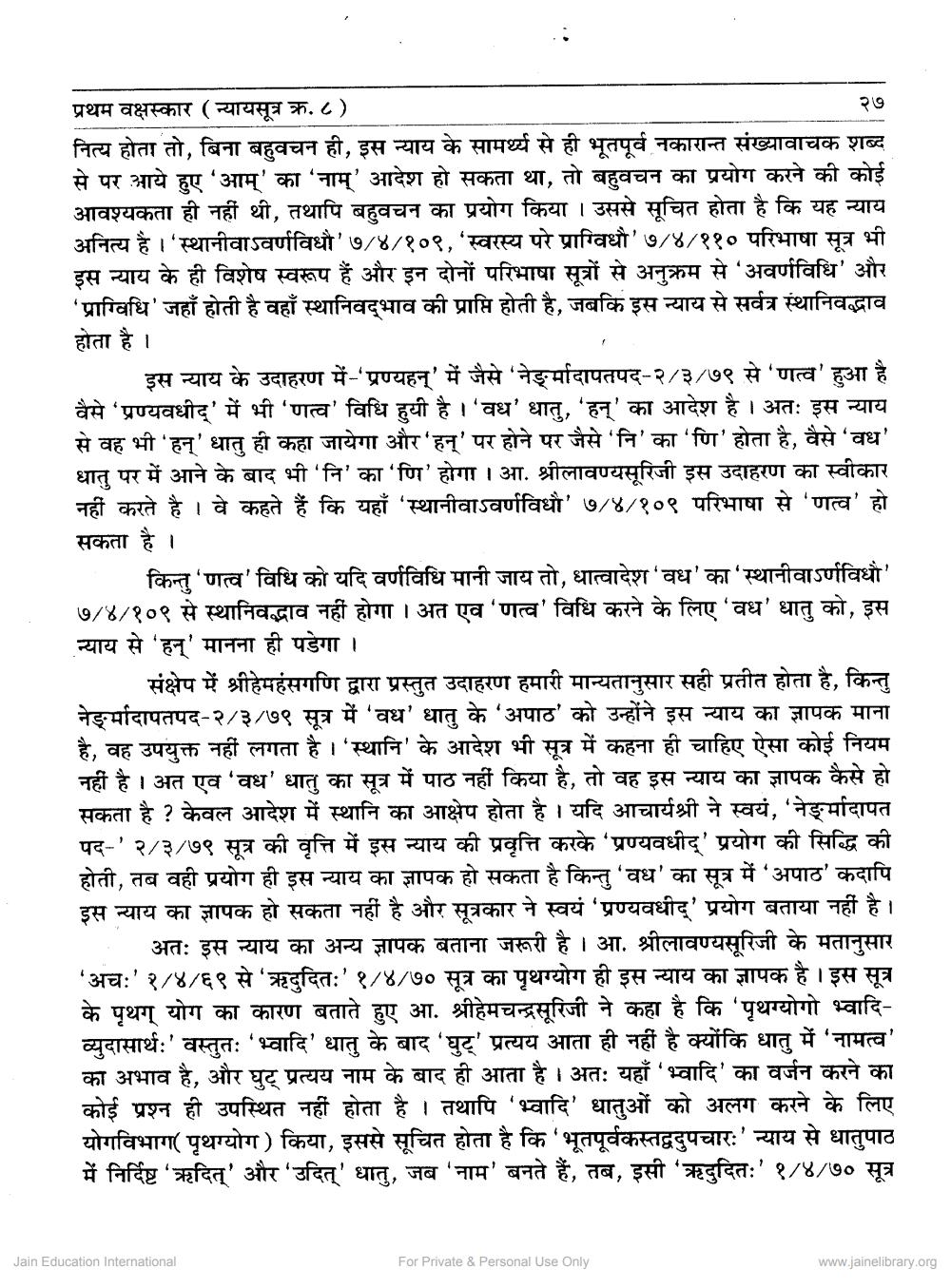________________
२७
प्रथम वक्षस्कार (न्यायसूत्र क्र.८) नित्य होता तो, बिना बहुवचन ही, इस न्याय के सामर्थ्य से ही भूतपूर्व नकारान्त संख्यावाचक शब्द से पर आये हुए 'आम्' का 'नाम्' आदेश हो सकता था, तो बहुवचन का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, तथापि बहुवचन का प्रयोग किया । उससे सूचित होता है कि यह न्याय अनित्य है । 'स्थानीवाऽवर्णविधौ' ७/४/१०९, 'स्वरस्य परे प्राग्विधौ' ७/४/११० परिभाषा सूत्र भी इस न्याय के ही विशेष स्वरूप हैं और इन दोनों परिभाषा सूत्रों से अनुक्रम से 'अवर्णविधि' और 'प्राग्विधि' जहाँ होती है वहाँ स्थानिवद्भाव की प्राप्ति होती है, जबकि इस न्याय से सर्वत्र स्थानिवद्भाव होता है।
इस न्याय के उदाहरण में-'प्रण्यहन्' में जैसे 'नेङ्र्मादापतपद-२/३/७९ से 'णत्व' हुआ है वैसे 'प्रण्यवधीद्' में भी ‘णत्व' विधि हुयी है । 'वध' धातु, 'हन्' का आदेश है । अतः इस न्याय से वह भी 'हन्' धातु ही कहा जायेगा और 'हन्' पर होने पर जैसे 'नि' का 'णि' होता है, वैसे 'वध' धातु पर में आने के बाद भी 'नि' का 'णि' होगा । आ. श्रीलावण्यसूरिजी इस उदाहरण का स्वीकार नहीं करते है । वे कहते हैं कि यहाँ 'स्थानीवाऽवर्णविधौ' ७/४/१०९ परिभाषा से 'णत्व' हो सकता है।
किन्तु ‘णत्व' विधि को यदि वर्णविधि मानी जाय तो, धात्वादेश 'वध' का 'स्थानीवाऽर्णविधौ' ७/४/१०९ से स्थानिवद्भाव नहीं होगा । अत एव ‘णत्व' विधि करने के लिए ‘वध' धातु को, इस न्याय से 'हन्' मानना ही पडेगा ।
संक्षेप में श्रीहेमहंसगणि द्वारा प्रस्तुत उदाहरण हमारी मान्यतानुसार सही प्रतीत होता है, किन्तु नेर्मादापतपद-२/३/७९ सूत्र में 'वध' धातु के 'अपाठ' को उन्होंने इस न्याय का ज्ञापक माना है, वह उपयुक्त नहीं लगता है । 'स्थानि' के आदेश भी सूत्र में कहना ही चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। अत एव 'वध' धात का सत्र में पाठ नहीं किया है, तो वह इस न्याय का ज्ञापक कैसे हो सकता है ? केवल आदेश में स्थानि का आक्षेप होता है। यदि आचार्यश्री ने स्वयं, 'नेमादापत
द-' २/३/७९ सत्र की वत्ति में इस न्याय की प्रवत्ति करके 'प्रण्यवधीद' प्रयोग की सिद्धि की होती, तब वही प्रयोग ही इस न्याय का ज्ञापक हो सकता है किन्तु 'वध' का सूत्र में 'अपाठ' कदापि इस न्याय का ज्ञापक हो सकता नहीं है और सूत्रकार ने स्वयं 'प्रण्यवधीद्' प्रयोग बताया नहीं है।
अतः इस न्याय का अन्य ज्ञापक बताना जरूरी है । आ. श्रीलावण्यसूरिजी के मतानुसार 'अचः' १/४/६९ से 'ऋदुदितः' १/४/७० सूत्र का पृथग्योग ही इस न्याय का ज्ञापक है । इस सूत्र के पृथग् योग का कारण बताते हुए आ. श्रीहेमचन्द्रसूरिजी ने कहा है कि 'पृथग्योगो भ्वादिव्युदासार्थः' वस्तुतः 'भ्वादि' धातु के बाद 'घुट्' प्रत्यय आता ही नहीं है क्योंकि धातु में 'नामत्व' का अभाव है, और घुट् प्रत्यय नाम के बाद ही आता है। अतः यहाँ 'भ्वादि' का वर्जन करने का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है । तथापि 'भ्वादि' धातुओं को अलग करने के लिए योगविभाग( पृथग्योग) किया, इससे सूचित होता है कि 'भूतपूर्वकस्तद्वदुपचारः' न्याय से धातुपाठ में निर्दिष्ट 'ऋदित्' और 'उदित्' धातु, जब 'नाम' बनते हैं, तब, इसी 'ऋदुदितः' १/४/७० सूत्र
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org