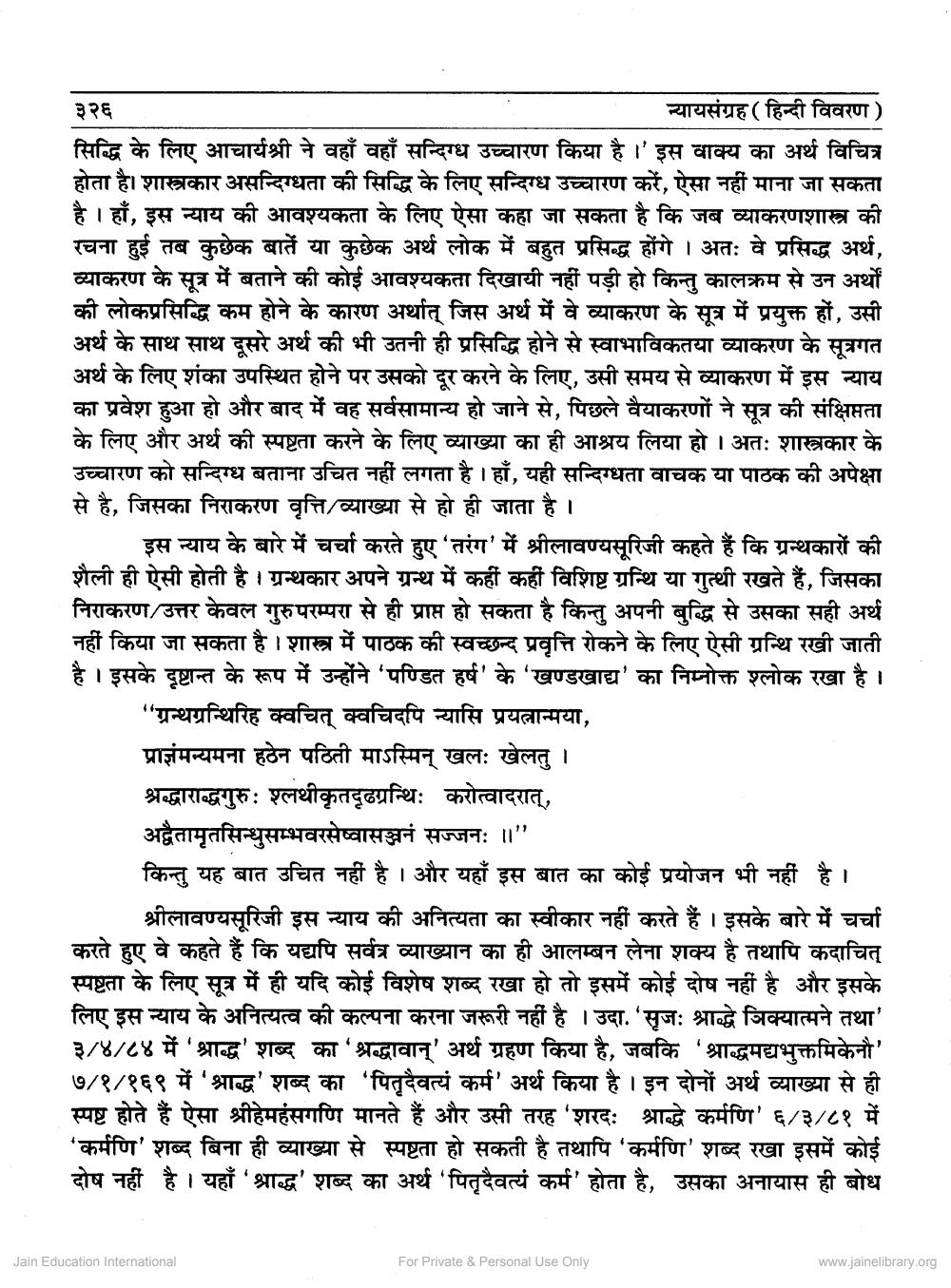________________
३२६
न्यायसंग्रह (हिन्दी विवरण )
सिद्धि के लिए आचार्यश्री ने वहाँ वहाँ सन्दिग्ध उच्चारण किया है।' इस वाक्य का अर्थ विचित्र होता है। शास्त्रकार असन्दिग्धता की सिद्धि के लिए सन्दिग्ध उच्चारण करें, ऐसा नहीं माना जा सकता है । हाँ, इस न्याय की आवश्यकता के लिए ऐसा कहा जा सकता है कि जब व्याकरणशास्त्र की रचना हुई तब कुछेक बातें या कुछेक अर्थ लोक में बहुत प्रसिद्ध होंगे। अतः वे प्रसिद्ध अर्थ, व्याकरण के सूत्र में बताने की कोई आवश्यकता दिखायी नहीं पड़ी हो किन्तु कालक्रम से उन अर्थों की लोकप्रसिद्धि कम होने के कारण अर्थात् जिस अर्थ में वे व्याकरण के सूत्र में प्रयुक्त हों, उसी अर्थ के साथ साथ दूसरे अर्थ की भी उतनी ही प्रसिद्धि होने से स्वाभाविकतया व्याकरण के सूत्रगत अर्थ के लिए शंका उपस्थित होने पर उसको दूर करने के लिए, उसी समय से व्याकरण में इस न्याय IT प्रवेश हुआ हो और बाद में वह सर्वसामान्य हो जाने से, पिछले वैयाकरणों ने सूत्र की संक्षिप्तता के लिए और अर्थ की स्पष्टता करने के लिए व्याख्या का ही आश्रय लिया हो । अतः शास्त्रकार के उच्चारण को सन्दिग्ध बताना उचित नहीं लगता है। हाँ, यही सन्दिग्धता वाचक या पाठक की अपेक्षा से है, जिसका निराकरण वृत्ति/ व्याख्या से हो ही जाता है ।
इस न्याय के बारे में चर्चा करते हुए 'तरंग' में श्रीलावण्यसूरिजी कहते हैं कि ग्रन्थकारों की शैली ही ऐसी होती है । ग्रन्थकार अपने ग्रन्थ में कहीं कहीं विशिष्ट ग्रन्थि या गुत्थी रखते हैं, जिसका निराकरण/ उत्तर केवल गुरुपरम्परा से ही प्राप्त हो सकता है किन्तु अपनी बुद्धि से उसका सही अर्थ नहीं किया जा सकता है। शास्त्र में पाठक की स्वच्छन्द प्रवृत्ति रोकने के लिए ऐसी ग्रन्थि रखी जाती है । इसके दृष्टान्त के रूप में उन्होंने 'पण्डित हर्ष' के 'खण्डखाद्य' का निम्नोक्त श्लोक रखा है ।
"ग्रन्थग्रन्थिरिह क्वचित् क्वचिदपि न्यासि प्रयत्नान्मया, प्राज्ञंमन्यमना हठेन पठिती माऽस्मिन् खलः खेलतु । श्रद्धाराद्धगुरुः श्लथीकृतदृढग्रन्थिः करोत्वादरात्, अद्वैतामृतसिन्धुसम्भवरसेष्वासञ्जनं सज्जनः ॥।”
किन्तु यह बात उचित नहीं है । और यहाँ इस बात का कोई प्रयोजन भी नहीं है ।
श्रीलावण्यसूरिजी इस न्याय की अनित्यता का स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बारे में चर्चा
करते हुए वे कहते हैं कि यद्यपि सर्वत्र व्याख्यान का ही आलम्बन लेना शक्य है तथापि कदाचित् स्पष्टता के लिए सूत्र में ही यदि कोई विशेष शब्द रखा हो तो इसमें कोई दोष नहीं है और इसके लिए इस न्याय के अनित्यत्व की कल्पना करना जरूरी नहीं है । उदा. 'सृजः श्राद्धे ञिक्यात्मने तथा ' ३/४/८४ में ‘श्राद्ध' शब्द का 'श्रद्धावान्' अर्थ ग्रहण किया है, जबकि 'श्राद्धमद्यभुक्तमिकेनौ' ७/१/१६९ में 'श्राद्ध' शब्द का 'पितृदैवत्यं कर्म' अर्थ किया है । इन दोनों अर्थ व्याख्या से ही स्पष्ट होते हैं ऐसा श्रीहेमहंसगणि मानते हैं और उसी तरह 'शरद: श्राद्धे कर्मणि' ६/३/८१ में 'कर्मणि' शब्द बिना ही व्याख्या से स्पष्टता हो सकती है तथापि 'कर्मणि' शब्द रखा इसमें कोई दोष नहीं है । यहाँ 'श्राद्ध' शब्द का अर्थ 'पितृदैवत्यं कर्म' होता है, उसका अनायास ही बोध
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org