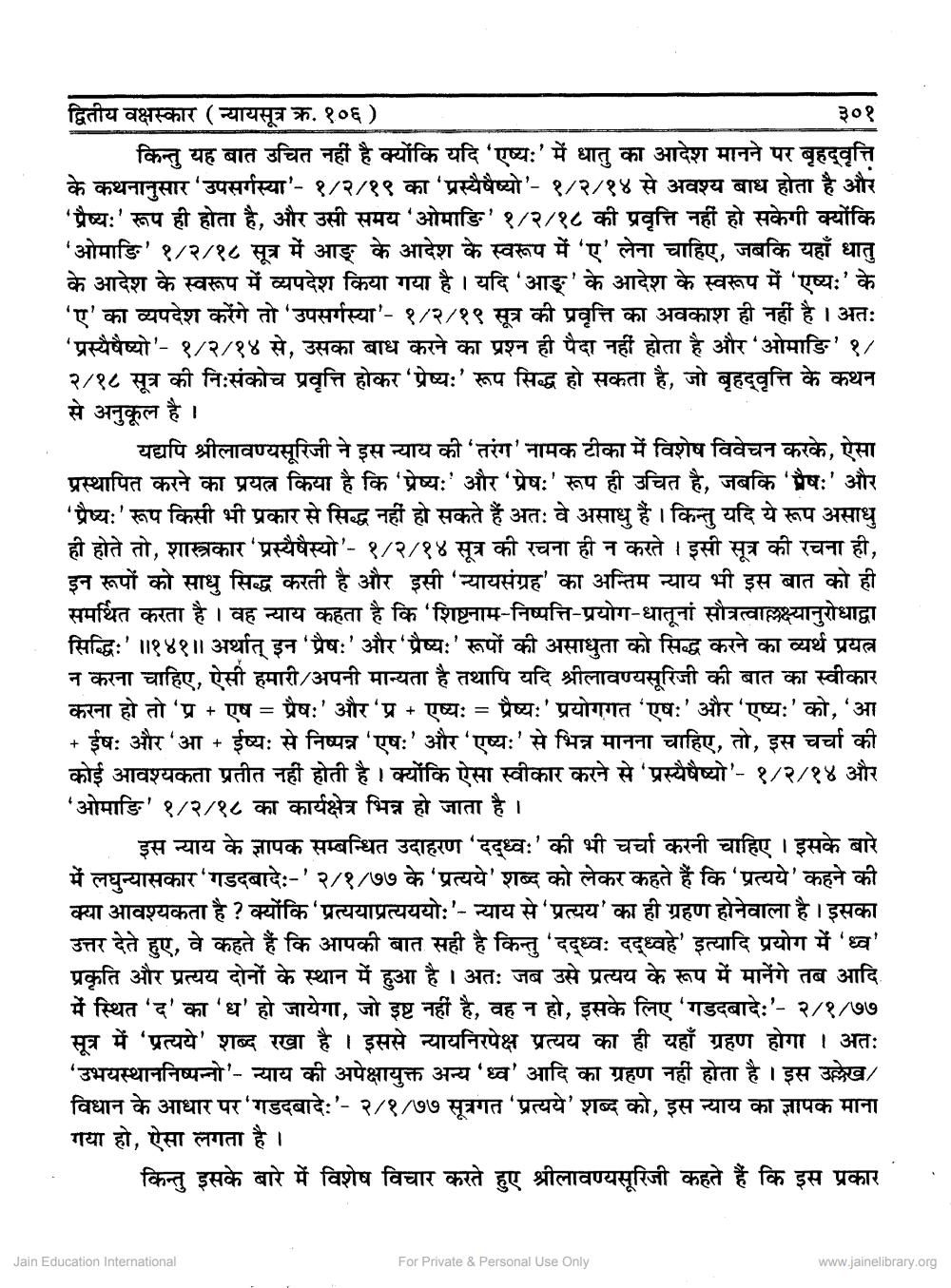________________
द्वितीय वक्षस्कार (न्यायसूत्र क्र. १०६)
३०१ किन्तु यह बात उचित नहीं है क्योंकि यदि 'एष्यः' में धातु का आदेश मानने पर बृहद्वृत्ति के कथनानुसार 'उपसर्गस्या'- १/२/१९ का 'प्रस्यैषैष्यो'- १/२/१४ से अवश्य बाध होता है और 'प्रैष्यः' रूप ही होता है, और उसी समय 'ओमाङि' १/२/१८ की प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी क्योंकि 'ओमाङि' १/२/१८ सूत्र में आङ् के आदेश के स्वरूप में 'ए' लेना चाहिए, जबकि यहाँ धातु के आदेश के स्वरूप में व्यपदेश किया गया है। यदि आङ्' के आदेश के स्वरूप में 'एष्यः' के 'ए' का व्यपदेश करेंगे तो 'उपसर्गस्या'- १/२/१९ सूत्र की प्रवृत्ति का अवकाश ही नहीं है । अतः 'प्रस्यैषैष्यो'- १/२/१४ से, उसका बाध करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है और ओमाङि' १/ २/१८ सूत्र की निःसंकोच प्रवृत्ति होकर 'प्रेष्यः' रूप सिद्ध हो सकता है, जो बृहद्वृत्ति के कथन से अनुकूल है।
यद्यपि श्रीलावण्यसूरिजी ने इस न्याय की 'तरंग' नामक टीका में विशेष विवेचन करके, ऐसा प्रस्थापित करने का प्रयत्न किया है कि 'प्रेष्यः' और 'प्रेषः' रूप ही उचित है, जबकि 'प्रैषः' और 'प्रैष्यः' रूप किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकते हैं अतः वे असाधु हैं । किन्तु यदि ये रूप असाधु ही होते तो, शास्त्रकार 'प्रस्यैषैस्यो'- १/२/१४ सूत्र की रचना ही न करते । इसी सूत्र की रचना ही, इन रूपों को साधु सिद्ध करती है और इसी 'न्यायसंग्रह' का अन्तिम न्याय भी इस बात को ही समर्थित करता है । वह न्याय कहता है कि 'शिष्टनाम-निष्पत्ति-प्रयोग-धातूनां सौत्रत्वाल्लक्ष्यानुरोधाद्वा सिद्धिः' ॥१४१॥ अर्थात् इन 'प्रैषः' और 'प्रैष्यः' रूपों की असाधुता को सिद्ध करने का व्यर्थ प्रयत्न न करना चाहिए, ऐसी हमारी/अपनी मान्यता है तथापि यदि श्रीलावण्यसूरिजी की बात का स्वीकार करना हो तो 'प्र + एष = प्रैषः' और 'प्र + एष्यः = प्रैष्यः' प्रयोगगत 'एषः' और 'एष्यः' को, 'आ + ईषः और 'आ + ईष्यः से निष्पन्न 'एषः' और 'एष्यः' से भिन्न मानना चाहिए, तो, इस चर्चा की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। क्योंकि ऐसा स्वीकार करने से 'प्रस्यैषैष्यो'- १/२/१४ और 'ओमाङि' १/२/१८ का कार्यक्षेत्र भिन्न हो जाता है।
इस न्याय के ज्ञापक सम्बन्धित उदाहरण 'दद्ध्वः' की भी चर्चा करनी चाहिए । इसके बारे में लघुन्यासकार 'गडदबादेः-' २/१/७७ के 'प्रत्यये' शब्द को लेकर कहते हैं कि प्रत्यये' कहने की क्या आवश्यकता है ? क्योंकि प्रत्ययाप्रत्यययो:'- न्याय से प्रत्यय' का ही ग्रहण होनेवाला है। इसका उत्तर देते हुए, वे कहते हैं कि आपकी बात सही है किन्तु 'दद्ध्वः दद्ध्वहे' इत्यादि प्रयोग में 'ध्व' प्रकृति और प्रत्यय दोनों के स्थान में हुआ है । अत: जब उसे प्रत्यय के रूप में मानेंगे तब आदि में स्थित 'द' का 'ध' हो जायेगा, जो इष्ट नहीं है, वह न हो, इसके लिए 'गडदबादेः'- २/१/७७ सूत्र में 'प्रत्यये' शब्द रखा है। इससे न्यायनिरपेक्ष प्रत्यय का ही यहाँ ग्रहण होगा । अतः 'उभयस्थाननिष्पन्नो'- न्याय की अपेक्षायुक्त अन्य 'ध्व' आदि का ग्रहण नहीं होता है । इस उल्लेख/ विधान के आधार पर 'गडदबादेः'- २/१/७७ सूत्रगत 'प्रत्यये' शब्द को, इस न्याय का ज्ञापक माना गया हो, ऐसा लगता है।
किन्तु इसके बारे में विशेष विचार करते हुए श्रीलावण्यसूरिजी कहते हैं कि इस प्रकार
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org