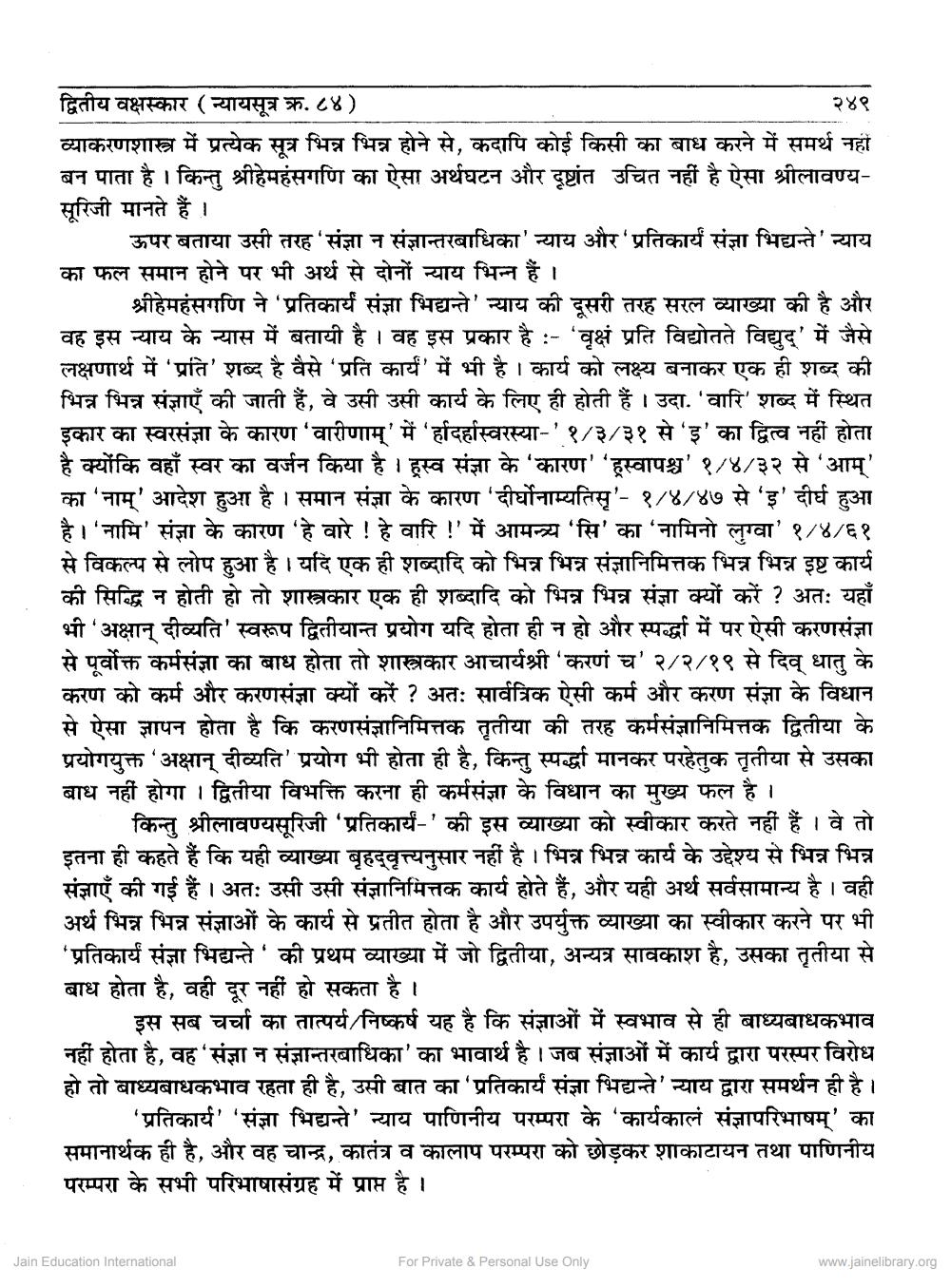________________
द्वितीय वक्षस्कार (न्यायसूत्र क्र.८४)
२४९ व्याकरणशास्त्र में प्रत्येक सूत्र भिन्न भिन्न होने से, कदापि कोई किसी का बाध करने में समर्थ नहीं बन पाता है । किन्तु श्रीहेमहंसगणि का ऐसा अर्थघटन और दृष्टांत उचित नहीं है ऐसा श्रीलावण्यसूरिजी मानते हैं।
ऊपर बताया उसी तरह 'संज्ञा न संज्ञान्तरबाधिका' न्याय और प्रतिकार्यं संज्ञा भिद्यन्ते' न्याय का फल समान होने पर भी अर्थ से दोनों न्याय भिन्न हैं।
श्रीहेमहंसगणि ने 'प्रतिकार्य संज्ञा भिद्यन्ते' न्याय की दूसरी तरह सरल व्याख्या की है और वह इस न्याय के न्यास में बतायी है । वह इस प्रकार है :- 'वृक्षं प्रति विद्योतते विद्युद्' में जैसे लक्षणार्थ में 'प्रति' शब्द है वैसे 'प्रति कार्यं' में भी है। कार्य को लक्ष्य बनाकर एक ही शब्द की भिन्न भिन्न संज्ञाएँ की जाती हैं, वे उसी उसी कार्य के लिए ही होती हैं । उदा. 'वारि' शब्द में स्थित इकार का स्वरसंज्ञा के कारण 'वारीणाम्' में 'दिर्हास्वरस्या-' १/३/३१ से 'इ' का द्वित्व नहीं होता है क्योंकि वहाँ स्वर का वर्जन किया है । इस्व संज्ञा के 'कारण' 'हुस्वापश्च' १/४/३२ से 'आम्' का 'नाम्' आदेश हुआ है । समान संज्ञा के कारण 'दीर्घोनाम्यतिसृ'- १/४/४७ से 'इ' दीर्घ हुआ है। 'नामि' संज्ञा के कारण 'हे वारे ! हे वारि !' में आमन्त्र्य 'सि' का 'नामिनो लुग्वा' १/४/६१ से विकल्प से लोप हुआ है। यदि एक ही शब्दादि को भिन्न भिन्न संज्ञानिमित्तक भिन्न भिन्न इष्ट कार्य की सिद्धि न होती हो तो शास्त्रकार एक ही शब्दादि को भिन्न भिन्न संज्ञा क्यों करें ? अतः यहाँ भी 'अक्षान् दीव्यति' स्वरूप द्वितीयान्त प्रयोग यदि होता ही न हो और स्पर्धा में पर ऐसी करणसंज्ञा से पर्वोक्त कर्मसंजा का बाध होता तो शास्त्रकार आचार्यश्री करणं च' २/२/१९ से दिव धात के करण को कर्म और करणसंज्ञा क्यों करें ? अतः सार्वत्रिक ऐसी कर्म और करण संज्ञा के विधान से ऐसा ज्ञापन होता है कि करणसंज्ञानिमित्तक तृतीया की तरह कर्मसंज्ञानिमित्तक द्वितीया के प्रयोगयुक्त अक्षान् दीव्यति' प्रयोग भी होता ही है, किन्तु स्पर्द्धा मानकर परहेतुक तृतीया से उसका बाध नहीं होगा । द्वितीया विभक्ति करना ही कर्मसंज्ञा के विधान का मुख्य फल है।
किन्तु श्रीलावण्यसूरिजी 'प्रतिकार्यं-' की इस व्याख्या को स्वीकार करते नहीं हैं । वे तो इतना ही कहते हैं कि यही व्याख्या बृहवृत्त्यनुसार नहीं है । भिन्न भिन्न कार्य के उद्देश्य से भिन्न भिन्न संज्ञाएँ की गई हैं । अतः उसी उसी संज्ञानिमित्तक कार्य होते हैं, और यही अर्थ सर्वसामान्य है । वही अर्थ भिन्न भिन्न संज्ञाओं के कार्य से प्रतीत होता है और उपर्युक्त व्याख्या का स्वीकार करने पर भी 'प्रतिकार्यं संज्ञा भिद्यन्ते ' की प्रथम व्याख्या में जो द्वितीया, अन्यत्र सावकाश है, उसका तृतीया से बाध होता है, वही दूर नहीं हो सकता है।
इस सब चर्चा का तात्पर्य/निष्कर्ष यह है कि संज्ञाओं में स्वभाव से ही बाध्यबाधकभाव नहीं होता है, वह 'संज्ञा न संज्ञान्तरबाधिका' का भावार्थ है। जब संज्ञाओं में कार्य द्वारा परस्पर विरोध हो तो बाध्यबाधकभाव रहता ही है, उसी बात का 'प्रतिकार्यं संज्ञा भिद्यन्ते' न्याय द्वारा समर्थन ही है।
'प्रतिकार्य' 'संज्ञा भिद्यन्ते' न्याय पाणिनीय परम्परा के कार्यकालं संज्ञापरिभाषम्' का समानार्थक ही है, और वह चान्द्र, कातंत्र व कालाप परम्परा को छोड़कर शाकाटायन तथा पाणिनीय परम्परा के सभी परिभाषासंग्रह में प्राप्त है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org