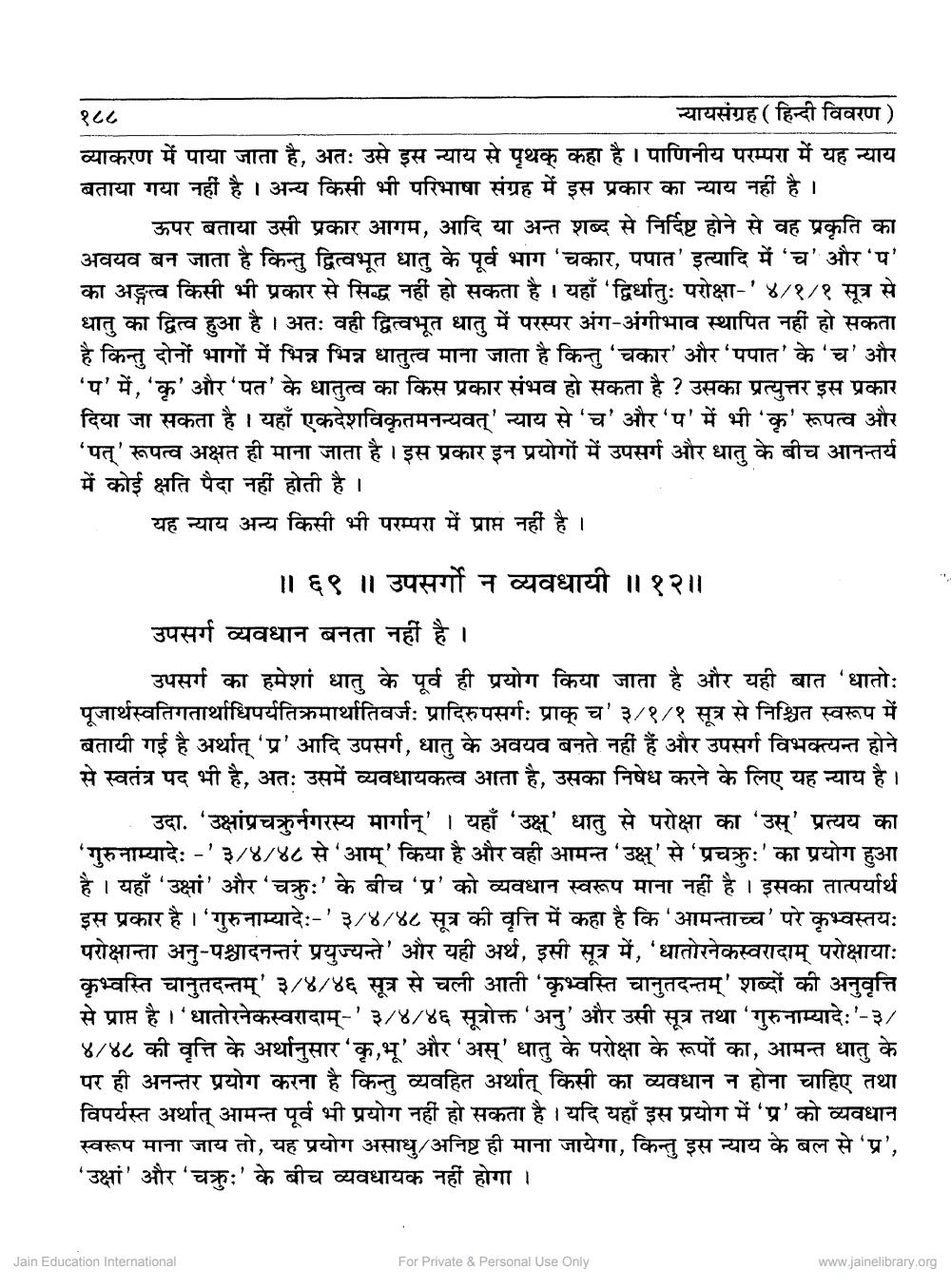________________
१८८
न्यायसंग्रह (हिन्दी विवरण) व्याकरण में पाया जाता है, अतः उसे इस न्याय से पृथक् कहा है। पाणिनीय परम्परा में यह न्याय बताया गया नहीं है । अन्य किसी भी परिभाषा संग्रह में इस प्रकार का न्याय नहीं है।
ऊपर बताया उसी प्रकार आगम, आदि या अन्त शब्द से निर्दिष्ट होने से वह प्रकृति का अवयव बन जाता है किन्तु द्वित्वभूत धातु के पूर्व भाग 'चकार, पपात' इत्यादि में 'च' और 'प' का अङ्गत्व किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता है । यहाँ 'द्विर्धातुः परोक्षा-' ४/१/१ सूत्र से धातु का द्वित्व हुआ है । अतः वही द्वित्वभूत धातु में परस्पर अंग-अंगीभाव स्थापित नहीं हो सकता है किन्तु दोनों भागों में भिन्न भिन्न धातुत्व माना जाता है किन्तु 'चकार' और 'पपात' के 'च' और 'प' में, 'कृ' और 'पत' के धातुत्व का किस प्रकार संभव हो सकता है ? उसका प्रत्युत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है । यहाँ एकदेशविकृतमनन्यवत्' न्याय से 'च' और 'प' में भी 'कृ' रूपत्व और 'पत्' रूपत्व अक्षत ही माना जाता है । इस प्रकार इन प्रयोगों में उपसर्ग और धातु के बीच आनन्तर्य में कोई क्षति पैदा नहीं होती है ।
यह न्याय अन्य किसी भी परम्परा में प्राप्त नहीं है ।
॥६९ ॥ उपसर्गो न व्यवधायी ॥१२॥ उपसर्ग व्यवधान बनता नहीं है।
उपसर्ग का हमेशां धातु के पूर्व ही प्रयोग किया जाता है और यही बात 'धातोः पूजार्थस्वतिगतार्थाधिपर्यतिक्रमार्थातिवर्जः प्रादिरुपसर्गः प्राक् च' ३/१/१ सूत्र से निश्चित स्वरूप में बतायी गई है अर्थात् 'प्र' आदि उपसर्ग, धातु के अवयव बनते नहीं हैं और उपसर्ग विभक्त्यन्त होने से स्वतंत्र पद भी है, अतः उसमें व्यवधायकत्व आता है, उसका निषेध करने के लिए यह न्याय है।
उदा. 'उक्षांप्रचक्रुर्नगरस्य मार्गान्' । यहाँ 'उर्' धातु से परीक्षा का 'उस्' प्रत्यय का 'गुरुनाम्यादेः -' ३/४/४८ से 'आम्' किया है और वही आमन्त 'उक्ष' से 'प्रचक्रुः' का प्रयोग हुआ है । यहाँ 'उक्षां' और 'चक्रुः' के बीच 'प्र' को व्यवधान स्वरूप माना नहीं है । इसका तात्पर्यार्थ इस प्रकार है । 'गुरुनाम्यादेः-' ३/४/४८ सूत्र की वृत्ति में कहा है कि 'आमन्ताच्च' परे कृभ्वस्तयः परोक्षान्ता अनु-पश्चादनन्तरं प्रयुज्यन्ते' और यही अर्थ, इसी सूत्र में, 'धातोरनेकस्वरादाम् परोक्षायाः कृभ्वस्ति चानुतदन्तम्' ३/४/४६ सूत्र से चली आती 'कृभ्वस्ति चानुतदन्तम्' शब्दों की अनुवृत्ति से प्राप्त है। धातोरनेकस्वरादाम्-' ३/४/४६ सूत्रोक्त 'अनु' और उसी सूत्र तथा 'गुरुनाम्यादेः'-३/ ४/४८ की वृत्ति के अर्थानुसार 'कृ,भू' और 'अस्' धातु के परीक्षा के रूपों का, आमन्त धातु के पर ही अनन्तर प्रयोग करना है किन्तु व्यवहित अर्थात् किसी का व्यवधान न होना चाहिए तथा विपर्यस्त अर्थात् आमन्त पूर्व भी प्रयोग नहीं हो सकता है । यदि यहाँ इस प्रयोग में 'प्र' को व्यवधान स्वरूप माना जाय तो, यह प्रयोग असाधु/अनिष्ट ही माना जायेगा, किन्तु इस न्याय के बल से 'प्र', 'उक्षां' और 'चक्रुः' के बीच व्यवधायक नहीं होगा।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org