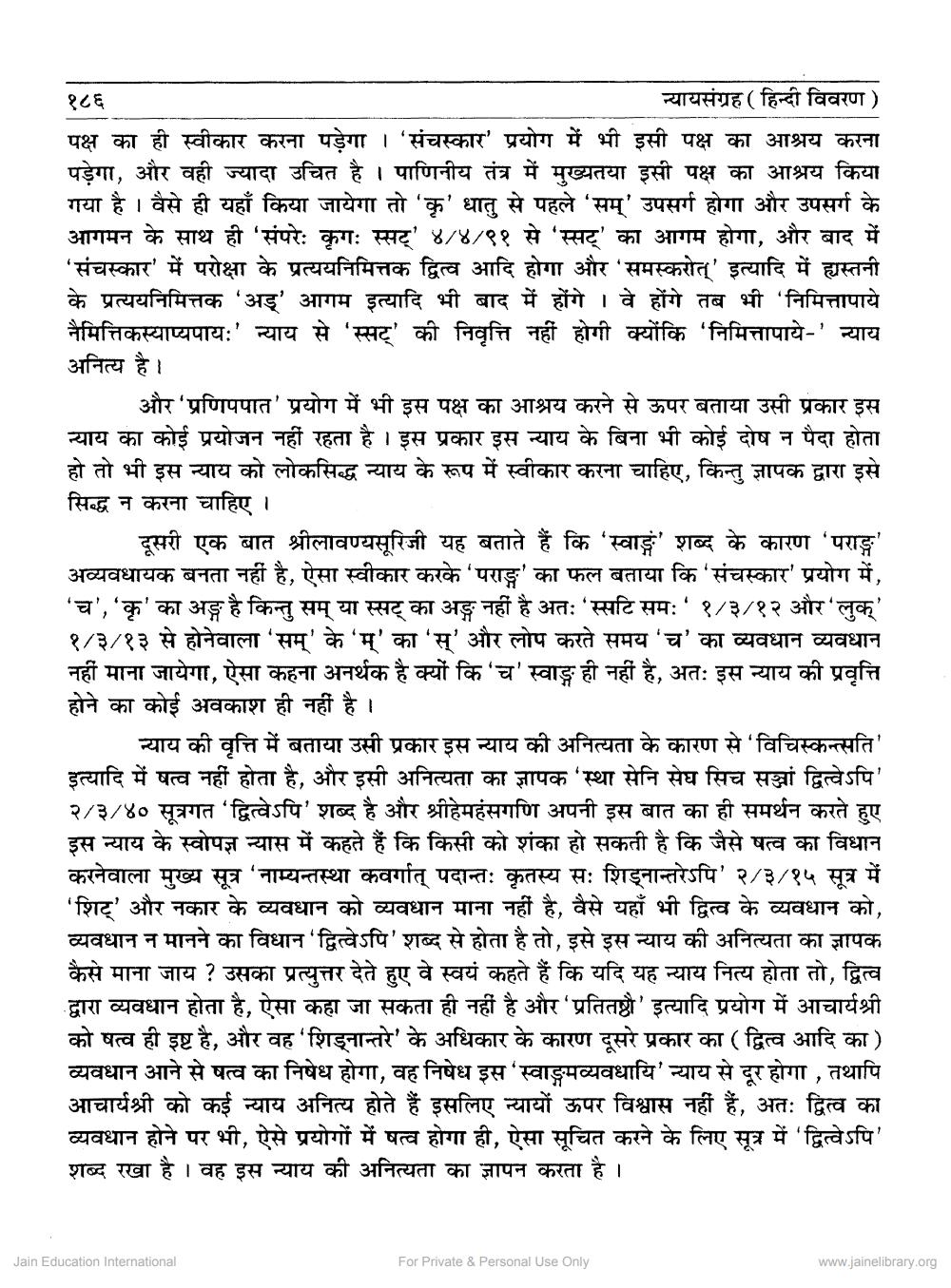________________
१८६
न्यायसंग्रह (हिन्दी विवरण) पक्ष का ही स्वीकार करना पड़ेगा । 'संचस्कार' प्रयोग में भी इसी पक्ष का आश्रय करना पड़ेगा, और वही ज्यादा उचित है । पाणिनीय तंत्र में मुख्यतया इसी पक्ष का आश्रय किया गया है । वैसे ही यहाँ किया जायेगा तो 'कृ' धातु से पहले 'सम्' उपसर्ग होगा और उपसर्ग के आगमन के साथ ही 'संपरेः कृगः स्सट्' ४/४/९१ से 'स्सट्' का आगम होगा, और बाद में 'संचस्कार' में परोक्षा के प्रत्ययनिमित्तक द्वित्व आदि होगा और 'समस्करोत्' इत्यादि में हस्तनी के प्रत्ययनिमित्तक 'अड्' आगम इत्यादि भी बाद में होंगे । वे होंगे तब भी 'निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपाय:' न्याय से 'स्सट' की निवृत्ति नहीं होगी क्योंकि 'निमित्तापाये-' न्याय अनित्य है।
और 'प्रणिपपात' प्रयोग में भी इस पक्ष का आश्रय करने से ऊपर बताया उसी प्रकार इस न्याय का कोई प्रयोजन नहीं रहता है । इस प्रकार इस न्याय के बिना भी कोई दोष न पैदा होता हो तो भी इस न्याय को लोकसिद्ध न्याय के रूप में स्वीकार करना चाहिए, किन्तु ज्ञापक द्वारा इसे सिद्ध न करना चाहिए ।
दूसरी एक बात श्रीलावण्यसूरिजी यह बताते हैं कि 'स्वाङ्गं' शब्द के कारण ‘पराङ्ग' अव्यवधायक बनता नहीं है, ऐसा स्वीकार करके 'पराङ्ग' का फल बताया कि 'संचस्कार' प्रयोग में, 'च', 'कृ' का अङ्ग है किन्तु सम् या स्सट का अङ्ग नहीं है अतः ‘स्सटि समः - १/३/१२ और लुक्' १/३/१३ से होनेवाला 'सम्' के 'म्' का 'स्' और लोप करते समय 'च' का व्यवधान व्यवधान नहीं माना जायेगा, ऐसा कहना अनर्थक है क्यों कि 'च' स्वाङ्ग ही नहीं है, अतः इस न्याय की प्रवृत्ति होने का कोई अवकाश ही नहीं है।
न्याय की वृत्ति में बताया उसी प्रकार इस न्याय की अनित्यता के कारण से विचिस्कन्त्सति' इत्यादि में षत्व नहीं होता है, और इसी अनित्यता का ज्ञापक 'स्था सेनि सेघ सिच सञ्जां द्वित्वेऽपि' २/३/४० सूत्रगत 'द्वित्वेऽपि' शब्द है और श्रीहेमहंसगणि अपनी इस बात का ही समर्थन करते हुए इस न्याय के स्वोपज्ञ न्यास में कहते हैं कि किसी को शंका हो सकती है कि जैसे षत्व का विधान करनेवाला मुख्य सूत्र 'नाम्यन्तस्था कवर्गात् पदान्तः कृतस्य सः शिड्नान्तरेऽपि' २/३/१५ सूत्र में 'शिट्' और नकार के व्यवधान को व्यवधान माना नहीं है, वैसे यहाँ भी द्वित्व के व्यवधान को, व्यवधान न मानने का विधान 'द्वित्वेऽपि' शब्द से होता है तो, इसे इस न्याय की अनित्यता का ज्ञापक कैसे माना जाय ? उसका प्रत्युत्तर देते हुए वे स्वयं कहते हैं कि यदि यह न्याय नित्य होता तो, द्वित्व द्वारा व्यवधान होता है, ऐसा कहा जा सकता ही नहीं है और 'प्रतितष्ठौ' इत्यादि प्रयोग में आचार्यश्री को षत्व ही इष्ट है, और वह 'शिइनान्तरे' के अधिकार के कारण दूसरे प्रकार का (द्वित्व आदि का) व्यवधान आने से षत्व का निषेध होगा, वह निषेध इस 'स्वाङ्गमव्यवधायि' न्याय से दूर होगा , तथापि आचार्यश्री को कई न्याय अनित्य होते हैं इसलिए न्यायों ऊपर विश्वास नहीं हैं, अतः द्वित्व का व्यवधान होने पर भी, ऐसे प्रयोगों में षत्व होगा ही, ऐसा सूचित करने के लिए सूत्र में 'द्वित्वेऽपि' शब्द रखा है । वह इस न्याय की अनित्यता का ज्ञापन करता है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org