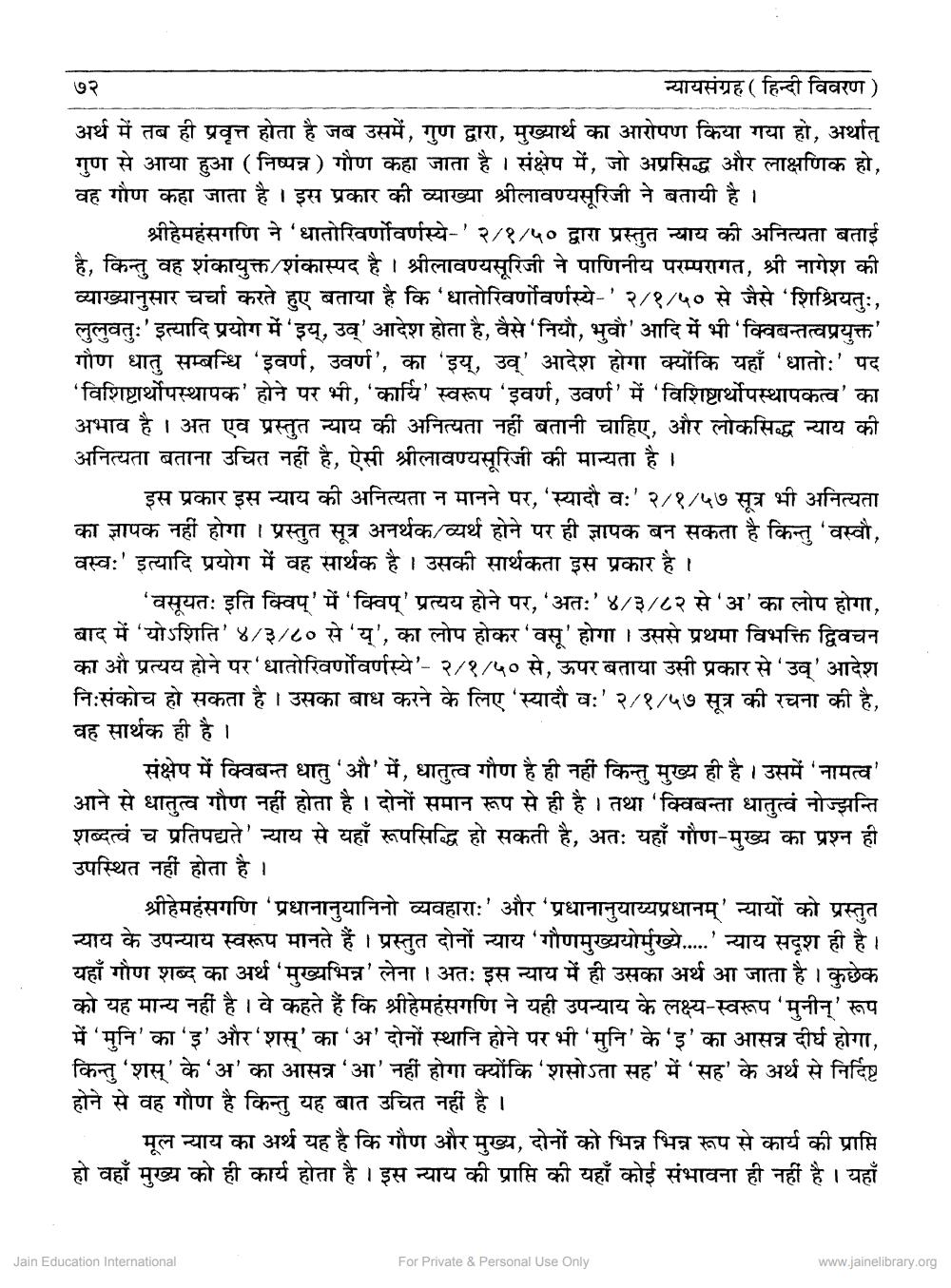________________
७२
न्यायसंग्रह ( हिन्दी विवरण )
अर्थ में तब ही प्रवृत्त होता है जब उसमें, गुण द्वारा, मुख्यार्थ का आरोपण किया गया हो, अर्थात् गुण से आया हुआ (निष्पन्न ) गौण कहा जाता है। संक्षेप में, जो अप्रसिद्ध और लाक्षणिक हो, वह गौण कहा जाता है । इस प्रकार की व्याख्या श्रीलावण्यसूरिजी ने बतायी है ।
श्रीमहंसगणि ने ' धातोरिवर्णोवर्णस्ये- ' २/१/५० द्वारा प्रस्तुत न्याय की अनित्यता बताई है, किन्तु वह शंकायुक्त / शंकास्पद है । श्रीलावण्यसूरिजी ने पाणिनीय परम्परागत, श्री नागेश की व्याख्यानुसार चर्चा करते हुए बताया है कि 'धातोरिवर्णोवर्णस्ये- ' २/१/५० से जैसे 'शिश्रियतुः, लुलुवतुः' इत्यादि प्रयोग में 'इय्, उव्' आदेश होता है, वैसे 'नियौ, भुवौ' आदि में भी 'क्विबन्तत्वप्रयुक्त ' गौ धातु सम्बन्धि 'इवर्ण, उवर्ण', का 'इय्, उव्' आदेश होगा क्योंकि यहाँ 'धातो:' पद 'विशिष्टार्थोपस्थापक' होने पर भी, 'कार्यि' स्वरूप 'इवर्ण, उवर्ण' में 'विशिष्टार्थोपस्थापकत्व' का अभाव है । अत एव प्रस्तुत न्याय की अनित्यता नहीं बतानी चाहिए, और लोकसिद्ध न्याय की अनित्यता बताना उचित नहीं है, ऐसी श्रीलावण्यसूरिजी की मान्यता है ।
इस प्रकार इस न्याय की अनित्यता न मानने पर, 'स्यादौ वः' २/१/५७ सूत्र भी अनित्यता का ज्ञापक नहीं होगा । प्रस्तुत सूत्र अनर्थक / व्यर्थ होने पर ही ज्ञापक बन सकता है किन्तु 'वस्वौ, वस्व:' इत्यादि प्रयोग में वह सार्थक है । उसकी सार्थकता इस प्रकार है ।
'वसूयतः इति क्विप्' में 'क्विप्' प्रत्यय होने पर, 'अत: ' ४/३/८२ से 'अ' का लोप होगा, बाद में ‘योऽशिति' ४/३/८० से 'य्', का लोप होकर 'वसू' होगा । उससे प्रथमा विभक्ति द्विवचन का औ प्रत्यय होने पर 'धातोरिवर्णोवर्णस्ये'- २/१/५० से, ऊपर बताया उसी प्रकार से 'उव्' आदेश निःसंकोच हो सकता है । उसका बाध करने के लिए 'स्यादौ वः' २/१/५७ सूत्र की रचना की है, वह सार्थक ही है ।
संक्षेप में क्विन्त धातु 'औ' में, धातुत्व गौण है ही नहीं किन्तु मुख्य ही है । उसमें 'नामत्व' आने से धातुत्व गौण नहीं होता है । दोनों समान रूप से ही है। तथा 'क्विबन्ता धातुत्वं नोज्झन्ति शब्दत्वं च प्रतिपद्यते' न्याय से यहाँ रूपसिद्धि हो सकती है, अतः यहाँ गौण-मुख्य का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।
श्रीहेमहंसगणि 'प्रधानानुयानिनो व्यवहारा:' और 'प्रधानानुयाय्यप्रधानम्' न्यायों को प्रस्तुत न्याय के उपन्याय स्वरूप मानते हैं । प्रस्तुत दोनों न्याय 'गौणमुख्ययोर्मुख्ये ....' न्याय सदृश ही है । यहाँ गौण शब्द का अर्थ 'मुख्यभिन्न' लेना । अतः इस न्याय में ही उसका अर्थ आ जाता है । कुछेक को यह मान्य नहीं है । वे कहते हैं कि श्रीहेमहंसगणि ने यही उपन्याय के लक्ष्य स्वरूप 'मुनीन्' रूप में 'मुनि' का 'इ' और 'शस्' का 'अ' दोनों स्थानि होने पर भी 'मुनि' के 'इ' का आसन्न दीर्घ होगा, किन्तु 'शस्' के 'अ' का आसन्न 'आ' नहीं होगा क्योंकि 'शसोऽता सह' में 'सह' के अर्थ से निर्दिष्ट होने से वह गौण है किन्तु यह बात उचित नहीं है ।
1
मूल न्याय का अर्थ यह है कि गौण और मुख्य, दोनों को भिन्न भिन्न रूप से कार्य की प्राप्ति हो वहाँ मुख्य को ही कार्य होता है । इस न्याय प्राप्ति की यहाँ कोई संभावना ही नहीं है। यहाँ
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org