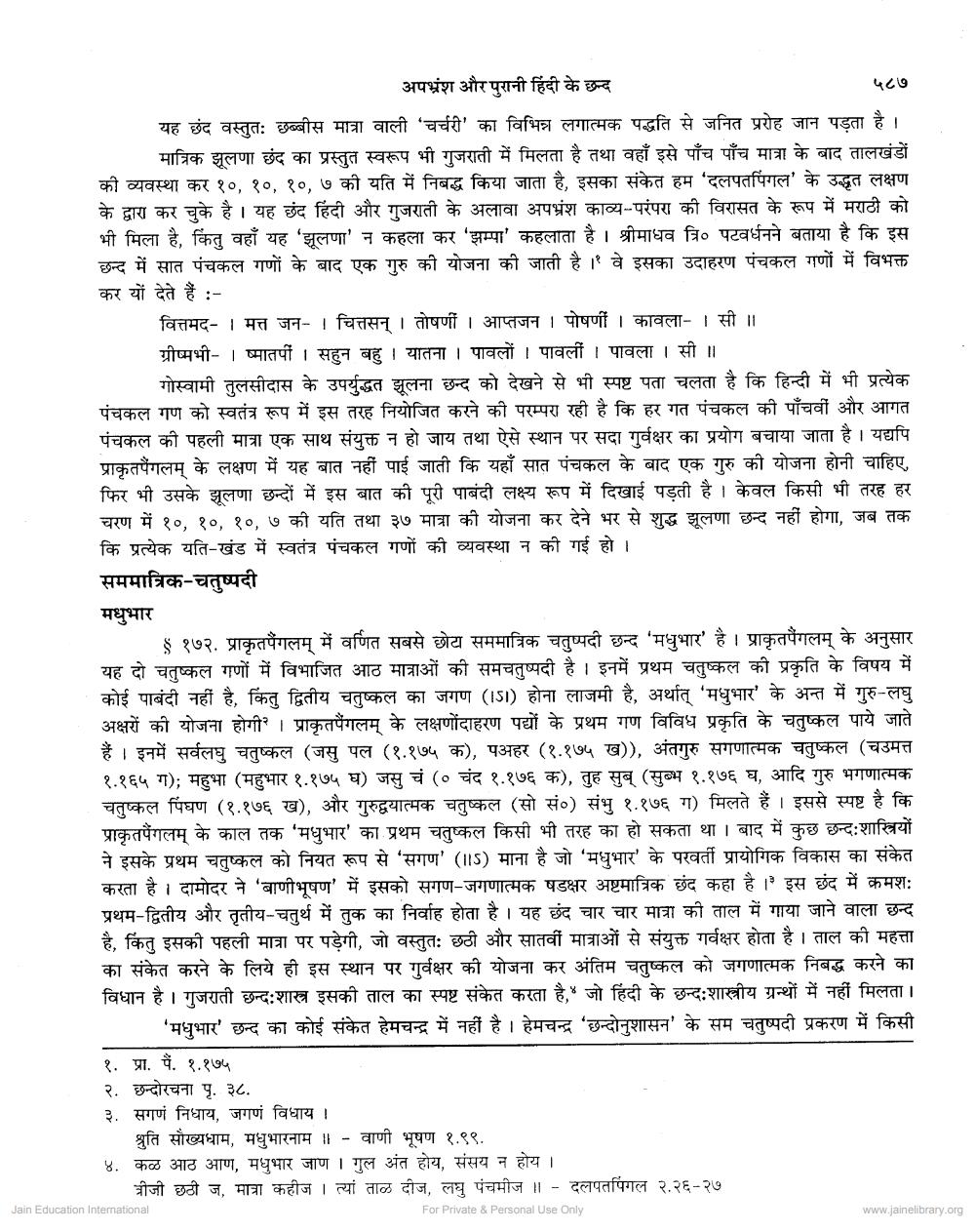________________
अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के छन्द
५८७ यह छंद वस्तुतः छब्बीस मात्रा वाली 'चर्चरी' का विभिन्न लगात्मक पद्धति से जनित प्ररोह जान पड़ता है।
मात्रिक झूलणा छंद का प्रस्तुत स्वरूप भी गुजराती में मिलता है तथा वहाँ इसे पाँच पाँच मात्रा के बाद तालखंडों की व्यवस्था कर १०, १०, १०, ७ की यति में निबद्ध किया जाता है, इसका संकेत हम 'दलपतपिंगल' के उद्धृत लक्षण के द्वारा कर चुके है। यह छंद हिंदी और गुजराती के अलावा अपभ्रंश काव्य-परंपरा की विरासत के रूप में मराठी को भी मिला है, किंतु वहाँ यह 'झूलणा' न कहला कर 'झम्पा' कहलाता है। श्रीमाधव त्रि० पटवर्धनने बताया है कि इस छन्द में सात पंचकल गणों के बाद एक गुरु की योजना की जाती है। वे इसका उदाहरण पंचकल गणों में विभक्त कर यों देते हैं :
वित्तमद- | मत्त जन- | चित्तसन् । तोषणीं । आप्तजन । पोषणीं । कावला- । सी ॥ ग्रीष्मभी- । ष्मातपी । सहुन बहु । यातना । पावलों । पावली । पावला । सी ॥
गोस्वामी तुलसीदास के उपर्युद्धत झूलना छन्द को देखने से भी स्पष्ट पता चलता है कि हिन्दी में भी प्रत्येक पंचकल गण को स्वतंत्र रूप में इस तरह नियोजित करने की परम्परा रही है कि हर गत पंचकल की पाँचवीं और आगत पंचकल की पहली मात्रा एक साथ संयुक्त न हो जाय तथा ऐसे स्थान पर सदा गुर्वक्षर का प्रयोग बचाया जाता है । यद्यपि प्राकृतपैंगलम् के लक्षण में यह बात नहीं पाई जाती कि यहाँ सात पंचकल के बाद एक गुरु की योजना होनी चाहिए, फिर भी उसके झूलणा छन्दों में इस बात की पूरी पाबंदी लक्ष्य रूप में दिखाई पड़ती है। केवल किसी भी तरह हर चरण में १०, १०, १०, ७ की यति तथा ३७ मात्रा की योजना कर देने भर से शुद्ध झूलणा छन्द नहीं होगा, जब तक कि प्रत्येक यति-खंड में स्वतंत्र पंचकल गणों की व्यवस्था न की गई हो । सममात्रिक-चतुष्पदी मधुभार
६ १७२. प्राकृतपैंगलम् में वर्णित सबसे छोटा सममात्रिक चतुष्पदी छन्द 'मधुभार' है। प्राकृतपैंगलम् के अनुसार यह दो चतुष्कल गणों में विभाजित आठ मात्राओं की समचतुष्पदी है। इनमें प्रथम चतुष्कल की प्रकृति के विषय में कोई पाबंदी नहीं है, किंतु द्वितीय चतुष्कल का जगण (151) होना लाजमी है, अर्थात् 'मधुभार' के अन्त में गुरु-लघु अक्षरों की योजना होगी । प्राकृतपैंगलम् के लक्षणोंदाहरण पद्यों के प्रथम गण विविध प्रकृति के चतुष्कल पाये जाते हैं। इनमें सर्वलघु चतुष्कल (जसु पल (१.१७५ क), पअहर (१.१७५ ख)), अंतगुरु सगणात्मक चतुष्कल (चउमत्त १.१६५ ग); महुभा (महुभार १.१७५ घ) जसु चं (० चंद १.१७६ क), तुह सुब् (सुब्भ १.१७६ घ, आदि गुरु भगणात्मक चतुष्कल पिंघण (१.१७६ ख), और गुरुद्वयात्मक चतुष्कल (सो सं०) संभु १.१७६ ग) मिलते हैं। इससे स्पष्ट है कि प्राकृतपैंगलम् के काल तक 'मधुभार' का प्रथम चतुष्कल किसी भी तरह का हो सकता था। बाद में कुछ छन्दःशास्त्रियों ने इसके प्रथम चतुष्कल को नियत रूप से 'सगण' (15) माना है जो 'मधुभार' के परवर्ती प्रायोगिक विकास का संकेत करता है। दामोदर ने 'बाणीभूषण' में इसको सगण-जगणात्मक षडक्षर अष्टमात्रिक छंद कहा है। इस छंद में क्रमश: प्रथम-द्वितीय और तृतीय-चतुर्थ में तुक का निर्वाह होता है। यह छंद चार चार मात्रा की ताल में गाया जाने वाला छन्द है, किंतु इसकी पहली मात्रा पर पड़ेगी, जो वस्तुतः छठी और सातवीं मात्राओं से संयुक्त गर्वक्षर होता है। ताल की महत्ता का संकेत करने के लिये ही इस स्थान पर गुर्वक्षर की योजना कर अंतिम चतुष्कल को जगणात्मक निबद्ध करने का विधान है। गुजराती छन्दःशास्त्र इसकी ताल का स्पष्ट संकेत करता है, जो हिंदी के छन्दःशास्त्रीय ग्रन्थों में नहीं मिलता।
_ 'मधुभार' छन्द का कोई संकेत हेमचन्द्र में नहीं है। हेमचन्द्र 'छन्दोनुशासन' के सम चतुष्पदी प्रकरण में किसी १. प्रा. पैं. १.१७५ २. छन्दोरचना पृ. ३८. ३. सगणं निधाय, जगणं विधाय ।।
श्रुति सौख्यधाम, मधुभारनाम || - वाणी भूषण १.९९. ४. कळ आठ आण, मधुभार जाण । गुल अंत होय, संसय न होय ।
त्रीजी छठी ज, मात्रा कहीज । त्यां ताळ दीज, लघु पंचमीज ।। - दलपतपिंगल २.२६-२७ Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org