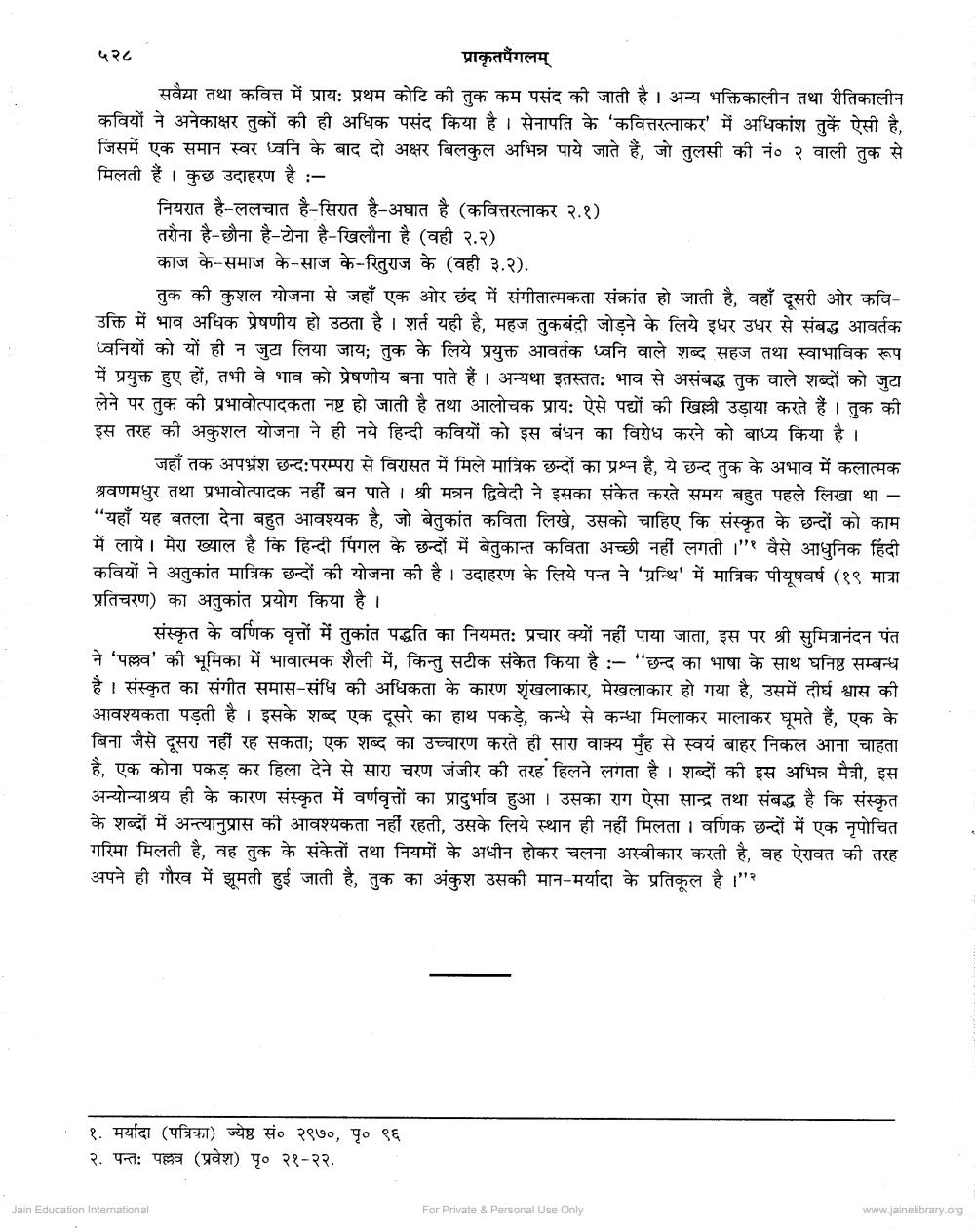________________
५२८
प्राकृतगलम् सवैया तथा कवित्त में प्रायः प्रथम कोटि की तुक कम पसंद की जाती है। अन्य भक्तिकालीन तथा रीतिकालीन कवियों ने अनेकाक्षर तुकों की ही अधिक पसंद किया है । सेनापति के 'कवित्तरत्नाकर' में अधिकांश तुकें ऐसी है, जिसमें एक समान स्वर ध्वनि के बाद दो अक्षर बिलकुल अभिन्न पाये जाते हैं, जो तुलसी की नं० २ वाली तुक से मिलती हैं । कुछ उदाहरण है :
नियरात है-ललचात है-सिरात है-अघात है (कवित्तरत्नाकर २.१) तरौना है-छौना है-टोना है-खिलौना है (वही २.२) काज के-समाज के-साज के-रितुराज के (वही ३.२).
तुक की कुशल योजना से जहाँ एक ओर छंद में संगीतात्मकता संक्रांत हो जाती है, वहाँ दूसरी ओर कविउक्ति में भाव अधिक प्रेषणीय हो उठता है। शर्त यही है, महज तुकबंदी जोड़ने के लिये इधर उधर से संबद्ध आवर्तक ध्वनियों को यों ही न जुटा लिया जाय; तुक के लिये प्रयुक्त आवर्तक ध्वनि वाले शब्द सहज तथा स्वाभाविक रूप में प्रयुक्त हुए हों, तभी वे भाव को प्रेषणीय बना पाते हैं। अन्यथा इतस्ततः भाव से असंबद्ध तुक वाले शब्दों को जुटा लेने पर तुक की प्रभावोत्पादकता नष्ट हो जाती है तथा आलोचक प्रायः ऐसे पद्यों की खिल्ली उड़ाया करते हैं। तुक की इस तरह की अकुशल योजना ने ही नये हिन्दी कवियों को इस बंधन का विरोध करने को बाध्य किया है।
जहाँ तक अपभ्रंश छन्दः परम्परा से विरासत में मिले मात्रिक छन्दों का प्रश्न है, ये छन्द तुक के अभाव में कलात्मक श्रवणमधुर तथा प्रभावोत्पादक नहीं बन पाते । श्री मन्नन द्विवेदी ने इसका संकेत करते समय बहुत पहले लिखा था - "यहाँ यह बतला देना बहुत आवश्यक है, जो बेतुकांत कविता लिखे, उसको चाहिए कि संस्कृत के छन्दों को काम में लाये। मेरा ख्याल है कि हिन्दी पिंगल के छन्दों में बेतुकान्त कविता अच्छी नहीं लगती ।"१ वैसे आधुनिक हिंदी कवियों ने अतुकांत मात्रिक छन्दों की योजना की है। उदाहरण के लिये पन्त ने 'ग्रन्थि' में मात्रिक पीयूषवर्ष (१९ मात्रा प्रतिचरण) का अतुकांत प्रयोग किया है।
संस्कृत के वर्णिक वृत्तों में तुकांत पद्धति का नियमतः प्रचार क्यों नहीं पाया जाता, इस पर श्री सुमित्रानंदन पंत ने 'पल्लव' की भूमिका में भावात्मक शैली में, किन्तु सटीक संकेत किया है :- "छन्द का भाषा के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। संस्कृत का संगीत समास-संधि की अधिकता के कारण शृंखलाकार, मेखलाकार हो गया है, उसमें दीर्घ श्वास की आवश्यकता पड़ती है । इसके शब्द एक दूसरे का हाथ पकड़े, कन्धे से कन्धा मिलाकर मालाकर घूमते हैं, एक के बिना जैसे दूसरा नहीं रह सकता; एक शब्द का उच्चारण करते ही सारा वाक्य मुँह से स्वयं बाहर निकल आना चाहता है, एक कोना पकड़ कर हिला देने से सारा चरण जंजीर की तरह हिलने लगता है। शब्दों की इस अभिन्न मैत्री, इस अन्योन्याश्रय ही के कारण संस्कृत में वर्णवृत्तों का प्रादुर्भाव हुआ । उसका राग ऐसा सान्द्र तथा संबद्ध है कि संस्कृत के शब्दों में अन्त्यानुप्रास की आवश्यकता नहीं रहती, उसके लिये स्थान ही नहीं मिलता । वर्णिक छन्दों में एक नृपोचित गरिमा मिलती है, वह तुक के संकेतों तथा नियमों के अधीन होकर चलना अस्वीकार करती है, वह ऐरावत की तरह अपने ही गौरव में झूमती हुई जाती है, तुक का अंकुश उसकी मान-मर्यादा के प्रतिकूल है।"२
१. मर्यादा (पत्रिका) ज्येष्ठ सं० २९७०, पृ० ९६ २. पन्तः पल्लव (प्रवेश) पृ० २१-२२.
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org