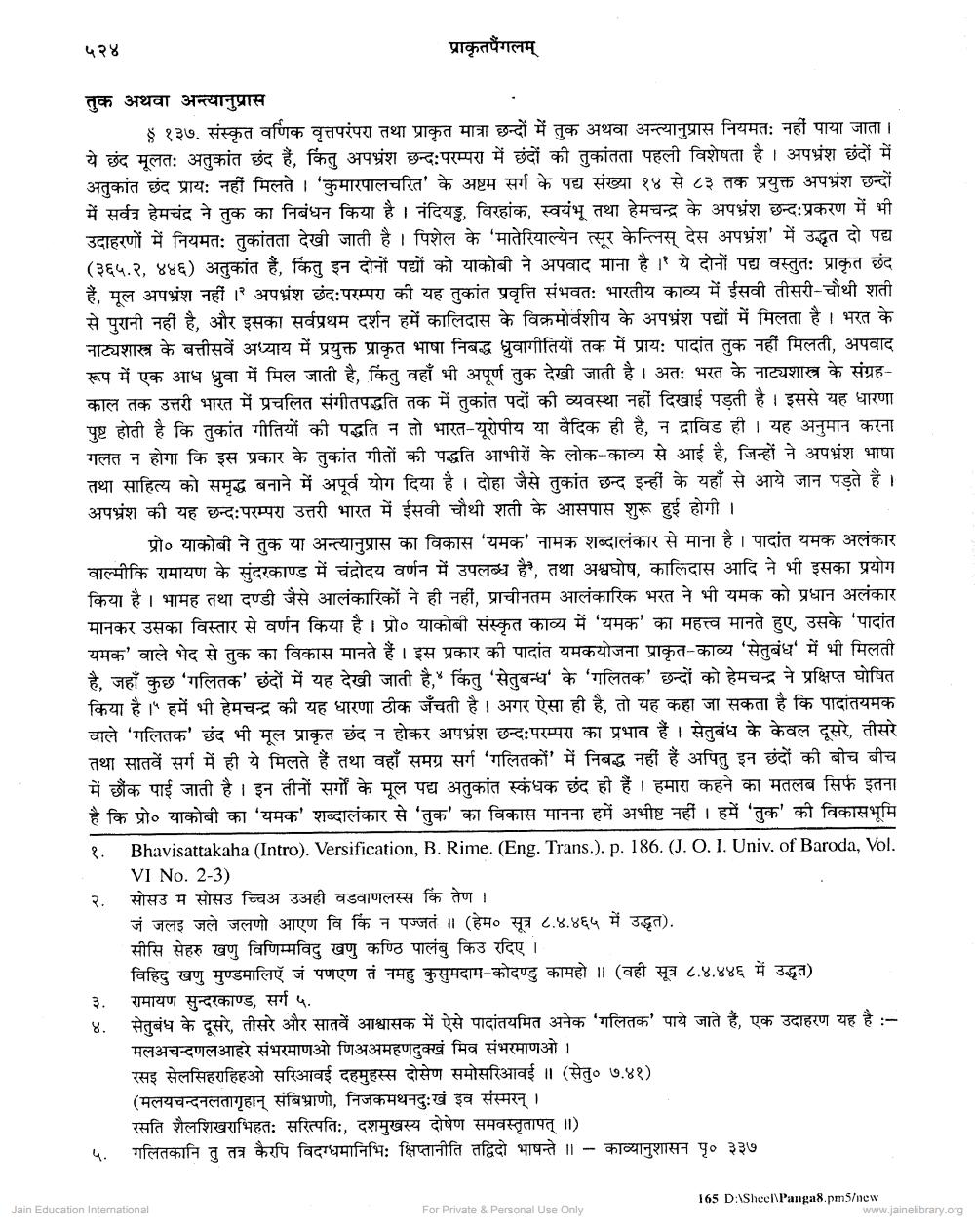________________
५२४
तुक अथवा अन्त्यानुप्रास
१३७. संस्कृत वर्णिक वृत्तपरंपरा तथा प्राकृत मात्रा छन्दों में तुक अथवा अन्त्यानुप्रास नियमतः नहीं पाया जाता। ये छंद मूलतः अतुकांत छंद है, किंतु अपभ्रंश छन्दः परम्परा में छंदों की तुकांतता पहली विशेषता है। अपभ्रंश छंदों में अतुकांत छंद प्रायः नहीं मिलते। 'कुमारपालचरित' के अष्टम सर्ग के पद्य संख्या १४ से ८३ तक प्रयुक्त अपभ्रंश छन्दों में सर्वत्र हेमचंद्र ने तुक का निबंधन किया है । नंदियङ्क, विरहांक, स्वयंभू तथा हेमचन्द्र के अपभ्रंश छन्दः प्रकरण में भी उदाहरणों में नियमतः तुकांतता देखी जाती है । पिशेल के 'मातेरियाल्येन त्सूर केन्निस् देस अपभ्रंश' में उद्धृत दो पद्य (३६५.२, ४४६) अतुकांत है, किंतु इन दोनों पद्यों को याकोबी ने अपवाद माना है। ये दोनों पद्य वस्तुतः प्राकृत छंद हैं, मूल अपभ्रंश नहीं अपभ्रंश छंदः परम्परा की यह तुकांत प्रवृत्ति संभवतः भारतीय काव्य में ईसवी तीसरी चौथी शती से पुरानी नहीं है, और इसका सर्वप्रथम दर्शन हमें कालिदास के विक्रमोर्वशीय के अपभ्रंश पद्यों में मिलता है। भरत के नाट्यशास्त्र के बत्तीसवें अध्याय में प्रयुक्त प्राकृत भाषा निबद्ध धुवागीतियों तक में प्रायः पादांत तुक नहीं मिलती, अपवाद रूप में एक आध ध्रुवा में मिल जाती है, किंतु वहाँ भी अपूर्ण तुक देखी जाती है। अतः भरत के नाट्यशास्त्र के संग्रहकाल तक उत्तरी भारत में प्रचलित संगीतपद्धति तक में तुकांत पदों की व्यवस्था नहीं दिखाई पड़ती है। इससे यह धारणा पुष्ट होती है कि तुकांत गीतियों की पद्धति न तो भारत यूरोपीय या वैदिक ही है, न द्राविड ही यह अनुमान करना गलत न होगा कि इस प्रकार के तुकांत गीतों की पद्धति आभीरों के लोक-काव्य से आई है, जिन्हों ने अपभ्रंश भाषा तथा साहित्य को समृद्ध बनाने में अपूर्व योग दिया है । दोहा जैसे तुकांत छन्द इन्हीं के यहाँ से आये जान पड़ते हैं । अपभ्रंश की यह छन्दः परम्परा उत्तरी भारत में ईसवी चौथी शती के आसपास शुरू हुई होगी ।
प्रो० याकोबी ने तुक या अन्त्यानुप्रास का विकास 'यमक' नामक शब्दालंकार से माना है । पादांत यमक अलंकार वाल्मीकि रामायण के सुंदरकाण्ड में चंद्रोदय वर्णन में उपलब्ध है', तथा अश्वघोष, कालिदास आदि ने भी इसका प्रयोग किया है। भामह तथा दण्डी जैसे आलंकारिकों ने ही नहीं, प्राचीनतम आलंकारिक भरत ने भी यमक को प्रधान अलंकार मानकर उसका विस्तार से वर्णन किया है। प्रो० याकोबी संस्कृत काव्य में 'यमक' का महत्व मानते हुए, उसके पादांत यमक' वाले भेद से तुक का विकास मानते हैं। इस प्रकार की पादांत यमकयोजना प्राकृत काव्य 'सेतुबंध' में भी मिलती है, जहाँ कुछ 'गलितक' छंदों में यह देखी जाती है, किंतु 'सेतुबन्ध' के 'गलितक' छन्दों को हेमचन्द्र ने प्रक्षिप्त घोषित किया है। हमें भी हेमचन्द्र की यह धारणा ठीक जँचती है। अगर ऐसा ही है, तो यह कहा जा सकता है कि पादांतयमक वाले 'गलितक' छंद भी मूल प्राकृत छंद न होकर अपभ्रंश छन्दः परम्परा का प्रभाव है। सेतुबंध के केवल दूसरे, तीसरे तथा सातवें सर्ग में ही ये मिलते हैं तथा वहाँ समग्र सर्ग 'गलितकों' में निबद्ध नहीं हैं अपितु इन छंदों की बीच बीच में छौंक पाई जाती है। इन तीनों सर्गों के मूल पद्य अतुकांत स्कंधक छंद ही हैं। हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि प्रो० याकोबी का 'यमक' शब्दालंकार से 'तुक' का विकास मानना हमें अभीष्ट नहीं
हमें 'तुक' की विकासभूमि
१.
प्राकृतपैंगलम्
Bhavisattakaha (Intro). Versification, B. Rime. (Eng. Trans.). p. 186. (J. O. I. Univ. of Baroda, Vol. VI No. 2-3)
२.
सोसउ म सोसउ च्चिअ उअही वडवाणलस्स किं तेण ।
जं जल जले जलगो आएण वि किं न पज्जतं ॥ (हेम० सूत्र ८.४.४६५ में उद्धृत).
सीसि सेहरु खणु विणिम्मविदु खणु कण्ठि पालंबु किउ रदिए ।
विहिदु खणु मुण्डमालिऍ जं पणएण तं नमहु कुसुमदाम कोदण्डु कामहो । (वही सूत्र ८.४.४४६ में उद्धृत)
३.
४.
५.
रामायण सुन्दरकाण्ड, सर्ग ५.
सेतुबंध के दूसरे, तीसरे और सातवें आश्वासक में ऐसे पादांतयमित अनेक 'गलितक' पाये जाते हैं, एक उदाहरण यह है :मलअचन्दणल आहरे संभरमाणओ निअअमहणदुक्खं मिव संभरमाणओ
रसइ सेलसिहराहिहओ सरिआवई दहमुहस्स दोसेण समोसरिआवई ॥ ( सेतु० ७.४१ )
(मलयचन्दनलतागृहान् संविभ्राणो, निजकमधनदुःखं इव संस्मरन् ।
रसति शैलशिखराभिहतः सरित्पतिः, दशमुखस्य दोषेण समवस्तृतापत् ॥ )
गलितकानि तु तत्र कैरपि विदग्धमानिभिः क्षिप्तानीति तद्विदो भाषन्ते ॥ काव्यानुशासन पृ० ३३७
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
165 D:\Sheel\Panga8.pm5/new
www.jainelibrary.org