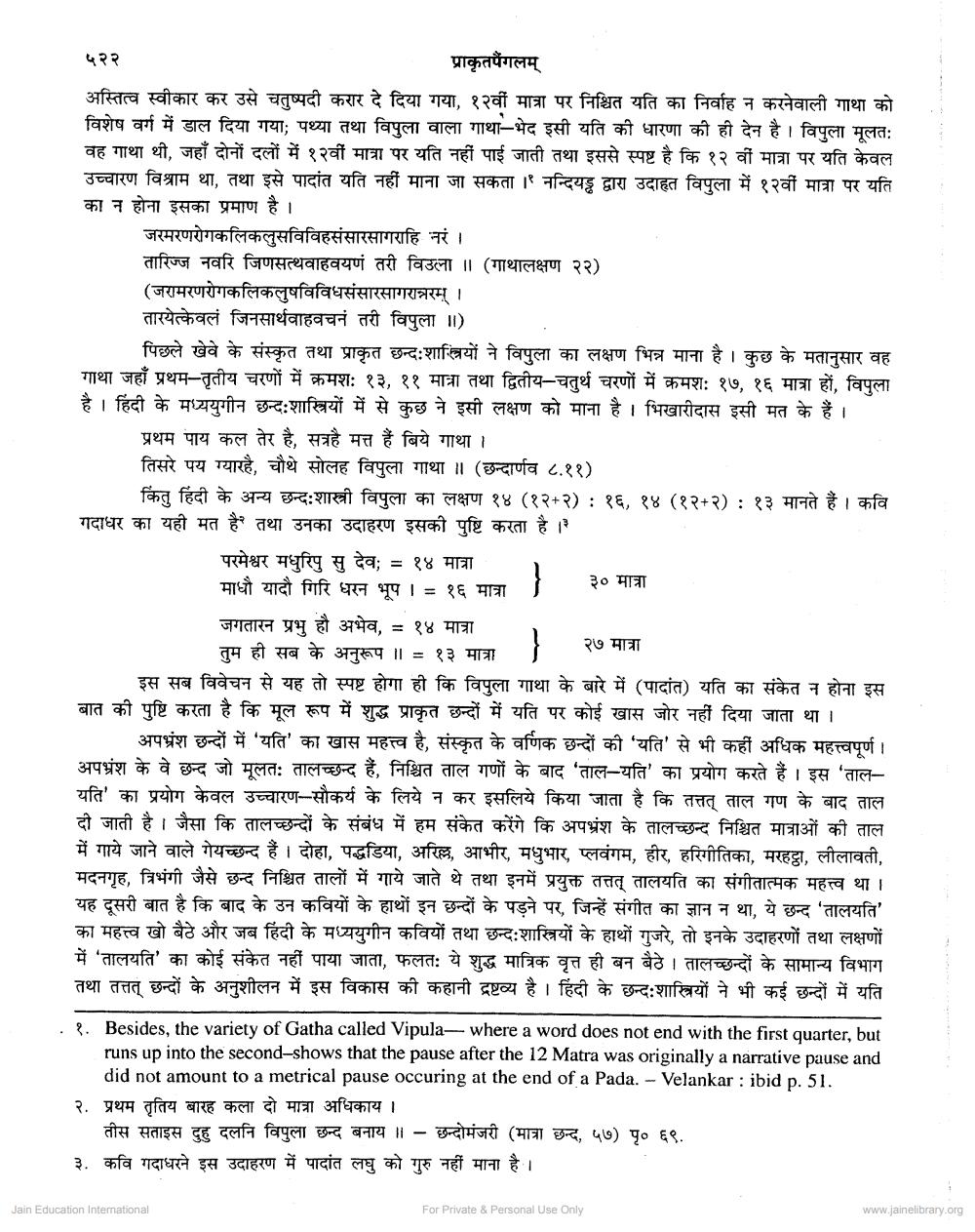________________
५२२
प्राकृतपैंगलम् अस्तित्व स्वीकार कर उसे चतुष्पदी करार दे दिया गया, १२वी मात्रा पर निश्चित यति का निर्वाह न करनेवाली गाथा को विशेष वर्ग में डाल दिया गया; पथ्या तथा विपुला वाला गाथा-भेद इसी यति की धारणा की ही देन है। विपुला मूलतः वह गाथा थी, जहाँ दोनों दलों में १२वी मात्रा पर यति नहीं पाई जाती तथा इससे स्पष्ट है कि १२ वी मात्रा पर यति केवल उच्चारण विश्राम था, तथा इसे पादांत यति नहीं माना जा सकता । नन्दियड्ड द्वारा उदाहृत विपुला में १२वी मात्रा पर यति का न होना इसका प्रमाण है।
जरमरणरोगकलिकलुसविविहसंसारसागराहि नरं । तारिज्ज नवरि जिणसत्थवाहवयणं तरी विउला ॥ (गाथालक्षण २२) (जरामरणरोगकलिकलुषविविधसंसारसागरान्नरम् । तारयेत्केवलं जिनसार्थवाहवचनं तरी विपुला ||)
पिछले खेवे के संस्कृत तथा प्राकृत छन्दःशास्त्रियों ने विपुला का लक्षण भिन्न माना है । कुछ के मतानुसार वह गाथा जहाँ प्रथम-तृतीय चरणों में क्रमश: १३, ११ मात्रा तथा द्वितीय-चतुर्थ चरणों में क्रमशः १७, १६ मात्रा हों, विपुला है । हिंदी के मध्ययुगीन छन्दःशास्त्रियों में से कुछ ने इसी लक्षण को माना है । भिखारीदास इसी मत के हैं।
प्रथम पाय कल तेर है, सत्रहै मत्त हैं बिये गाथा । तिसरे पय ग्यारहै, चौथे सोलह विपुला गाथा ॥ (छन्दार्णव ८.११)
किंतु हिंदी के अन्य छन्दःशास्त्री विपुला का लक्षण १४ (१२+२) : १६, १४ (१२+२) : १३ मानते हैं। कवि गदाधर का यही मत है तथा उनका उदाहरण इसकी पुष्टि करता है ।
परमेश्वर मधुरिपु सु देव; = १४ मात्रा माधौ यादौ गिरि धरन भूप । = १६ मात्रा ३० मात्रा जगतारन प्रभु हौ अभेव, = १४ मात्रा
२७ मात्रा तुम ही सब के अनुरूप ॥ = १३ मात्रा इस सब विवेचन से यह तो स्पष्ट होगा ही कि विपुला गाथा के बारे में (पादांत) यति का संकेत न होना इस बात की पुष्टि करता है कि मूल रूप में शुद्ध प्राकृत छन्दों में यति पर कोई खास जोर नहीं दिया जाता था ।
अपभ्रंश छन्दों में 'यति' का खास महत्त्व है, संस्कृत के वर्णिक छन्दों की 'यति' से भी कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण । अपभ्रंश के वे छन्द जो मूलतः तालच्छन्द हैं, निश्चित ताल गणों के बाद 'ताल-यति' का प्रयोग करते हैं । इस 'तालयति' का प्रयोग केवल उच्चारण-सौकर्य के लिये न कर इसलिये किया जाता है कि तत्तत् ताल गण के बाद ताल दी जाती है। जैसा कि तालच्छन्दों के संबंध में हम संकेत करेंगे कि अपभ्रंश के तालच्छन्द निश्चित मात्राओं की ताल में गाये जाने वाले गेयच्छन्द हैं । दोहा, पद्धडिया, अरिल्ल, आभीर, मधुभार, प्लवंगम, हीर, हरिगीतिका, मरहट्ठा, लीलावती, मदनगृह, त्रिभंगी जैसे छन्द निश्चित तालों में गाये जाते थे तथा इनमें प्रयुक्त तत्तत् तालयति का संगीतात्मक महत्त्व था। यह दूसरी बात है कि बाद के उन कवियों के हाथों इन छन्दों के पड़ने पर, जिन्हें संगीत का ज्ञान न था, ये छन्द 'तालयति' का महत्त्व खो बैठे और जब हिंदी के मध्ययुगीन कवियों तथा छन्दःशास्त्रियों के हाथों गुजरे, तो इनके उदाहरणों तथा लक्षणों में 'तालयति' का कोई संकेत नहीं पाया जाता, फलतः ये शुद्ध मात्रिक वृत्त ही बन बैठे। तालच्छन्दों के सामान्य विभाग तथा तत्तत् छन्दों के अनुशीलन में इस विकास की कहानी द्रष्टव्य है। हिंदी के छन्दःशास्त्रियों ने भी कई छन्दों में यति
. १. Besides, the variety of Gatha called Vipula-where a word does not end with the first quarter, but
runs up into the second-shows that the pause after the 12 Matra was originally a narrative pause and
did not amount to a metrical pause occuring at the end of a Pada. - Velankar : ibid p. 51. २. प्रथम तृतिय बारह कला दो मात्रा अधिकाय ।
तीस सताइस दुहु दलनि विपुला छन्द बनाय ॥ - छन्दोमंजरी (मात्रा छन्द, ५७) पृ० ६९. ३. कवि गदाधरने इस उदाहरण में पादांत लघु को गुरु नहीं माना है।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org