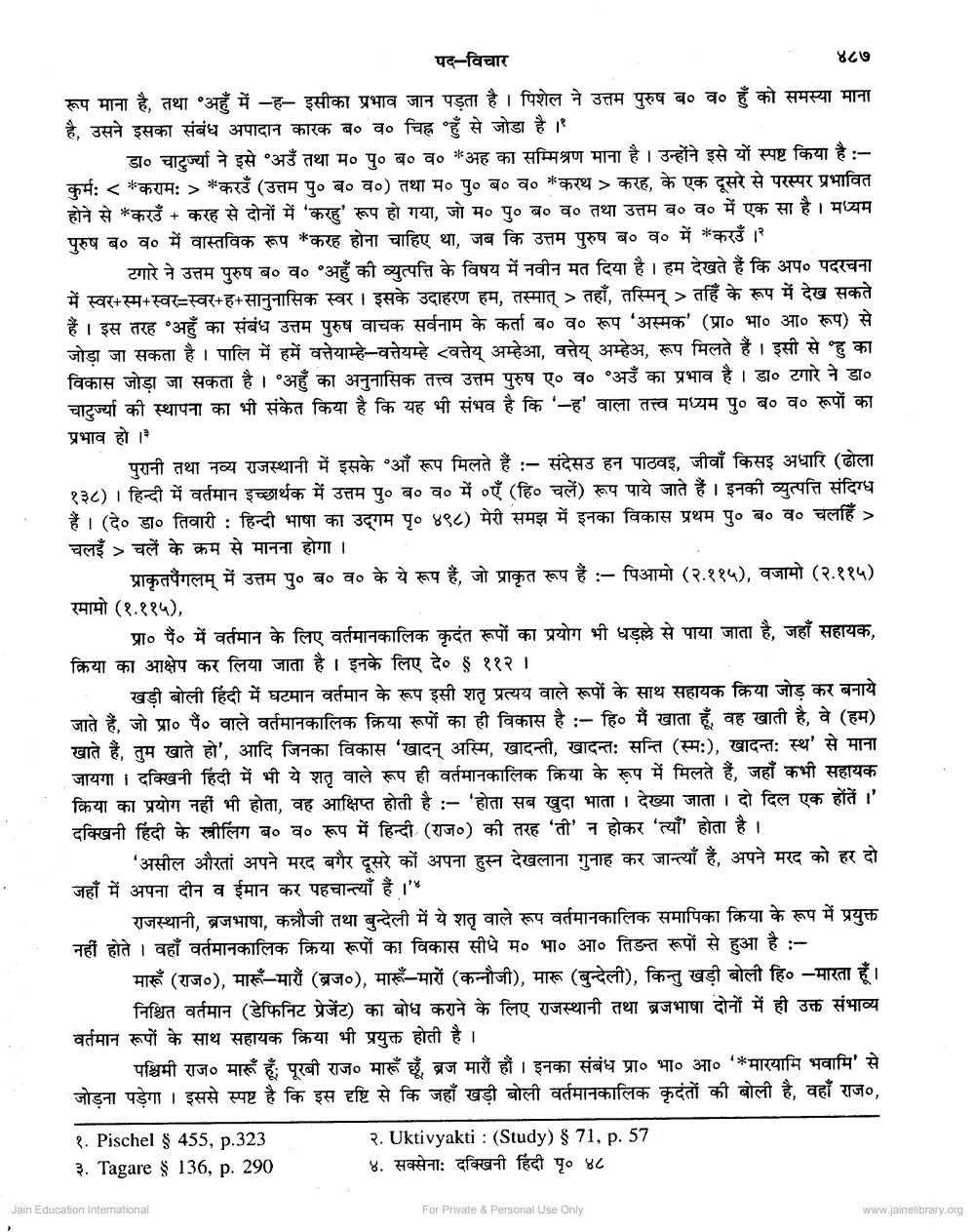________________
पद-विचार
४८७
रूप माना है, तथा 'अहुँ में -ह- इसीका प्रभाव जान पड़ता है। पिशेल ने उत्तम पुरुष ब० व० हुँ को समस्या माना है, उसने इसका संबंध अपादान कारक ब० व० चिह्न हुँ से जोडा है ।।
डा० चाटुा ने इसे अउँ तथा म० पु० ब० व० *अह का सम्मिश्रण माना है। उन्होंने इसे यों स्पष्ट किया है :कुर्मः < *करामः > *करउँ (उत्तम पु० ब० व०) तथा म० पु० ब० व० *करथ > करह, के एक दूसरे से परस्पर प्रभावित होने से *करउँ + करह से दोनों में 'करहु रूप हो गया, जो म० पु० ब० व० तथा उत्तम ब० व० में एक सा है। मध्यम पुरुष ब० व० में वास्तविक रूप *करह होना चाहिए था, जब कि उत्तम पुरुष ब० व० में *करउँ ।
टगारे ने उत्तम पुरुष ब० व० अहुँ की व्युत्पत्ति के विषय में नवीन मत दिया है । हम देखते हैं कि अप० पदरचना में स्वर+स्म+स्वर स्वर+ह-सानुनासिक स्वर । इसके उदाहरण हम, तस्मात् > तहाँ, तस्मिन् > तहिँ के रूप में देख सकते हैं। इस तरह 'अहुँ का संबंध उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम के कर्ता ब० व० रूप 'अस्मक' (प्रा० भा० आ० रूप) से जोड़ा जा सकता है। पालि में हमें वत्तेयाम्हे-वत्तेयम्हे <वत्तेय् अम्हेआ, वत्तेय् अम्हेअ, रूप मिलते हैं । इसी से हु का विकास जोड़ा जा सकता है। अहुँ का अनुनासिक तत्त्व उत्तम पुरुष ए० व० अउँ का प्रभाव है । डा० टगारे ने डा० चाटुा की स्थापना का भी संकेत किया है कि यह भी संभव है कि '-ह' वाला तत्त्व मध्यम पु० ब० व० रूपों का प्रभाव हो ।
पुरानी तथा नव्य राजस्थानी में इसके आँ रूप मिलते हैं :- संदेसउ हन पाठवइ, जीवाँ किसइ अधारि (ढोला १३८) । हिन्दी में वर्तमान इच्छार्थक में उत्तम पु० ब० व० में ०एँ (हि० चलें) रूप पाये जाते हैं । इनकी व्युत्पत्ति संदिग्ध हैं । (दे० डा० तिवारी : हिन्दी भाषा का उद्गम पृ० ४९८) मेरी समझ में इनका विकास प्रथम पु० ब० व० चलहिँ > चलइँ > चलें के क्रम से मानना होगा।
प्राकृतपैंगलम् में उत्तम पु० ब० व० के ये रूप हैं, जो प्राकृत रूप हैं :- पिआमो (२.११५), वजामो (२.११५) रमामो (१.११५),
प्रा० पैं० में वर्तमान के लिए वर्तमानकालिक कृदंत रूपों का प्रयोग भी धड़ल्ले से पाया जाता है, जहाँ सहायक, क्रिया का आक्षेप कर लिया जाता है। इनके लिए दे०६ ११२ ।
खड़ी बोली हिंदी में घटमान वर्तमान के रूप इसी शतृ प्रत्यय वाले रूपों के साथ सहायक क्रिया जोड़ कर बनाये जाते हैं, जो प्रा० पैं० वाले वर्तमानकालिक क्रिया रूपों का ही विकास है :- हि० मैं खाता हूँ, वह खाती है, वे (हम) खाते हैं, तुम खाते हो', आदि जिनका विकास 'खादन् अस्मि, खादन्ती, खादन्तः सन्ति (स्मः), खादन्तः स्थ' से माना जायगा । दक्खिनी हिंदी में भी ये शत वाले रूप ही वर्तमानकालिक क्रिया के रूप में मिलते हैं, जहाँ कभी सहायक किया का प्रयोग नहीं भी होता, वह आक्षिप्त होती है :- 'होता सब खुदा भाता । देख्या जाता । दो दिल एक होंतें ।' दक्खिनी हिंदी के स्त्रीलिंग ब० व० रूप में हिन्दी (राज.) की तरह 'ती' न होकर 'त्याँ' होता है ।
'असील औरतां अपने मरद बगैर दूसरे को अपना हुस्न देखलाना गुनाह कर जान्त्याँ हैं, अपने मरद को हर दो जहाँ में अपना दीन व ईमान कर पहचान्त्याँ हैं ।'
राजस्थानी, ब्रजभाषा, कन्नौजी तथा बुन्देली में ये शतृ वाले रूप वर्तमानकालिक समापिका क्रिया के रूप में प्रयुक्त नहीं होते । वहाँ वर्तमानकालिक क्रिया रूपों का विकास सीधे म० भा० आ० तिङन्त रूपों से हुआ है :
मारूँ (राज०), मारूं-मारौं (ब्रज०), मारूं-मारों (कन्नौजी), मारू (बुन्देली), किन्तु खड़ी बोली हि० –मारता हूँ।
निश्चित वर्तमान (डेफिनिट प्रेजेंट) का बोध कराने के लिए राजस्थानी तथा ब्रजभाषा दोनों में ही उक्त संभाव्य वर्तमान रूपों के साथ सहायक क्रिया भी प्रयुक्त होती है।
पश्चिमी राज० मारूँ हूँ; पूरबी राज० मारूँ छु, ब्रज मा हौं । इनका संबंध प्रा० भा० आ० *मारयामि भवामि' से जोड़ना पड़ेगा। इससे स्पष्ट है कि इस दृष्टि से कि जहाँ खड़ी बोली वर्तमानकालिक कृदंतों की बोली है, वहाँ राज०,
१. Pischel $455, p.323 ३. Tagare $ 136, p. 290
२. Uktivyakti : (Study) 871, p. 57 ४. सक्सेनाः दक्खिनी हिंदी पृ० ४८
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org